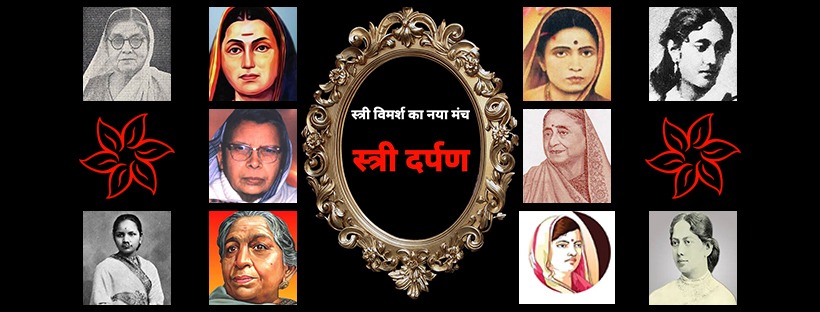अनुराधा गुप्ता
जन्म और शिक्षा कानपुर (UP) से।
सम्प्रति- सहायक प्रवक्ता हिंदी विभाग कमला नेहरू कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय
शोध व अध्ययन का क्षेत्र व रुचि- हिंदी कथा आलोचना
कई पत्र पत्रिकाओं में लेख प्रकाशित।
………………
कृष्णा सोबती : ‘बादलों के घेरे’ से
“औक़त न क़लम की /न लेखक की/न लेखन की/ज़िन्दगी फैलती चली गई/कागज़ के पन्नों पर/कुछ इस तरह ज्यों धरती में उग आया हो/विशाल जड़ों वाला एक ज़िदा रुख”(कृष्णा सोबती,‘ज़िंदगीनामा’ के आरम्भ में दी गई पंक्तियाँ)
कहानी के सिरजे गए पात्र जब रचनाकार के जीवन की संचित अनुभूति का परिणाम हों तो निश्चय ही कागज़ के पन्नों पर सायास गढ़े गए चरित्र नहीं असल ज़िन्दगियां खुद-ब-खुद फैलती जाती हैं..अनायास| कृष्णा सोबती न सिर्फ हिन्दी कथा जगत बल्कि पूरे विश्व के कथा साहित्य में एक अकेली, अपनी तरह की अनोखी सशक्त कथाकारा हैं| हिन्दी कथा लेखन में जिस तरह के बोल्ड लेखन की शुरुआत उन्होंने की वह स्त्री विमर्श के क्षेत्र का क्रांतिकारी कदम था|उनकी पहचान एक ऐसी लेखिका के रूप में जानी जाती है जो भारतीय स्त्री के अव्यक्त मन की सघन, बहुपरतीय खोह के भीतर मचलते-सुबकते स्पंदन को महसूस कर उसकी सूक्ष्म से सूक्ष्म गांठ को खोल देने का साहस और सामर्थ्य रखती हो| निःसंदेह कृष्णा सोबती का नाम हिन्दी कथाकारों में अग्रणी है|
१९५० में उनकी पहली रचना प्रकाशित हुई और अभी हाल ही में उनका नाम ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए घोषित किया गया | कह सकते हैं कि ६७ साल की साधना जब किसी पुरस्कार तक पहुंचती है तो उस पुरस्कार की अहमियत बढ़ जाती है| उनका साहित्य हिन्दुस्तानी ज़ुबान का म्यूजियम कहा जाता है| उनकी किसी भी किताब के पन्ने पलट लें,आप उन शब्दों के साथ जीने लगेगे जो हमारे पुरखे विरासत में छोड़ गए है| ९२ वर्ष की सोबती हिन्दी साहित्य और समाज का चलता फिरता इतिहास हैं| वो हिन्दी की सबसे नौजवान और जुझारू लेखिका हैं| बीते साल बढती असहिष्णुता को लेकर जब चिंतित बौद्धिकों और चिंतकों ने सभा की तो कृष्णा सोबती ने भी विरोध की आवाज़ मुखर कर बाबरी से दादरी के खिलाफ बराबरी की बात की| ये प्रतिरोध किसी दल विशेष के समर्थन या असमर्थन में नहीं था बल्कि उनकी इंसानी और लोकतांत्रिक वैचारिक पक्षधरता का परिणाम था तभी कांग्रेस शासन में भी उन्होंने पद्मविभूषण का प्रस्ताव लौटाया | वो प्रतिरोध की आवाज़ हैं जो लगातार रचनारत है | ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा करते हुए और उन्हें बधाई देते हुए लीलाधर मंडलोई ने कहा कि हिन्दी उर्दू पंजाबी भाषा की लोकशीलता के साथ उन्होंने जो अद्भुत शिल्प, वस्तु और अंतर्वस्तु की शिनाख्त की है वो बेजोड़ है.
हिन्दी साहित्य समाज में जिस आज़ाद औरत की बात की जाती है सोबती ने सम्भवत: उसे सबसे पहले गढ़ा| उनके कथा साहित्य की नायिकाएं जिस जिंदादिली, बेलौस, बेधकड़क अंदाज में अपना जीवन जीती रहीं उसे बाद में कई लेखिकाओं ने अपने किरदारों के लिए अपनाया. अपनी नई किताब ‘गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिन्दुस्तान’ में वो अपनी ज़िन्दगी के एक हिस्से को उपन्यास में ढालती हैं. उस हिस्से को जब देश बटा था समाज बटा था तहजीब बटी थी और इंसानियत लहू-लुहान होकर कट-छट गयी थी| इस उपन्यास में वे बेहद तकलीफ से लिखती हैं, “अब तो हम तेज़ किए हुए चाकू हैं| हम आग का पलीता हैं| हम दुश्मनों को चाक कर देने वाली गरम हिंसा हैं| हम दुल्हनों की बाँहें काट देने वाले टोके हैं| हम गंडासे हैं| अब हम हम नहीं हैं, हथियार हैं|”
कृष्णा सोबती लगभग एक पूरी सदी जी चुकी हैं ,उनके संस्मरण, आत्मकथात्मक लेख और साक्षात्कार पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई वाचिक इतिहास शुरू हो गया हो| जिस साल भारत गणतन्त्र बना १९५० में ‘लामा’ उनकी पहली कहानी छपी| तब से उनकी कलम चलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है| सोबती का साहित्य इतिहास द्वारा बेदखल की जा रही मनुष्यता का पक्ष है| मेरे लेख का केंद्र उनका कहानी संग्रह ‘बादलों के घेरे’ है, जिसका का प्रकाशन 1980 में हुआ| इसमें २४ छोटी बड़ी रचानाएं हैं| विषय की दृष्टि से इन्हें प्रेम और स्त्री-पुरुष सम्बन्ध से सम्बन्धी, पूरे सामाजिक परिप्रेक्ष्य में स्त्री की यातना को और उस के परिवेशगत अंतर्द्वंद्व के चित्रण सम्बन्धी और विभाजन की यातना को जीती, लहू-लुहान होती इंसानियत से सम्बन्धी कहानियों की श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं| इस संग्रह के कवर पेज पर वे लिखती हैं कि इन कहानियों में एक समय है जो बीत जाने के बाद भी हमारे जीवन में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, जो अविस्मरणीय है और उससे कुछ न कुछ हम सीखते हैं और अपने जीवन को आगे बढाने के लिए प्रेरित होते हैं| ये कहानियाँ पाठकों को सम्वेदनाओं के कई धरातलों पर छूती हैं उन्हें झकझोरती और उनका हृदय करुणा और सम्वेदना से भर उठता है. विजय मोहन सिंह इनकी रचनाओं के बारे में ‘बीसवीं शताब्दी का हिन्दी साहित्य’ में लिखते हैं , “ सोबती जी के कथा लेखन की विशेषता समझने के लिए उनका बारीकी से अध्य्यन करना जरूरी है वरना उनकी कहानियों की बनावट इतनी सघन है कि प्राय: आसानी से सरलीकृत निष्कर्ष निकाल लिए जाते हैं|” इस सरलीकृत का ही नतीजा है कि आलोचक गोपाल राय हिन्दी कहानी का इतिहास -2 में ‘बादलों के घेरे’ कहानी के बरक्स उनकी अन्य कहानियों में ‘याद रखने वाली कोई विशेष बात नहीं’ देखते हैं|
कृष्णा सोबती जिस समय रचना कर्म में पदार्पण करती हैं वह समय न सिर्फ राजनीति, और समाज बल्कि उनके लेखन के दौर के क्रम में साहित्य में भी गहरे बदलाव और उथल-पुथल का दौर था| ‘बादलों के घेरे’ की दो चार कहानियों को छोड़कर बाकी की कहानियों का रचना काल हिन्दी कहानी साहित्य में ‘नई कहानी’ आन्दोलन नाम से जाना जाता है| यह वह समय था जब आज़ादी के बाद का मोहभंग, मूल्य संक्रमण, संयुक्त परिवारों का विघटन, पुरानी पीढ़ी के परिवार में व्यर्थ होते जाने की पीड़ा, स्त्री-पुरुष संबंधों में आता गहरा बदलाव, व्यक्ति स्वातन्त्र्य, अस्तित्व के लिए संघर्ष और स्त्री में आती चेतना जैसे नए बदलाव तेजी से उभर रहे थे| सोबती इस समय को जी रहीं थीं| उनका लेखन इस बदलाव को आत्मसात कर धीरे-धीरे अपनी रौ में बहता है , यहाँ बदलाव की सब कुछ उखाड़ फेंकने की आंधी नहीं| ये सच है कि प्रेम सम्बन्धों को लेकर इस संग्रह की कहानियां उनके उपन्यासों के बरअक्स रोमानी और भावुक हैं| “बावजूद ,इस तथ्य को नए सिरे से उद्घाटित करतीं हैं कि तन का धर्म मन के धर्म से अलग नहीं होता | नई कहानी आन्दोलन के दौर में जैनेन्द्र और अज्ञेय की मनोवैज्ञानिक कहानियों के विरुद्ध काफी कुछ लिखा गया| कृष्णा सोबती उसी परिवर्तित दृष्टि को रचनात्मक स्तर व्यक्त करती हैं|”(मधुरेश,हिन्दी कहानी का विकास,पृष्ठ103) इस जगह वे अपने दौर के अमूमन कहानी लेखकों से अलग भी पड़ती दिखती हैं जहाँ उनके समकालीन लेखक स्त्री-पुरुष रिश्तों में अहम की गुंजलकों में उलझे थे, वे प्रेम और सिर्फ प्रेम को तरजीह देती हैं| वे प्रेम से भरे स्त्री-पुरुष विशेषकर स्त्री के मन की अतल गहराइयों को गहरे नापने की कोशिश करती हैं| यहाँ वे नई कहानी आन्दोलन के मूल स्वर ‘भोगे हुए यथार्थ’ के स्थान पर समाज में मौजूद चलते-फिरते पात्रों की कहानियाँ कहने का प्रयास करती हैं| उन्होंने जटिल यथार्थ को कहानी में रचा,फिर चाहे क्यों न उस पर आदर्श और रुमान के आरोप लगे हों |
‘बादलों के घेरे’, ‘कुछ नहीं-कोई नहीं’, ‘एक दिन’, ‘पहाड़ों के साए तले’ और ‘दो राहें :दो बाँहें’ जैसी कहानियां अलग-अलग तरीके से एक ही भाव को कैनवस पर अलग-अलग रंगों से उकेरती हैं ये भाव है स्त्री-पुरुष का अह्मरहित, निज रहित अटूट सान्द्र प्रेम| ‘बादलों के घेरे’ में व्याप्त स्वार्थरहित निश्छल प्रेम की सघनता और गहरी सम्वेदना के सन्दर्भ में गोपाल राय लिखते हैं, “जो कहानी सम्वेदनात्मक तीव्रता की दृष्टि से मन को छूती है, और बार-बार पढ़कर भी बासी नहीं लगती, वह कहानी है : ‘बादलों के घेरे’| इस कहानी में प्रेम की जानमारू संवेदना का, क्षय रोग से ग्रस्त,मृत्यु की प्रतीक्षा करते व्यक्ति के रीतते प्राणों की घुटन और अकेलापन का, अपनों के पराए हो जाने की विवशता का दुर्लभ अंकन हुआ है |प्रेम की सम्वेदना का अंकन इतने संकेतात्मक, पर प्रभावी रूप में हुआ है कि उससे गुजरते हुए सिहरन हो जाती है|…इस कहानी में भाषा अपनी सर्जनात्मकता के शिखर पर पहुंची हुई है और उससे संवेदना मानो टपकती हुई प्रतीत होती है|”(हिन्दी कहानी का इतिहास-2 पृष्ठ ६६-६७)
‘कुछ नहीं-कोई नहीं’ में पर-पुरुष के प्रेम में पड़ी विवाहित स्त्री के मन के द्वंद बेहद बारीकी से उजागर हुए हैं| पति रूप के मित्र आनन्द के प्रति शिवा के अंजाने आकर्षण और समर्पण के बाद पति की ठंडी और कठोर प्रतिक्रिया उसे घर छोडकर आनन्द के साथ जाने को विवश कर देती है| किन्तु वह कभी भी आनन्द के साथ रूप की पत्नी की तरह स्वाभिमान और अधिकार से नहीं रह पाती| बच्चों के लिए वह दूसरी माँ है, जो जिम्मेदार है उनके पिता को उनसे अलग करने के लिए, समाज की दृष्टि में ‘दूसरी औरत’ के भाव के अपराध बोध से ग्रस्त शिवा के पास अपने निर्णय पर पछताने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं| उसकी नियति इतनी कठोर है कि आनन्द की मृत्यु हो जाती है, घर और उसकी प्रापर्टी पर उसका कोई हक नहीं इसलिए उसे घर से बाहर जाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया जाता है| अंतत: अपने निर्णय के कारण शिवा एकाकी, अपराध बोध से ग्रस्त जीवन बिताने पर विवश है| वहीं ‘एक दिन’ में दो स्त्रियाँ एक पुरुष की पत्नी बनकर उसकी प्रेम की दया पर निर्भर हैं,यही उनकी नियति है| धर्मपाल पत्नी शीला के होते हुए भी दूसरी स्त्री श्यामा को घर में पत्नी की तरह रखता है| शीला की पीड़ा ,श्यामा के भीतर का असुरक्षा का भाव और धर्मपाल का उनके भाग्य विधाता के रूप में दोनों तरफ डांवाडोल मन; स्त्री के कोमल मन, पति रूपी पुरुष के प्रति पूर्ण समर्पण, समाज भीरुता , पति के प्रति स्वामी भाव और निष्ठा को व्यक्त करता है| पहली कहानी जहां ‘समाज में प्रेम के अनाम सम्बन्ध की अपेक्षा वैवाहिक जीवन का प्रेम ही अंतत: सत्य है’ का दर्शन , वहीं दूसरी कहानी पति के व्यभिचारी, अनैतिक, अमर्यादित रूप को शीला द्वारा क्षमा कर, मायके गयी श्यामा के कारण पति के कुछ दिनों के खैरात में मिले प्रेम को पुन: अपनाकर अपना भाग्य सराहना; समाज में पुरुष शोषित व्यवस्था का चित्रण है| ये दोनों कहानियाँ ’५२, से , ‘५५ के समय की हैं| विजयमोहन सिंह की यदि मानें तो इन्हें तत्कालीन समय का दस्तावेज़ समझ आदर्श प्रेम, आदर्श समाज, वैवाहिक संस्था की आदर्श परिकल्पना की कहानियां समझना इनका सरलीकृत निष्कर्ष होगा| तो क्या ६० के दशक में ‘मित्रो मरजानी’ की मित्रो जैसी कद्दावर पात्र रचने वाली सोबती इन कहानियों के रूप में पुरुषपोषक व्यवस्था का पोषण कर रही थीं? मेरी समझ में ऐसा नहीं है | वो शिवा, श्यामा, और शीला जैसे स्त्री पात्रों के माध्यम से अपने समय को रच रहीं थीं| ये वो स्त्रियाँ हैं जिनका मानसिक अनुकूलन पुरुष सत्तात्मक समाज द्वारा किया गया है| ये अनुकूलन ही स्त्री शोषण की जड़ है| स्त्री का द्वंद और तनाव, झटके से रिश्तों को तोड़ न पाने की कशमकश ; यह शुरुवात थी उस प्रतिरोध की जो आगे जाकर मित्रो की आवाज़ बनती है| यहीं से आगे चलकर सोबती के पात्र जीवन के तमाम निषेधों, वर्जनाओं, द्वन्द्वों और अपराधबोध को तोड़कर बाहर आ सके|
इस संग्रह की कहानियों की कालावधि १९४४ से १९६० तक की है| जिसमें ‘नफ़ीसा’ जैसी डेढ़ पृष्ठ की छोटी सी कहानी से लेकर २० पृष्ठ तक की ‘बादलों के घेरे’ जैसी लम्बी कहानियां हैं| उनके कथा साहित्य का फलक विस्तृत है| इनकी ‘मित्रो मरजानी’, ‘ तिन पहाड़’, ‘यारों के यार’ जैसी रचनाएं उन दिनों कहानी के रूप में विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपीं बाद में उन्हें उपन्यास का रूप दिया गया| इनकी कहानियों में व्याप्त मांसलता और बोल्डनेस को लेकर विभिन्न आलोचकों ने समय-समय पर अपना विवाद, ऐतराज जाहिर किया क्योंकि जिस तरह के लेखन का साहस वो कर सकीं उनके दौर की सम्भवत; ही कोई लेखिका कर सकी. ‘बादलों के घेरे’ में उनकी लम्बी कथा-यात्रा को समेटती चौबीस कहानियां हैं| इनमें उनकी एकदम आरम्भिक दौर की कहानियों में ‘नफ़ीसा’ और ‘लामा’ सन १९४४ की हैं| डेढ़ पृष्ठ की कहानी ‘नफ़ीसा’ और दो-सवा दो पृष्ठ की कहानी ‘लामा’ बालमन की बेहतरीन कहानियां हैं, जहां मृत्यु के अर्थ और उसके भय से बचपन नावाकिफ़ है| छोटी सी कहानी ‘नफ़ीसा’ एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो अपने परिवार से अलग अस्पताल में अपने नजदीक आती मृत्यु से अंजान,अपने परिवार और वहां बीतते दिनों की याद में तरसती है, हंसती है फिर खेलती है|उसकी मासूमियत,और उसके बचपन को निगलता काल कितना निर्मम और क्रूर है, वो नहीं जानती| छोटी सी कहानी में सम्वेदना का अंतर्व्याप्त सघन रूप चमत्कृत करता है , “वह जीवन का मोल नहीं जानती,मौत को भी नहीं पहचानती| उसकी आँखों में भोलापन है,सिर्फ भोलापन! उसे न बीमारी का खौफ़ है ,न मौत का डर| वह तो जानती है खिलौने, गुड़िया,मोटर,तांगा, अम्मी और अब्बा नूरी और इकबाल|” इसी तरह बचपन के खेल में जीवन को झकझोर देने वाली अप्रत्याशित घटना के बालमन पर प्रभाव को लेकर लिखी गयी कहानी ‘टीलो ही टीलो’ है|
‘बदली बरस गई’, ‘आज़ादी शम्मोजान की’ और ‘गुलाबजल गंडेरियाँ’ कहानियाँ स्त्री की अतीव पीड़ा और यातना को उनके सामाजिक परिप्रेक्ष्य में अंकित करने वाली कहानियां हैं| इनमें किसी भी प्रकार का निषेध या वर्जनाएं नहीं है, न ही भावुकता और रोमान| बदली बरस गई पति की मृत्यु के बाद ससुराल में यातना और घरेलू हिंसा की शिकार स्त्री का गुरु की शरण में जाना और वहां जाकर सांसारिक मोह माया से दूर होकर साध्वी माता बनने की कोशिश में युवा होती बेटी का सामाजिक मोह का चित्रण बेहद रोमांचक है| माँ ने समस्याओं से पलायन कर लिया लेकिन उसकी बेटी सामाजिक मोह माया से जबरन मुंह नहीं मोड़ सकती| वह उसी घर में पुन: जाने का फैसला लेती है जो उसकी माँ छोड़ कर आई थी| ‘आज़ादी शम्मोजान की’ बेहद मार्मिकता से देह व्यापार में संलिप्त स्त्रियों की पीड़ा को उकेरती है| पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा है लेकिन शम्मोजान के लिए आज़ादी का मतलब बेमानी है, बेमतलब है | यहाँ कमलेश्वर की कहानी ‘माँस का दरिया’ याद आती है| देह व्यापार की वीभत्सता और कुरूपता उनके तन और मन दोनों को छलनी कर देती है साथ ही इस कहानी में लेखिका एक प्रश्न और उठाती है देह की आज़ादी का, ‘मुन्नी ने अपनी कसी और तंग कमीज में से जरा लम्बी सांस लेकर कहा, “क्या कहा,आज़ादी? लोगों को आज मिल रही है आज़ादी! आज़ादी तो हमारे पास है| हम –सा आज़ाद कौन होगा,शम्मोजान ?”… अपने अंदर ढंके पर्दों को उघाड़कर अगर वह भी देखे,तो एक टूटी आहत छाया उसकी उनींदी आँखों से झलक जाएगी| सालों बीते जब शम्मोजान लाज-शर्म छोड़कर पहली बार इन दीवारों के अन्दर बैठकर मुस्करा दी थी कि अब वह आज़ाद है| जिस आज़ादी को अभी-अभी मुन्नी ने अपनी बेसुरी आवाज़ में याद किया था, वह आज कितनी विकृत और कितनी कुरूप हो चुकी है,यह आज उसे भूला नहीं|’ ‘दादी अम्मा’, ‘अभी उसी दिन ही तो’ कहानियां परिवारों में अधिकार छीन जाने के बाद सास और दादी बन जाने वाली स्त्रियों के आहत अभिमान की मार्मिक गाथा है| ये कहानियाँ चरमराते संयुक्त परिवारों की कहानियां हैं |
विभाजन की त्रासदी की मारक और प्रामाणिक कहानियाँ ‘सिक्का बदल गया’, ‘मेरी माँ कहाँ ..,’ ‘डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा’ हैं| इस सन्दर्भ में वे कहती हैं कि , “विभाजन एक ऐसे ऐतिहासिक विघटन की मानवीय स्मृति है जिसे भूलना नामुमकिन है याद रखना खतरनाक|”(कृष्णा सोबती,सोबती-वैद सम्वाद,लेखन और लेखक) ‘मेरी माँ कहाँ..’ की दहशत मंटो की इस थीम पर लिखी कहानियों की याद दिलाती है| सोबती की इन कहानियों की सबसे बड़ी विशेषता है, दोनों कौमों में व्याप्त नफरत, हिंसा, डर, अविश्वास और इन सबके बीच छलनी होती मानवता के बीच से ही फूटता इंसानियत का छोटा सा उत्स| ये उनका भरोसा था जो कायम रहा|
कृष्णा सोबती की कहानियों और उपन्यासों की एक अन्य बड़ी विशेषता है उनकी भाषा| जो उन्हें बाकी अन्य लेखकों से विशिष्ट बनाती है| वह कहती हैं, “भाषा सिर्फ वो नहीं जिसे हम लिखित में पढ़ते-लिखते हैं, संवाद में बोलते हैं, भाषा वह भी है जिसे हम जीते हैं|”( सोबती-वैद संवाद)
वस्तुत: कृष्णा सोबती की कहानियों में जीवन की चेतना है| ये कहानियां उनके समय और परिवेश का व्यापक वितान हैं, बल्कि इन्हें लगभग आधी शताब्दी का दस्तावेज़ कहा जा सकता हैं| ये कहानियां सोद्देश्यता को लेकर नहीं रची गईं बल्कि ये उनके रचनात्मक ,सजग लेखक मन की उपज हैं जो अपने समय को शब्दों का जामा पहनाकर खुद ब खुद सार्थक रूप लेती गयी| सोबती मानती हैं कि, ‘वो ऐसे ही लिखने के लिए नहीं बैठ पातीं जब कोई घटना, वस्तु, विचार आंदोलित करता है, जब वो उसे अपने अंदर आत्मसात करती हैं तब किसी रचना का जन्म होता है. उस कृति के साथ उनका निजी आत्मिक सम्बन्ध बन जाता है|’ ‘नई कहानी’ आन्दोलन में कृष्णा सोबती अकेली कहानीकार हैं जिन्होंने इतनी कम कहानियां लिखकर अपनी विशेष पहचान बनाई है. उनकी प्रतिनिधि कहानियों का संग्रह बादलों के घेरे सन ८० में प्रकाशित हुआ. अपने कम लिखने के कारणों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने एक साक्षात्कार में कहा है, ‘मुझ में एक गहरा ठंडापन है. कभी-कभार लिखने बैठ ही जाती हूँ तो वह मेरे निकट समूची प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है. कुछ भी लिखना मेरे निकट समूची प्रक्रिया का एक अंग बन जाता है. कुछ भी लिखना मेरे निकट एक गम्भीर और जोखिम भरी स्थिति बन जाती है इसीलिए मैं अपने लेखक को कभी पटाती नहीं. दांव पर नहीं लगाती. अपने से हटकर मैं उसे दूसरा व्यक्ति समझती हूँ और उसकी इज्ज़त करती हूँ…(सारिका ,जनवरी ’७९ पृष्ठ 9) ‘नई कहानी के बेहद आत्मपरकता वाले दौर में लेखक और भोक्ता के बीच की यह दूरी किसी हद तक आश्चर्यजनक लग सकती है| ऐसा नहीं है कि कृष्णा सोबती के अपने अनुभव और आग्रह उनकी कहानियों में न हों,लेकिन उनके जीवन-प्रसंगों में प्रवेश की वैसी छूट नहीं मिलाती जैसी उस दौर के अन्य बहुत से लेखकों के साथ मिलाती है| उनकी कहानियां उनके अनुभवों का ताप संजोए रखकर भी उन्हें आत्मवृत्तांत के रूप में लिए जाने की छूट प्राय: नहीं देती|’(हिन्दी कहानी का विकास ,मधुरेश पृष्ठ102-103) तभी स्त्री विमर्श पर बेहद प्रमाणिक लेखन करने वाली सोबती कहती हैं कि , “लेखन तुक्कों की मार नहीं ,लेखक होना एक पूरी तालीम है| लेखक के पास लेखक का अनुभव संसार है| अपने अंदर की बाहर की स्थितियों को और अपने को पढने की जीवन दृष्टि|”
डॉ. अनुराधा गुप्ता
कमला नेहरु कॉलेज ,हिन्दी विभाग
9968253219
………………
श्रंखला की एक और कड़ी का अवसान
15 नवम्बर 2021, की दोपहर हिन्दी जगत के एक जाने-माने सम्पादक द्वारा मिली प्रिय लेखिका मन्नू भंडारी के निधन की ख़बर ने भागते समय को मानो थाम सा लिया| खबर के स्रोत पर संदेह का प्रश्न नहीं था बावज़ूद इसके आँखें हर जगह इस खबर की तस्दीक कर रहीं थीं, एक उम्मीद के साथ कि शायद यह अफ़वाह हो| किन्तु खबर सच थी, इसे न स्वीकार करना अपने को भुलावा देने के अलावा और कुछ न था| मन्नू जी के निधन की खबर थोड़ी ही देर में सोशल मीडिया के लगभग सभी प्लेटफॉर्म में फ्लैश होने लगी| हर कोई अपनी प्रिय कथा लेखिका के न रहने की दुखद खबर से संतप्त था| मिरांडा हाउस की अपराजिता शर्मा के गुजरने के बाद मेरे लिए यह दूसरी बेहद दुखद ख़बर थी| बहुत कम लोग होते हैं जिनका जाना एक गहरी ख़लिश और उदासी छोड़ जाता है| मन्नू जी का जाना ऐसा ही था…जैसे एक वैक्यूम ..जिसे कभी न भरा जा सके, जिससे अंजाने ही आँखें और मन दोनों भर आएं| अपराजिता जहाँ लगभग 40 की उम्र में, अपनी रचनात्मकता के उठान पर, इस दुनिया को छोड़ चली गईं, वहीं मन्नू जी 90 वर्ष की अवस्था में एक भरा-पूरा जीवन जी कर अपने पीछे रचनात्मकता की बेहद समृद्ध दुनिया छोड़ कर गईं थीं किन्तु ‘जाना’ सिर्फ एक क्रिया नहीं है, मन एक ऐसी गहरी नौस्टेलियाजिक उदासी से घिर गया जिससे बाहर आना मेरे और उनके तमाम पाठकों के लिए फिलहाल सम्भव नहीं| कौन कह सकता है कि साहित्य और सिनेमा महज एक कला, फिक्शन और मनोरंजन की दुनिया है! जीवन से जुड़ी ये विधाएं यदि मन्नू जी जैसे लेखक द्वारा रची जा रहीं हों तो वो जीवन ही हो जाती हैं…एक दूसरे के समानांतर, एक-दूसरे में डूबती-उतराती, एक-दूसरे से भिन्न-अभिन्न दुनिया|
सोचती हूँ वो ऐसी क्या बात है जो मन्नू भंडारी को ‘मन्नू भंडारी’ बनाती है, ऐसा क्या ख़ास था कि हर आम और ख़ास पाठक के लिए वो उसकी अपनी निजी ‘मन्नू भंडारी’ हो जातीं हैं, उनकी लगभग हर रचना का रसास्वादन और उससे एक ख़ास तरह का जुड़ाव सामजिक कैसे और क्यों महसूस करता होगा! इस ओर जब देखती हूँ तो इसके पीछे मुझे सबसे बड़ी वज़ह दिखती उनकी अपनी विशिष्ट रचनात्मक दृष्टि व शैली; जिसका उत्स उनका निजी जीवन अनुभव व वह मर्मभेदी दृष्टि और सम्वेदना है जो एक स्त्री के रूप में उन्हें प्रकृति प्रदत्त थी, इसके संयोजन से उनकी लेखकीय प्रतिभा समाज की उन अदृश्य भीतरी पर्तों को छील सकी जिसमें सदियों के जड़ संस्कार, आधी आबादी का अमूर्त-अनकहा शोषण, भीषण अन्तर्द्वन्द, उदासी, अँधेरा और गहरी चुप्पी व्याप्त थी| उनकी कितनी ही रचनाएं इस बात की हामी हैं कि स्त्री में धरती जैसा धैर्य हो सकता है, लेकिन उसी सीमा तक जब तक उसका अपना ‘स्व’ और ‘स्वाभिमान’ आहत न हो|
उन्होंने बदलते समय की नब्ज़ को बड़ी बारीकी से पकड़ा, उन तनावों और द्वंदों को, जो करवट लेते समय में खदबदा रहे थे, इतनी सहजता से वाणी दी कि लगा, हाँ! ये बिल्कुल वही था, बिल्कुल वैसा ही, जिसे अब कहा गया.. जो अभी तक अनकहा था; ‘आपका बंटी’, ‘महाभोज’, ‘यही सच है’, ‘मुक्ति’, ‘त्रिशंकु’, ‘सयानी बुआ’, ‘अकेली’, ‘स्त्री सुबोधिनी’, ‘एक प्लेट सैलाब’, ‘एक इंच मुस्कान’, ‘स्वामी’, ‘एक कहानी यह भी’(आत्मकथा जिसे उपन्यास भी माना जाता है) जैसी अनेक कहानियाँ व उपन्यास अपने चुने गए विषय, कथानक और ट्रीटमेंट के कारण हिन्दी कथा साहित्य में सर्वथा अलहदा स्थान रखते हैं| यहाँ किसी भी प्रकार की न लिजलिजी भावुकता है न कृत्रिम क्रांति की आँधी| ‘यही सच है’ की नायिका का प्रेम के चुनाव को लेकर नैतिकता-अनैतिकता से परे निर्द्वन्द आचरण, ‘आपका बंटी’ की नायिका का मातृत्व और व्यक्तित्व को लेकर गहरा द्वन्द, ‘स्त्री-सुबोधिनी’ की नायिका का पुरुष प्रेम के भावनात्मक छल जाल से स्त्री प्रजाति को चेतावनी, ‘मुक्ति’ की अम्मा का मरते पति के प्रति ‘अनक्रेडिटेबल’ सेवा- भक्ति और मरने वाले पति की अपेक्षा बेथक निरंतर सेवा करने वाली पत्नी के बीच मुक्ति के प्रश्न , ‘एखाने आकाश नाईं’, ‘सयानी बुआ’ और ‘अकेली’ आदि कथा जगत के स्त्री चरित्र.. क्या तमाम भारतीय परिवेश की स्त्रियों के आत्म और बाह्य जगत के अनछुए पहलुओं का चलचित्र सामने नहीं रख देते! दरअसल ये वे भाव और चरित्र हैं जो पहली बार हिन्दी कथा जगत में अपने ‘वर्जिन’ रूप में सामने आए थे| ६० के दशक के बाद का पाठक एक नई दुनिया से परिचित हो रहा था|
इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं कि मन्नू भंडारी स्त्री अस्मिता-चेतना-मन की सबसे सशक्त लेखिका थीं और हैं| आज भी उनकी कहानियां स्त्री विमर्श की सशक्त और आधारभूत तत्वों की सबसे प्रबल पैरोकार हैं| मन्नू जी के लेखन में एक अलग तरह की ताजगी दिखती है जो उनके लेखन को सर्वथा नई ऊर्जा ही नहीं मौलिकता, ईमानदार- सहज और सशक्त अभिव्यक्ति के साथ ‘साधारण’ के प्रति अतिरिक्त समर्पित बनाता है| मन्नू जी के लेखन की सहजता उनके लेखन की विशिष्टता का सबसे बड़ा कारण है| अपने चारों तरफ़ बड़े-बड़े नामी लेखकों/संगठनों की उपस्थिति के बावज़ूद उनकी रचनाओं पर किसी अन्य की छाया,प्रभाव, आग्रह/दुराग्रह दिखाई नहीं देता| तमाम तरह के पूर्वाग्रहों, विचारधाराओं, बौद्धिकता के अतिरेक से सर्वथा मुक्त ..एक स्वच्छन्द राह की अन्वेषी| मन्नू जी अपने एक साक्षात्कार में कहती हैं, “ जहाँ तक किसी लेखक के प्रभाव पड़ने की बात है, मुझे आश्चर्य है कि किसी एक व्यक्ति का नाम मैं नहीं ले सकूंगी| मुझे किसी एक व्यक्ति की कोई रचना अच्छी लगी, किसी की कोई एक| पर ये नहीं कह सकती कि किसी एक व्यक्ति का, उसके लेखन का मेरे लेखन पर प्रभाव पड़ा| न देशी, न विदेशी| बहुत ईमानदारी से कहूं कि विदेशी साहित्य मैंने पढ़ा ही बहुत कम है| पर जो भी पढ़ा | जहाँ तक विचारधारा की बात है, अब जाके चाहे मैं महसूस करूं कि शायद मार्क्सवाद का प्रभाव हो, किन्तु है नहीं, मेरी जो विचारधारा है, जो जुड़ाव है, वो ज़िंदगी के साथ है, न किसी विचारधारा, न किसी व्यक्ति| ज़िंदगी को नंगी आँखों से देखा और जैसा देखा, जो महसूस किया, ज़िंदगी के साथ जुड़कर उसको ही अपनी कहानी में अभिव्यक्ति दी|”
मन्नू जी के पास ‘ज़िन्दगी को नंगी आँखों से देखने के बाद जो ज़िन्दगी से जुड़ाव की अभिव्यक्ति’ है, उसने उन्हें एक ख़ास तरह का ‘पॉवर बैंक’ दिया, जिसकी वज़ह से न जाने कितने जीवंत चरित्र रचे गए जो आज भी वे अपनी सम्पूर्ण अस्तित्व के साथ हमारे बीच मौज़ूद हैं| ख़ास तौर पर मन्नू भंडारी द्वारा रची जाती स्त्री व स्त्री-पुरुष के आत्मीय व दुनियावी रिश्तों में स्त्री की अवस्थिति; अपने पूरे वितान में स्त्री अस्तित्व और उसकी चेतना की ऐसी सजीव दुनिया है जो ६० के दशक की भारत के महानगरीय मध्यवर्ग की स्त्री का एक पूरा कोलाज सामने उपस्थित कर देती है| आधी शताब्दी से अधिक समय गुजरने के बाद भी ‘शकुन’, ‘बंटी’, (आपका बंटी)‘दीपा’(यही सच है) ‘अम्मा’(मुक्ति), ‘तनु’, ‘मम्मी’(त्रिशंकु) ‘मैं’,’शिंदे’ (स्त्री सुबोधिनी) ‘कैफे हॉउस के पात्र (एक प्लेट सैलाब), ‘बुआ’ (सयानी बुआ), ‘सोमा बुआ’ (अकेली), ‘बिसेसर’, ‘दा साहब’, ‘बिंदा’ (महाभोज) ‘रजनी’ (दूरदर्शन के लिए लिखा गया धारावाहिक) जैसे पात्र आज भी अपने पूरे वजूद के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं|
उनके कथा जगत और कथेतर साहित्य से गुजरते हुए यह बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकती हूँ कि उनके द्वारा रचित ‘स्त्री विमर्श’ का ऐसा अघोषित और सशक्त चित्रण पूरे हिन्दी जगत में अपने आप में अकेला है| मन्नू भंडारी की स्त्री हाड़-माँस की बनी ऐसी चेतन सम्पन्न, बौद्धिक व सम्वेदनशील स्त्री है, जो बिना किसी शोर अथवा आरोपित या आयातित विमर्श के, अपनी धरती से पैर टिकाए आसमान की सीमा तक पहुँचने का प्रयास करती है| यह स्त्री मन्नू भंडारी के जीवनानुभव की उपज है जहाँ कभी-कभी संतुलन बनाए रखना उसके लिए ज़रूरी होता है किन्तु अपने ‘स्व’ और स्वाभिमान की कीमत पर नहीं| उनकी आत्मकथा मानी जाने वाली ‘एक कहानी यह भी’ उनके इसी स्त्री रूप की यात्रा है| मेधावी आलोचक गरिमा श्रीवास्तव ने मन्नू भंडारी के निधन के बाद श्रद्धांजलि स्वरुप लिखे अपने एक लेख में इस संतुलन को लेकर उनकी इस रचना के माध्यम से कई प्रश्नों को उठाया है| उनके भीतर मन्नू जी की वह ग्रन्थि भीषण प्रश्नाकुलता और रहस्य को जन्म देती है, जिनकी वजह से वो अपने वैवाहिक स्टेटस को बचाने के लिए अंत तक प्रयासरत रहती हैं| गरिमा जी इसे मन्नू भंडारी के सामन्ती- सवर्ण संस्कार, पिता की इच्छा के विरुद्ध जाकर विवाह करने के अपने फैसले को उनके सामने गलत ठहरते हुए देखने का भय और हीनता बोध, अपने रूप-रंग को लेकर कॉम्प्लैक्स आदि वज़हों को मानती हैं; जिनकी वज़ह से मन्नू भंडारी जैसी सशक्त मेधावी लेखिका पति और गृहस्थी को बचाने और संतुलन बनाने के भीषण मकड़जाल में फँसती चली गयी, “ प्रेम के विश्वासघात को स्त्री आजीवन नहीं भूलती|..उसके भीतर एक पितृसत्तात्मक व्यवस्था में पली-बढ़ी संस्कारित स्त्री बैठी है, जो पुरुष के अभाव की कल्पना से भी डरती है|कभी बच्ची टिंकू के लिए, तो कभी दुनिया क्या कहेगी और सबसे ज्यादा अपने लिए जो पति की ज्यादतियों पर जितना चाहे रो गा ले, लौट आती है फिर उसी खूंटे पर, न लिख पाने के कारणों में वह घरेलू व्यस्तताओं, स्वास्थ संबंधी समस्याओं, पति की उपेक्षा और संकट के समय पत्नी को छोड़कर अपने सुख मनोरंजन की तरफ ध्यान देने को प्रमुख मानती हैं जबकि आत्मोत्सर्ग के पीछे सामन्ती मूल्य संरचना वाले समाज में पोषित उनकी मानसिकता को देखा जाना चाहिए…यह पुरुषसत्तात्मक दृष्टिकोण ही है कि वह अपने जीवन के पैंतीस वर्ष कलपते हुए काट देती है, लेकिन अपने को इस बंधन से मुक्त नहीं कर पाती|”- गरिमा श्रीवास्तव, स्मृतिशेष: मन्नू भंडारी, बिछड़े सभी बारी-बारी, समालोचन : अरुण देव, 16 नवम्बर 2021
गरिमा जी द्वारा इंगित मन्नू जी के जीवन की यह विसंगति और पीड़ा मन्नू जी के लेखन और बातचीत में कई बार छलक पड़ती है| एक बेहद प्रतिभाशाली स्त्री कैसे तमाम द्वंदों और तनाव में जीती, पति की तमाम जाहिर और छिपी ज्यादतियों को सहनशीलता की हद तक बर्दाश्त कर अन्तत: विवाह के ३५ वर्ष बाद रिश्ते से मुक्त होने अथवा मुक्त करने का सफ़ल-असफ़ल उपक्रम करती है| रिश्ते को बचाए और बनाए रखने की जद्दोज़हद निश्चित ही उसके लिए एक भीषण द्वन्द है| एक आज़ाद ख़याल, आत्मनिर्भर, सचेतन स्त्री जो भारतीय परिवेश और उसकी जड़ों से गहरे जुड़ी है, जहाँ परिवार तथा वैवाहिक रिश्ते को बचाने के पीछे सबसे अधिक जोर उसके एक माँ होने के कारण है| ‘आपका बंटी’ इस द्वंद और विघटित परिवारों में बच्चों के त्रासद मनोविज्ञान का सशक्त उदाहरण है| वस्तुत: यह एक बेहद सम्वेदनशील स्त्री की पीड़ा है, जहाँ रिश्तों में समझौता और सामंजस्य की कोशिश उसकी कमजोरी नहीं..बल्कि वो प्रवृत्ति व नियति है, जहाँ वह कुछ भी बिखरने नहीं देना चाहती| किन्तु ‘अपना’ सब कुछ समेट लेने की कोशिशों में कहीं वह ख़ुद न सिमट जाए, इसके लिए वो बराबर चिंतित रहती हैं, तभी मन्नू जी कहती हैं, ‘सम्बन्ध को निभाने की ख़ातिर अपने को ख़त्म कर देने से अच्छा है कि सम्बन्ध को खत्म कर दो|”(आपका बंटी)
वो पुरुष की मक्कारियों को बखूबी समझती हैं, इसलिए ‘स्त्री सुबोधिनी’ जैसी सीख परक कहानियों में ही नहीं अन्य जगह मौक़ा मिलते ही अपनी हमजात को सावधान करती चलती हैं| “ इस देश में प्रेम के बीच मन और शरीर की ‘पवित्र भूमि’ में नहीं, ठेठ घर-परिवार की उपजाऊ भूमि से ही फलते-फूलते हैं. भूलकर भी शादीशुदा आदमी के प्रेम में मत पड़िए. ‘दिव्य’ और ‘महान प्रेम’ की खातिर बीवी-बच्चों को दाँव पर लगाने वाले प्रेम-वीरों की यहाँ पैदावार ही नहीं होती. दो नावों पर पैर रखकर चलनेवाले ‘शूरवीर’ जरूर सरेआम मिल जाएंगे. हाँ, शादीशुदा औरतें चाहें, तो भले ही शादीशुदा आदमी से प्रेम कर लें. जब तक चाहा प्रेम किया, मन भर गया तो लौटकर अपने खूंटे पर. न कोई डर, न घोटाला, जब प्रेम में लगा हो शादी का ताला|” (‘स्त्री-सुबोधिनी’)
‘मी टू’ अभियान के दौरान उनके द्वारा लिखे एक लेख ‘करतूते मरदां’ का यह एक बेहद मशहूर सीख बतौर उदाहरण देखिए- ‘ हर बात पर गदगद होकर बिछ जाने को तैयार बैठी नासमझ(मूर्ख) लड़कियों, औरतों से कहना है कि देखो, अगर किसी गीतकार के गीत पसंद आ जाएं तो मज़मे में बैठ कर सराह लो, कोई अच्छी फिल्म देखनी हो तो हॉल में देख लो या घर में टी वी पर, कहानी पत्रिका उपन्यास किताब में पढ़कर ही प्रसन्न हो लो बस, इसके आगे कभी मत बढ़ना| इनको रचने वालों के पास तो कभी मत जाना और बहुत घेराबंदी करने पर अपने पास तो बिलकुल फटकने मत देना|…भरोसे की जात बिल्कुल नहीं है, इनकी!” मन्नू जी के लेखन में स्त्रियों के लिए आत्मीयता और ममत्व इतना अधिक है कि उनकी किसी भी रचना में स्त्री स्त्री की दुश्मन कभी नहीं दिखती| एक इंटरव्यू में उनके प्रिय धारावाहिक के विषय में पूछे जाने पर वो कहती भी हैं कि अव्वल तो उन्होंने टी वी देखना बंद कर दिया, दूसरे उन्हें नए दौर के धारावाहिकों से इस बात के कारण सख्त ऐतराज़ है कि उसमें एक खलनायिका ज़रूर होती है|
मन्नू भंडारी की पहली कहानी सन 55-56 में ‘कहानी’ पत्रिका में प्रकाशित हुई, जिसके सम्पादक उस समय भैरव गुप्त थे| उस के बारे में याद करते हुए अपने एक साक्षात्कार में वो कहती हैं कि ‘इस पत्रिका में अपनी पहली कहानी चोरी-छिपे इसलिए दी थी कि शायद ही कोई इसकी सुध ले| लेकिन दो-तीन महीने बाद जब भैरव प्रसाद गुप्त का स्वीकृति पत्र ही नहीं मिला बल्कि उसमें उसकी प्रशंसा भी थी, तो वो खुशी जो उन्हें उस समय मिली ऐसी खुशी फिर कभी नहीं मिली, भले ही जीवन में खुशी के कई अवसर आए|’ यह स्मृति बयाँ करते हुए उनकी तरल आँखों और स्निग्ध चेहरे की पुलक और चमक साफ़ महसूस की जा सकती है| उनकी पुस्तक ‘एक कहानी यह भी’ के कई अंश, उनसे बातचीत के कई हिस्से पढ़ते/देखते हुए कुछ आलोचक उनमें किंचित आत्मविश्वास की कमी मानते हैं, जिसके कारण प्रखर प्रतिभाशाली होने के बावज़ूद वो उसे न बहुत स्वीकार कर सकीं न लेखकीय समाज में वे उतना उभर सकीं जितना उनसे कम प्रतिभाशाली उनके कुछ अन्य समकालीन| मेरी समझ से मामला उनके आत्मविश्वास या हीन भावना का न होकर, उनके व्यक्तित्व की अति सहजता और सौम्यता है, जिसकी वज़ह से वे उन मंचों पर भी कई बार असहज हो जातीं थीं जब उनके परिचय में कई तरह के विशेषण जोड़ दिए जाते थे| उनकी सहजता ही थी जिसके कारण वो आज भी उतनी ही लोकप्रिय, बहुपठित व प्रासंगिक लेखिका हैं, जितनी वो साठ व साठोत्तर दशक में रहीं| ये उनकी विशिष्टता ही है कि वो तकरीबन तीन पीढ़ियों में समान समादृत और पसंदीदा रहीं हैं|
मन्नू जी के लेखन का केंद्र ६० के दशक की एक ऐसी महानगरीय मध्यवर्ग की दुनिया थी, जो बेहद व्यापक स्तर पर संक्रमण काल से गुजर रही थी, जिसकी सामाजिक- पारिवारिक-मनोवैज्ञानिक संरचना सर्वाधिक जटिल और आकर्षक थी| ये हिन्दी साहित्य में नयी कहानी आन्दोलन का दौर था| कह सकते हैं रचनात्मकता की दृष्टि से स्वातन्त्र्योत्तर भारत के हिन्दी कथा जगत का यह स्वर्णिम युग था| जब पुरानी पीढ़ी का नए दौर की माँग के साथ तालमेल गड़बड़ाने लगा, तब मौलिक रचनात्मकता, युवा ऊर्जा और प्रखर प्रतिभा से भरी एक बेहद सम्भावनाशील सशक्त युवा पीढ़ी अपने समय को मुखर करती सामने आती है| बड़ी संख्या में रचनाकारों और उनकी एक से एक बढ़कर नयी रचनाओं का आना कथा लेखन में पुरानी पीढ़ी के चुक जाने के उद्घोष के समान था| जहाँ एक तरफ़ फणीश्वर नाथ रेणु, भीष्म साहनी, अमरकांत, निर्मल वर्मा, शेखर जोशी, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेन्द्र यादव जैसे लेखक ‘भोगे हुए यथार्थ’ की अभिव्यक्ति में अपनी मुहर लगा रहा था वहीं 55 के बाद का हिन्दी कथा साहित्य का पटल अन्य सशक्त लेखिकाओं के साथ ‘स्त्री त्रयी’ की रचनात्मक ऊर्जा के विस्फोट का गवाह भी बनता है, ये त्रयी थी ‘कृष्णा सोबती’, ‘मन्नू भंडारी’ और ‘उषा प्रियम्वदा’ की| ये अलग बात है कि ‘नयी कहानी’ आन्दोलन का बड़ी चालाकी से सारा श्रेय ‘पुरुष त्रयी’ द्वारा ले लिया गया| साहित्य की इन चालाक तिकड़मों का भान स्वयं मन्नू जी के कई लेखों, साक्षात्कारों और अप्रत्यक्ष रूप से उनके कथा संसार से हो जाता है| ‘तहलका’ में 7 जनवरी 2014 में छपे उनके एक लेख ‘कितने कमलेश्वर!’ इसकी सशक्त बानगी है|
एक लेखक अथवा कलाकार के साथ किसी सहृदय पाठक अथवा सामजिक का बेहद निजी रिश्ता होता है| उसका उससे तादात्मीयकरण, आत्मीयता की गहराई, लेखक की छवि के उसके लिए मायने कितने अलहदा और निजी हो सकते हैं, इस बात को किसी दूसरे के सामने व्यक्त कर पाना कई बार बेहद मुश्किल होता है. मेरे लिए मन्नू भंडारी लेखिका के रूप में उस ताले की चाभी की तरह हैं, जिसका इस्तेमाल कर मुझ 18 वर्ष की एक कस्बाई लड़की के सामने महानगरीय- मध्यवर्गीय दुनिया और उसकी आधुनिक स्त्री की बाह्य व अन्तरंग की वृहद दुनिया बेहद करीब से खुलती है| यह महज संयोग नहीं कि उस समय (नब्बे के दशक के बाद) की साहित्यक दुनिया के बड़े- बड़े स्थापित व चर्चित उपन्यास मेरे भीतर वो पाठकीय रस और तादात्म्य पैदा नहीं कर सके जो मन्नू भंडारी का ‘आपका बंटी’ और उषा प्रियम्वदा के ‘रुकोगी नहीं राधिका’ ने किया| क्या इसके लिए मेरी यह अनुभूतिपरक गवाही काफ़ी नहीं होगी कि बहुत कुछ विस्मृत होने के बाद बची हुई स्मृतियों में मुझे कॉलेज की लायब्रेरी में रखी इन दोनों पुस्तकों की जगह और पुस्तक की तस्वीर अभी भी साफ़-साफ़ याद है| सही-सही कैसे बताया जा सकता है कि मेरी चेतना के विकास में उनकी रचनाओं का कितना दाय है!
मन्नू जी के निधन उपरांत उन्हें याद करते हुए एक बातचीत में हिन्दी के जाने माने लेखक योगेन्द्र आहूजा जी जिस तरह मन्नू जी की कहानी और उस पर बनी फिल्म ‘रजनीगन्धा’ की भावपूर्ण ढंग से चर्चा कर रहे थे, राजकमल प्रकाशन द्वारा आयोजित मन्नू जी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने हेतु एक कार्यक्रम में जिस तरह जाने-माने पत्रकार दिनेश श्रीनेत उनकी इसी कहानी और फिल्म को याद कर रहे थे, ये सब अनायास नहीं…न ये भाव, न श्रद्धा, न नोस्टाल्जिया…यह सब अपने लेखक के प्रति पाठक का विशुद्ध प्रेम है ..अनायास, बेहद अन्तरंग, बेहद निजी, निःस्वार्थ व उदात्त| यदि ऐसा न हो तो तजाकिस्तान जैसे सुदूर मुल्क से एक व्यक्ति सिर्फ अपनी लेखिका को देखने और मिलने देर रात न आता| जहाँ हिन्दी भाषा के तमाम लेखकों में से वो उन्हीं को पढ़ता और जानता था| (उक्त किस्से की जानकारी हिन्दी के जाने-माने लेखक ओमा शर्मा जी से प्राप्त हुई|)
३ अप्रैल 1931 को म.प्र. के भानपुरा गाँव में जन्मी मन्नू भंडारी का जीवन एक लम्बी यात्रा कर नवम्बर २०२१ को विश्राम लेता है| एक लम्बा वक्त …जिसने उनके व्यक्तित्व में कई भिन्न, विरोधी, अनुकूल-प्रतिकूल अनुभवों का इज़ाफा किया| गुलाम भारत से आज़ाद भारत की तस्वीर और आज़ादी के आंदोलनों में शिरकत, पिता की बेहद स्वाभिमानी, कुछ दम्भी व पितृसत्तात्मक सोच और माँ का बेपढ़, व्यक्तित्वहीन, धरती के जैसा धैर्यवान अस्तित्व, अजमेर,कलकत्ता और फिर अंत तक दिल्ली तक की यात्रा के अनुभव, एक लेखक की पत्नी, वैवाहिक रिश्तों के तनाव, मातृत्व और व्यक्तित्व की कशमकश, गृहणी,कामकाजी और लेखिकीय पेशे के बीच का द्वंद…कितना कुछ है जो उन्हें बनाता है| मृत्यु सत्य है| मन्नू जी का भी इहलोक को छोड़कर जाना तय था, वो चलीं गई, एक ऐसी दुनिया में जहाँ से उसी रूप में कोई वापस नहीं आता| बस पीछे छूट गई उनकी खुशबू …जो तब तक रहेगी, जब तक हम मनुष्यों में उसकी चेतना और सम्वेदना शेष है|
लेख-
अनुराधा गुप्ता, सहायक प्रवक्ता कमला नेहरु कॉलेज, दिल्ली विश्विद्यालय, नई दिल्ली
E mail- anuradha2012@gmail.com
………………