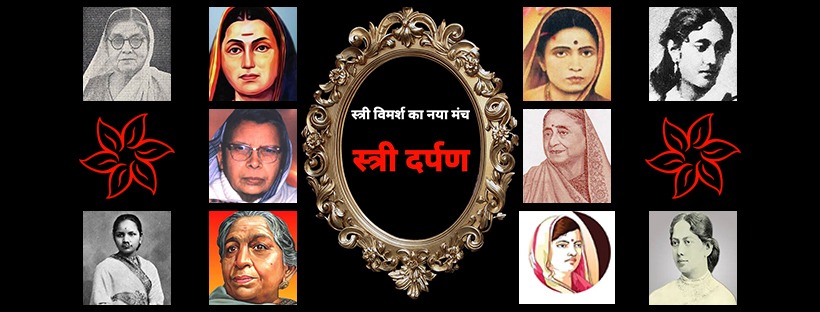गीता दूबे
जन्म : उत्तर प्रदेश के एक गांव में
शिक्षा : एम. ए. पी. एच. डी. ( कलकत्ता विश्वविद्यालय )
पुस्तकें :
1. हिंदी साहित्येर पंच पथिक ( बांग्ला, सहलेखन ) 2004
2. स्त्री लेखन : स्त्री दृष्टि ( सह संपादन ) 2014
3. करोना काल में हमारा साहित्यिक सफर, (ई बुक,संपादक मंडल) 2021
4. ऐ सखी सुन (ई बुक, समसामयिक एवं स्त्री मुद्दों पर केंद्रित) 2021
5. विस्मृत नायिकाएं (ई बुक, 2022)
6. मधुपुर आबाद रहे (कविता संग्रह) 2022
विभिन्न पत्र- पत्रिकाओं में कविताएं, आलेख, समीक्षाएं, शोध पत्र आदि प्रकाशित।
ऑनलाइन पत्रिकाओं में आलेख एवं समीक्षाएं प्रकाशित।
विभिन्न संगोष्ठियों का संयोजन, संचालन व शोध पत्रों का पाठ सहित सक्रिय भागीदारी
रेडियो, दूरदर्शन पर कविता पाठ व परिचर्चा में शामिल
“साहित्यिकी” संस्था की पूर्व सचिव
साहित्यिकी पत्रिका की पूर्व सह संपादक
संप्रति : स्कॉटिश चर्च महाविद्यालय के हिंदी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष (वर्तमान)
पता : पूजा अपार्टमेंट, फ्लैट संख्या ए 3, द्वितीय तल, 58 ए/1 प्रिंस गुलाम हुसैन शाह रोड, यादवपुर ,कोलकाता -700032
मोबाइल : 9883224358
मेल -dugeeta@gmail.com
…………
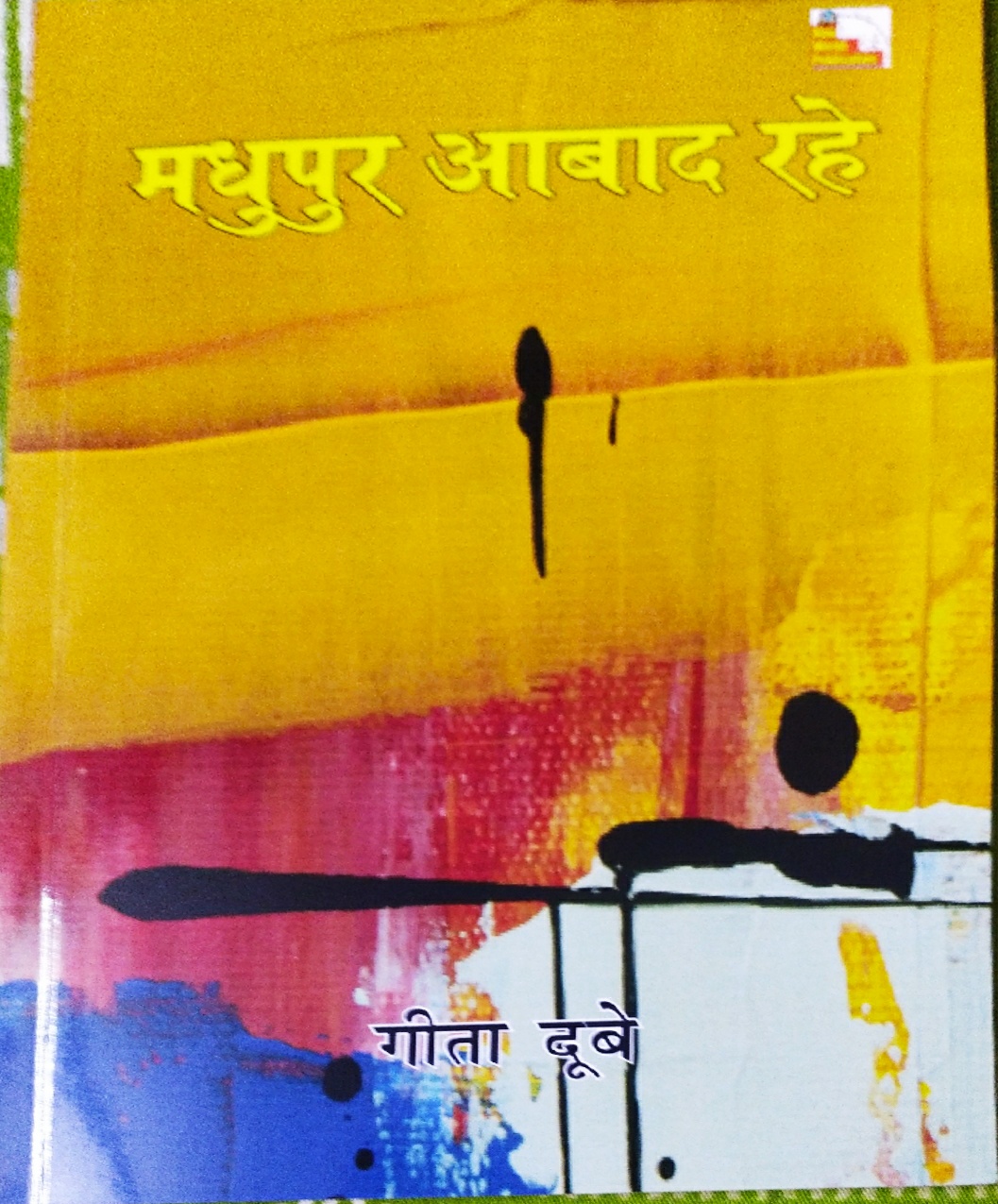
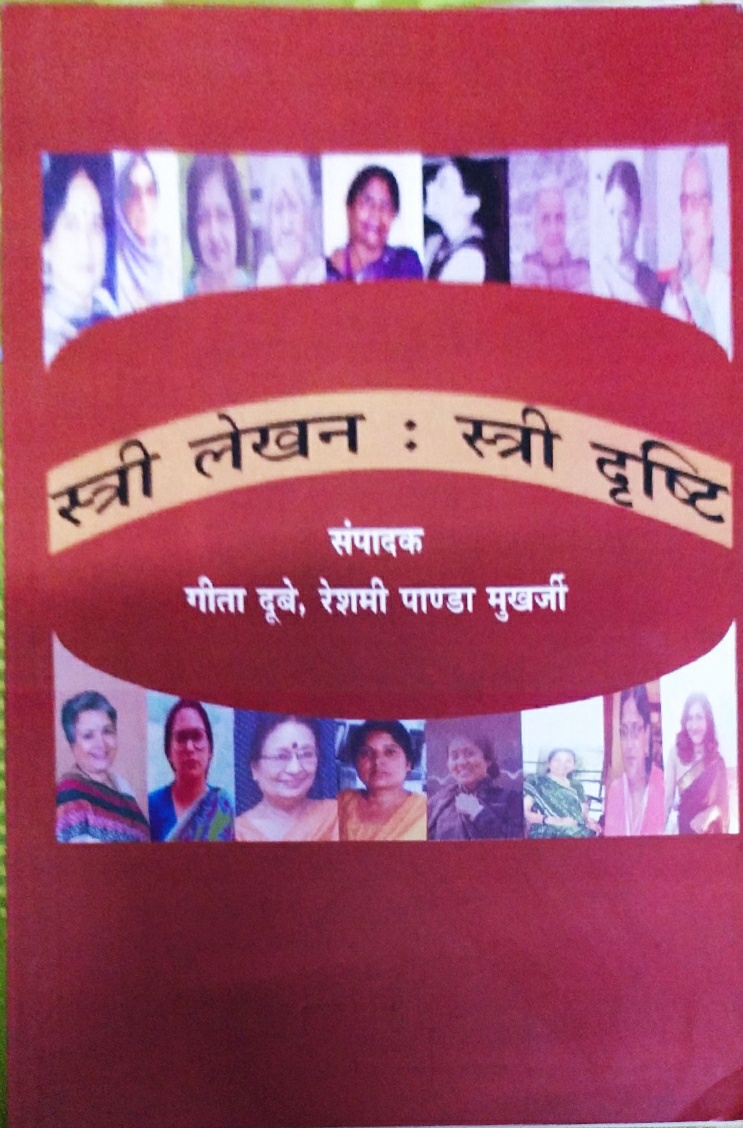
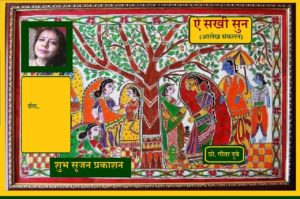
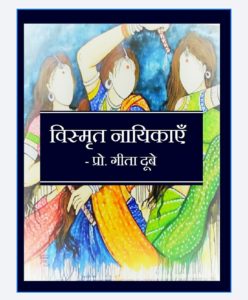
…………
बांग्ला की स्त्री आत्मकथाओं से झांकती मार्मिक जीवनानुभूतियाँ
गीता दूबे
स्त्री चाहे किसी भी देश या समाज की क्यों न हो, उसके पास अनुभवों का वह अनकहा खजाना होता है जिसके बारे में बहुधा हम अनुमान भर लगा सकते हैं। वह अपने भीतर दर्द का सैलाब समेटे, होठों पर मुस्कान सजाए, शोषण और प्रताड़ना का दर्द झेलती हुई भी निरंतर सृजनशील बने रहने का साहस करती है। यही साहस लेखिकाओं की रचनाओं और आत्मकथाओं में प्रतिभासित होता है ।
बांग्ला में सर्वप्रथम राससुंदरी दासी ने ‘आमार जीवोन ‘ ( 1876) लिखकर अपने निजी अनुभवों के माध्यम से तत्कालीन समाज में शोषण- चक्र में पिसती, घुटती स्त्रियों की कथा को समाज के सामने लाने का साहस किया। महज़ बारह वर्ष की उम्र में ब्याही गयी साधारण ग्रामवधू राससुंदरी ने तकरीबन छः वर्ष तक का वैवाहिक जीवन घूंघट तले बिताया। रसोईघर में छिपकर अक्षर मिला -मिलाकर पढ़ना सीखा और अंततः इतनी समर्थ हुईं कि अपनी कथा साहसपूर्वक कह पाईं जिनमें उनके दुखद जीवन प्रसंगों के साथ- साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता भी व्यक्त हुई है। समाज और परिवार के उन दबावों का मार्मिक चित्रण मिलता है जिसमें स्त्री का पढ़ना- लिखना अक्षम्य अपराध समझा जाता था। उन्होंने लिखा-” घर में कोई कागज पड़ा रहता था तो उसकी तरफ देखती भी नहीं थी कि कहीं लोग यह न कहे कि वह पढ़ रही है। प्रार्थना करती थी कि हे ईश्वर मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो।” इस आत्मकथा ने साहस और सृजन की जो चिंगारी सुलगाई उससे प्रेरित होकर अन्य महिलाओं ने भी अपने दर्द और संघर्ष को दुनिया के सामने लाने का साहस किया।
इसके बाद “आमार अतीत जीवन” (मान कुमारी बसु), “जनयिका (एकजनी) गृहवधूर डायरी”, “एकजन रमनीर इतिवृत्त”, “सेकालेर गृहवधूर डायरी”, “शिक्षिता, पतितार आत्मचरित” ( मनोदा देवी), “स्मृतिर खेया”( शहाना देवी), “आमादेर गृहे अंत:पुर: शिक्षा ओ ताहार संस्कार” (स्वर्ण कुमारी देवी, रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बहन), “सबारे आमि नमि” (कानन देवी), “स्मृतिचित्र” (प्रतिमा देवी), “मनीषा मन्दिरे” (कृष्णकुमारी गुप्त), “स्मृतिकथा” (ज्ञानदानंदिनी देवी) आदि रचनाओं ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। अभिनेत्री, कवयित्री विनोदिनी (नटी) दासी रचित ‘आमार कथा'(1912), देवी शरदसुंदरी दासी की ‘आत्मकथा” (1913), निस्तारिणी देवी की ‘सेकालेर कथा’ (1913), प्रसन्नमयी देवी रचित पूर्वकथा (1917) ,अमियबाला की ‘अमियबालार डायरी’ (1929), सुदक्षिणा सेन की ‘जीवनस्मृति ‘ (1932) आदि रचनाओं ने इस परंपरा को और भी समृद्ध किया। यह कारवां आगे बढ़ता गया और बांग्ला साहित्य को कई अविस्मरणीय आत्मकथाओं को सहेजने का गौरव प्राप्त हुआ। इनमें कुछ उल्लेखनीय नाम हैं- “कमबयसे आमि” (मानसी दासगुप्त, 1974) “जीवनेर झरा पाता” ( सरला देवी चौधुरानी, 1975 ) “छेलेबेलार दिनगुली” ( पूर्णलता चक्रवर्ती, 1980 ), “पूर्वस्मृति” (शांता देवी, 1983),”जेनाना फाटक” ( रानी चंद, 1987), “मंच ,परदा ओ जीवन कथाय सावित्री” (सावित्री चट्टोपाध्याय, 1992 ), “स्मृतिकथा” (कल्पना दत्त जोशी ,1992),”जीवनकथा” ( इंदिरा देवी चौधुरानी, 1993), “आमार जीवने स्वाधीनतार साध: चलार पथे” (इला मित्र, 1997) आदि । इनमें बंगाल की स्त्रियों की संघर्ष गाथा के साथ साथ उस समय का इतिहास भी वर्णित हुआ है।
1975 में प्रकाशित सरला देवी चौधुरानी (रवीन्द्रनाथ ठाकुर की बहन स्वर्ण कुमारी देवी की पुत्री) की आत्मकथा ‘जीवनेर झरापाता’ की चर्चा इसीलिए आवश्यक है क्योंकि यह एक शिक्षित बंग महिला की निजी अनुभूतियों की कथा मात्र न होकर बंगदेश की कथा भी है। उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दो और बीसवीं शताब्दी के प्रथम तीन दशकों अर्थात तकरीबन पचास वर्षों के इतिहास से यह पाठकों को परिचित कराती है। ‘देश’ में धारावाहिक रूप से छपते समय इसे काफी सराहा गया। ‘आनंदबाजार पत्रिका’ में छपा -” ऐसा लगता है कि ”रक्तकरबी’ ((रवीन्द्रनाथ का नाटक) की नंदिनी ने हाथों में कलम उठा ली है।”
कुछ लेखिकाओं की आत्मकथा में देश के राजनैतिक इतिहास के मार्मिक और प्रामाणिक चित्र पाठकों को उन ऐतिहासिक दस्तावेजों से रूबरू करवाते हैं जिनसे होकर ही हम समय की सही पड़ताल कर पाने में सक्षम हो पाएंगे। इनमें एक महत्वपूर्ण नाम है जहांआरा इमाम का, जिनकी आत्मकथा ‘एकात्तरेर दिनगुली” (1986) में बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध के कई दिल दहला देनेवाले अध्याय अंकित हैं। बांग्लादेशी मुक्तियोद्धा और शहीद के नाम से ख्यात जहांआरा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच 1971 में हुए खूनी संघर्ष की साक्षी ही नहीं रहीं बल्कि उसमें भाग भी लिया। बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध और उसके निर्माण के खूनी इतिहास को उन्होंने अपनी आत्मकथा में बड़े प्रामाणिकता से उकेरा है। उनके निजी जीवनानुभवों के साथ देश विभाजन के दौरान अपनी जड़ों से उखड़कर , टूटते- बिखरते परिवारों की भयावह त्रासदी को चित्रित करती यह पुस्तक पाठकों को झकझोर देती है। इसमें लेखिका के साथ उन हजार मांओं की कथा अंकित है जिन्होंने मुक्तियुद्ध में अपना सर्वस्व गंवा दिया।
बाल साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध एवं ‘गुपीर गुप्त खाता’, ‘टंगलिंग’, ‘हलदे पाखीर पाल’, ‘माथू’ इत्यादि चर्चित पुस्तकों की लेखिका लीला मजूमदार का नाम आत्मकथा लेखन के इतिहास में उल्लेखनीय है। विख्यात साहित्यकार उपेन्दर किशोर राय की वंशधर लीला विरचित ‘आर कोनखाने’ (1967) नामक संस्मराणत्मक आत्मकथा ने सहजता से साहित्यालोचकों को आकर्षित किया। रवीन्द्र पुरस्कार प्राप्त इस कृति में प्रकृतिप्रेमी रोमांटिक लेखिका के व्यक्तिगत जीवनानुभवों के साथ शिलांग का प्राकृतिक सौंदर्य खूबसूरती से उभरा है। इनका बचपन शिलांग में बीता था। वहाँ के निर्जन पहाड़ी सौन्दर्य का चित्रण उन्होंने अपनी आत्मकथा ‘पागडण्डी’ (1986) में भी किया। पहाड़ की गोद में बसे ,कांच की खिड़कियों से घिरे छोटे- छोटे घरों में बसनेवाले लोगों के जीवन को सुंदरता से दर्शाने के साथ वहाँ की कामकाजी खसिया औरतों, लड़कियों की खान -पान की आदतों , जीवन शैली, कर्मठता आदि का वर्णन भी उन्होंने विस्तार से किया है। ताऊ उपेन्द्र किशोर राय और भाई सुकुमार के कतिपय जीवन प्रसंगों को भी रोचकता के साथ कथा में पिरोया गया है।
प्रख्यात साहित्यकार प्रतिभा बसु के जीवन का आरंभिक दौर बांग्लादेश में बीता जहाँ वह गायिका रानू शोम के रूप में स्थापित हो चुकी थीं। विवाहोपरांत पति (बुद्धदेव बसु) के साथ बाकी जीवन कोलकाता में गुजारा। बांग्लादेश के मुक्तियुद्ध और विभाजन के त्रासद दृश्यों के साथ-साथ निजी जीवन के छोटे बड़े सुख -दुख की कथा बड़े प्रामाणिक रूप से प्रतिभा ने अपनी आत्मकथा “जीवनेर जलछवि” (1986) में कही है। विभाजन ने लोगों से उनकी जमीन और जहान ही नहीं छीना बल्कि बहुत से लोगों को अपनी पहचान तक से महरूम होना पड़ा। खोने के इस दर्द को प्रतिभा ने शिद्दत से महसूस किया था, निजी और सामाजिक जीवन, दोनों में। उनके जीवन के दोनों खंडों के चित्रण में देश के दो अलग -अलग कालखण्डों का इतिहास भी झांकता दिखाई देता है। जीवन में चलनेवाली सुख दुख की आंख मिचौली के मर्मस्पर्शी चित्रण के साथ -साथ तत्कालीन बांग्ला साहित्य की कई घटनाओं और चरित्रों के विश्वसनीय चित्र इस आत्मकथा में समाहित हैं।”स्मृतिकथा” में भी उनके व्यक्तिगत अनुभवों आए हैं और “स्मृति सतत सुखेर” में यात्रा वृत्तांतों के साथ निजी अनुभव सहज ही समाहित हो गये हैं।
जया मित्र रचित “हन्यमान” (1989,जो मारे जाएंगे) की चर्चा भले ही उनकी जेल डायरी या उपन्यास के रूप में होती है लेकिन इसे आत्मकथा कहा जाना चाहिए। नक्सल आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता जया अपने जेल जीवन के अनुभवों को शब्दबद्ध करते हुए देश की न्याय व्यवस्था , भारतीय कानूनी प्रक्रिया को निरंतर सवालों के घेरे में खड़ा करती हैं। जेलों के अंदर की घुटन, वहाँ व्याप्त भ्रष्टाचार, महिला कैदियों की दुर्दशा, उनके साथ पिसते उनके निरपराध बच्चों की व्यथा का वर्णन जया ने संजीदगी से किया है।
बांग्ला की स्त्री आत्मकथाओं की चर्चा हो तो बांग्लादेशी लेखिका तसलीम नसरीन की आत्मकथाओं का जिक्र स्वाभाविक है। प्रचलित पुरुष शब्दावली के समानांतर अपनी नयी स्त्री शब्दावली गढ़नेवाली तसलीमा की आत्मकथाएँ अपने बेबाक चित्रण और खुलेपन के कारण सनसनी भी फैलाती रहीं। औरत की आजादी के लिए निरंतर आवाज बुलंद करनेवाली तसलीमा ने धर्म और पुरुषसत्ता पर कठोर प्रहार किए जिसका खामियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ा। हिंदी में अनूदित और तकरीबन छ: खंडों में प्रकाशित इन आत्मकथाओं ने पाठकों और आलोचकों का ध्यानाकर्षित किया। “आमार मेयेबेला” ( मेरे बचपन के दिन, 2000 ) में उनके अपने शैशव के चित्रों के साथ तत्कालीन समाज में उपेक्षित स्त्रियों के चित्र जीवंत हो उठे हैं। अपने ही घर परिवार के लोगों के द्वारा होने वाले बच्चियों के यौन शोषण का खुला वर्णन तसलीमा ने किया है। “उत्ताल हवा” (2003) उनके किशोरावस्था के जीवन , संगी साथियों आदि को अपने में समेटे हुए है। “द्विखंडित” (2004 ) ने कई विवादों को जन्म दिया। इसे प्रतिबंधित कर दिया गया जो बाद में हाईकोर्ट के फैसले के बाद हटाया गया। “वे अंधेरे दिन” (2005) में तसलीमा ने उन दिनों की व्यथाकथा लिखी है जब उन्हें अपने ही देश में तकरीबन दो महीने तक छिपकर, भय और आतंक के साए में जीवन गुजारना पड़ा था। “मुझे मेरे घर ले चलो” (2007) में उन्होंने देश से दूर होने की पीड़ा के साथ -साथ अपने विश्व भ्रमण के अनुभवों को भी संजोया है। “नहीं, कहीं कुछ भी नहीं” (2012) वस्तुतः एक बेटी का माँ के नाम लिखा गया खुला पत्र है जिसमें अपनी दिवंगत मां को याद करती हुई लेखिका न केवल अपना दुख उनसे बाँटती हैं बल्कि मां के दुखों का आकलन करती हुई विश्वभर की महिलाओं के पीड़ाभरे इतिहास को भी दर्ज करती चलती हैं।
दिवंगत सुष्मिता बंद्योपाध्याय जिन्होंने एक आकर्षक काबुलीवाले जांबाज के प्रेम में पड़कर अपने परिवारवालों के विरोध के बावज़ूद उससे विवाह किया और काबुल में लंबे समय तक रहीं भी, ने अपने अनुभवों को अपनी तीन आत्मकथाओं “काबुलीवाले की बंगाली बीवी”(2002), “तालिबान अफगान और मैं”, “एक अक्षर भी झूठा नहीं” (2003) में समेटा है। व्यक्तिगत अनुभवों के साथ-साथ सुष्मिता ने अफगानिस्तान के सामाजिक, राजनीतिक जीवन के चित्र भी उकेरे हैं। तालिबानी आतंकवादियों का खुलकर चित्रण भी किया, जिनके हाथों अंततः उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी।
‘देश’ पत्रिका में धारावाहिक रूप से छपने के बाद 2008 में पुस्तक रूप में प्रकाशित, सत्यजित राय की पत्नी विजया राय की आत्मकथा ‘आमादेर कथा’ का जिक्र भी जरूरी है। रे के साथ अपने कैशोर्य प्रेम, विवाह से लेकर उनकी मृत्यु तक के समय को समेटते हुए, अपने जीवन की बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाओं, गोपन प्रसंगों को विजया ने बेहद साहस और ईमानदारी से चित्रित किया है। विख्यात राय परिवार के सदस्यों के जीवन की विश्वसनीय झलकियां भी इसमें झलकती हैं।
मंदार मुखोपाध्याय रचित “आस कथा : पास कथा” (2009) लेखिका के जीवन के आस – पास बिखरी तमाम कथाओं के छोटे- छोटे टुकड़ों से बुनी गयी एक रंगीन चादर है। इसे मैं आत्मकथात्मक कोलाज कहना चाहूंगी जिसके बारह अलग शीर्षकों में कहीं केन्द्र तो कहीं हाशिये के रूप में लेखिका स्वंय उपस्थित हैं । ऐसा ही एक और कोलाज है कल्याणी दत्त लिखित “पिंजरे बसिया”।
दीप्ति चंद की आत्मकथा “पद्यपातार दिन” (2010) एक साधारण महिला द्वारा लिखी गयी असाधारण कथा है। बेहद सहज सरल अंदाज में दीप्ति अपनी जीवनयात्रा और बंगाल की सांस्कृतिक विशिष्टताओं से पाठकों को अवगत कराती हैं। अपराजिता दासगुप्ता “इच्छेर गाछ ओ अन्यान्य” (2014) में अपने शैशव और कैशोर्य की सुखद स्मृतियों के साथ सत्तर के दशक के जलते-सुलगते कोलकाता की भयावह छवियाँ भी उकेरती हैं। अवसाद के साथ ही रचनात्मक आलोक से घिरी इस कथा में स्त्री चेतना की स्पष्ट छाप दिखाई देती है।
दलित स्त्री आत्मकथाओं की बात करें तो बेबी हाल्दार रचित ‘आलो आंधारी ( 2002) का जिक्र आवश्यक है जो बांग्ला में बाद में छपी, हिंदी अनुवाद पहले ही छपकर पर्याप्त चर्चा और प्रशंसा बटोरने में सफल हुआ। इसके अलावा मंजूश्री विश्वास रचित ‘जीवन कथा’ और नमिता दास की “कन्यारत्न” उल्लेखनीय हैं। नमिता दास ने पत्र शैली में बहुत कम शब्दों में अपनी मार्मिक संघर्षकथा संपादक के माध्यम से बाँटी है। अपनी तीन कन्याओं को कम साधनों के बावजूद रत्न में परिणत करनेवाली नमिता कविगुरू की वाणी से प्रेरणा ग्रहण करती हैं कि “खाना खाओ या न खाओ मगर अपने बेटे बेटियों को शिक्षा जरूर दिलवाओ।” कल्याणी ठाकुर चांडाल की “आमि केन चांडाल लिखी” (2016) में नम:शूद्र नारी के निजी संघर्ष के साथ जातिविशेष के लोगों के चुनौतीपूर्ण जीवनसंघर्ष का वर्णन भी ईमानदारी से हुआ है। इसकी भूमिका में कल्याणी ने लिखा है कि पुस्तक प्रकाशन के समय उन्होंने कुछ राजनीतिक लोगों का दबाव महसूस किया था, जिन्हें इस पुस्तक का छपना रास नहीं आ रहा था।
बंगाल की वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी की आत्मकथा ‘मेरी संघर्षपूर्ण यात्रा ‘ (2013) एक राजनीतिक कार्यकर्ता के सड़क से संसद और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुँचने के अनथक संघर्ष को सामने लाती है।
इसके अलावा बांग्ला लेखिकाओं ने बड़ी संख्या में ऐसे आत्मकथात्मक उपन्यासों की रचना की जिनमें उन्होंने अपने जीवनानुभवों को किसी काल्पनिक चरित्र के माध्यम से अभिव्यक्त किया। ये उपन्यास अपने समय और समाज का जीवंत दस्तावेज हैं। इनमें सर्वाधिक उल्लेखनीय हैं- आशापूर्णा देवी विरचित उपन्यास त्रयी-“प्रथम प्रतिश्रुति”, “सुवर्णलता” और “बकुलकथा”। “बकुलकथा” की कथा भले ही काल्पनिक पात्र बकुल की आत्मकथा है लेकिन इसमें लेखिका के अपने जीवनानुभव स्वतः समाविष्ट हो गये हैं । मैत्रेयी देवी के “न हन्यते” के बारे में भी आलोचकों का कहना है कि इसमें काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से मैत्रयी ने स्वयं अपनी जीवनकथा ही कही है। इसी तरह संगीता बंद्योपाध्याय ने “आर्विभाव” में कमोबेश अपनी जीवनकथा ही “तरी” के माध्यम से लिखी। बांग्ला साहित्य में यह आत्मकथात्मक शैली बेहद लोकप्रिय और स्वीकार्य रही है।
बांग्ला में हिंदी की ही तरह कई ऐसे स्मृतिचित्र या संस्मरण मिलते हैं जिनमें लेखिका के प्रिय पात्रों से जुड़े संस्मरणों में स्वयं लेखिका का जीवन भी झांकता -झिलमिलाता दिखाई देता है। ऐसी ही एक उल्लेखनीय किताब है, रानी चंद रचित “आलापचारी रवीन्द्र नाथ” (1943) जिसमें लेखिका ने कविगुरु रवीन्द्रनाथ ठाकुर से जुड़े अपने जीवनानुभवों को बड़ी सहज और मार्मिक शैली में उकेरा है। इसी कड़ी में “बाबार कथा” (उमा देवी), “रवीन्द्रस्मृति” (इंदिरा देवी चौधुरानी), “मृत्युहीन प्राण” (1977, शहाना देवी), “ऋत्विक”(1977, सुरमा घटक), “दीदीमार जुग ओ जीवन”, “प्रवासिनी दीदी माँ”(1992, 1994, अमिया चौधरानी), “संध्यारातेर शेफाली: आरती दास (शीर्ष बंधोपाध्याय, 2014) आदि नाम उल्लेखनीय हैं।
…………