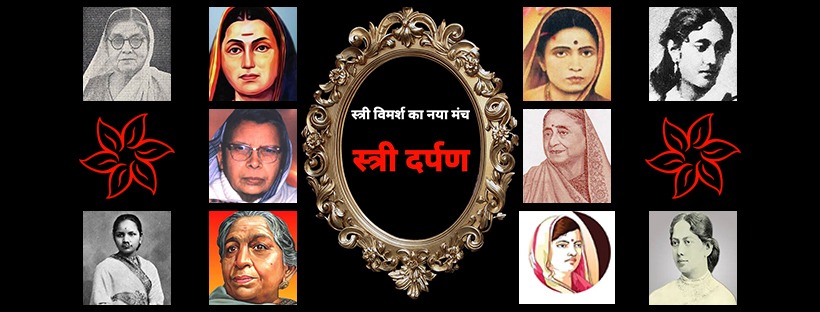- नाम – डॉ. रेनू यादव
- जन्मतिथि एवं जन्मस्थान – 16 सितम्बर,1984. गोरखपुर
- पद – फेकल्टी असोसिएट
- संप्रति – भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग (हिन्दी), गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा
- ई-मेल – renuyadav0584@gmail.com, renu@gbu.ac.in
- ब्लॉग – www.renukamal.blogspot.com
- शिक्षा – एम.ए., एम.फिल., पीएच.डी., यू.जी.सी-नेट
- रचनाएँ –
- ‘काला सोना’ (कहानी-संग्रह), 2022
- ‘महादेवी वर्मा के काव्य में वेदना का मनोविश्लेषण’ (आलोचनात्मक पुस्तक), 2010
-
- ‘मैं मुक्त हूँ’ (काव्य-संग्रह), 2013
- साक्षात्कारों के आईने में – सुधा ओम ढींगरा (संपादित पुस्तक), 2020
- प्रमुख कहानियाँ – कोपभवन, चऊकवँ राड़, वसुधा, छोछक, टोनहिन, मुखाग्नि, दबे पाँव
- प्रमुख कविताएँ – नमक, अस्तित्व, आम्रपाली, तड़फड़ाते हृदय के पाँवों में फफोले, रास्ते पर प्रसव
- प्रमुख शोध-पत्र – स्त्री विमर्श के आईने में राधा का प्रेम और अस्तित्व, पद्मावत और पूर्वराग, प्रवास में स्त्री-विमर्श टहल रहा है
- स्तम्भ – मासिक पत्रिका साहित्य नंदिनी में ‘चर्चा के बहाने’ स्तम्भ (कॉलम) प्रकाशित होता है तथा इससे पहले कैनेडा से निकलने वाली पत्रिका हिन्दी चेतना में ‘ओरियानी के नीचे’ नामक स्तम्भ प्रकाशित होता था ।
- स्त्री-विमर्श पर केन्द्रित कहानियाँ, कविताएँ एवं शोधात्मक आलेख आदि विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित ।
- सम्मान / पुरस्कार –
- ‘सृजन श्री’ सम्मान सृजन-सम्मान बहुआयामी सांस्कृतिक संस्था एवं प्रमोद वर्मा स्मृति संस्थान, रायपुर (छत्तीसगढ़) द्वारा प्राप्त । फरवरी, 2013 ।
- ‘विरांगना सावित्रीबाई फूले नेशनल फेलोशिप अवार्ड – 2012’ भारतीय दलित साहित्य अकादमी, दिल्ली द्वारा प्राप्त । दिसम्बर, 2012 ।
………………………….
किताबें
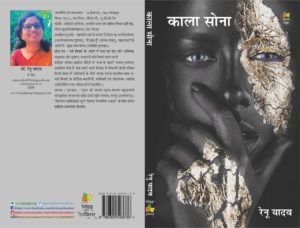
कहानी
मन छलनी तन काहे ना बिहरे
जिस समय साहित्य पर पुरूष लेखकों का पूरी तरह से वर्चस्व था, वैसे समय में मन्नू भंडारी ने लिखना शुरू किया । उनसे पूर्ववर्ती लेखिकाएँ कभी दबे-दबे स्वर में तो कभी मुखर होकर अपनी आवाज़ उठा रही थीं और अनेक आरोपों के बीच-बचाव में कभी पुल्लिंग में तो कभी स्त्रीलिंग में लिखते हुए पायी जाती थीं । परंतु मन्नू जी की पीढ़ी की लेखिकाओं में कृष्णा सोबती अपने बोल्ड लेखन के लिए, राजी सेठ मनोवैज्ञानिक लेखन के लिए और मन्नू भंडारी संवेदनात्मक लेखन के लिए पहचानी जा रही थीं । सीधे सपाट रूप से भावों को उकेरने वाली मन्नू समाज के उस यथार्थ को बिना लाग-लपेट के इस तरह से प्रस्तुत करती थीं कि उनकी कहानियाँ सीधे-सीधे पाठकों के हृदय में उतर जाती थीं ।
सन् 2012 में स्त्री-विमर्श का पाठ्यक्रम तैयार करते समय सुधा अरोड़ा जी से मेरी फोन पर बात हुई । उसके बाद फोन पर उनसे बात होती रहती थी, उनका जब दिल्ली आना हुआ तब उन्होंने बताया कि वे रचना जी के घर रूकेंगी, मैं उनसे मिलने वहीं आ जाऊँ । 28 सितम्बर, 2019 को रचना जी के घर पर सुधा अरोड़ा और मन्नू भंडारी जी से मिलना हुआ । वैसे तो मैं मन्नू भंडारी जी को पहले कई कार्यक्रमों में दूर से देख पायी थी, चलते फिरते प्रणाम भी हो गया था किंतु पहली बार इतने नज़दीक से मिली । उस दिन मन्नू जी कुछ विस्मृत्त अवस्था में थीं !
मेरे जाते ही उनकी सहायिका उन्हें बैठक में ले आयी और सोफा पर बैठा दिया और मैं उनके पैरों के पास बैठी रही । मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि जिन दो लेखिकाओं से मैं इतना प्रभावित हूँ, मैं उन्हें इतने करीब से देख पा रही हूँ । मैं हमेशा से चाहती थी कि उन दोनों लेखिकाओं के हाथों छू सकूँ जिन्होंने अपनी रचनाओं में इतनी संवेदना भरी हैं । शायद यह भी लालच रहा कि उनकी कुछ उर्जा महसूस कर सकूँ क्या पता उनकी कुछ तरंगें मुझ तक पहुँच जाएँ । न जाने ऐसा क्या था कि उस दिन मन्नू जी लगभग 1 घंटे से अधिक समय तक मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर बैठी रहीं । मैं दोनों ही लेखिकाओं के लिए साक्षात्कार के प्रश्न साथ ले गई थी, मन्नू जी अपने प्रश्नों को पढ़तीं और जो समझ में आता उसका जवाब देतीं और बीच बीच में उन जवाबों को सुधा जी पूरा करतीं । मैं वहाँ लगभग डेढ़-दो घंटे तक रही, लगातार मेरा संवाद सुधा जी से जारी रहा । सुधा जी बात करते समय बीच-बीच में उन्हें भी शामिल करते हुए बताती जातीं कि हम किस विषय पर बात कर रहे हैं अथवा उनका ध्यान हमारी बातों पर खींचने का प्रयास करतीं, कभी सफल होतीं तो कभी नहीं । संवादों के बीच में ही आदरणीय राजेन्द्र यादव जी की भी चर्चा शुरू हो गई । हमें लग रहा था कि मन्नू जी का ध्यान हमारी बातों पर नहीं होगा अथवा हमें अन्दाज़ा नहीं था कि वे इस प्रसंग पर ध्यान दे रही होंगी । उसी समय उन्होंने हमारी बात काटते हुए सुधा जी से पूछा, “क्या बात कर रही हो” ?
“हम राजेन्द्र जी के विषय में बात कर रहे हैं” सुधा जी ने बहुत ही प्यार से बताया
“किसके विषय में” ? शायद वे नाम सुन नहीं पायी थीं
“राजेन्द्र जी” सुधा जी ने ऊँची आवाज़ में बताया ताकि वे सुन सकें ।
“मत करो” मन्नू जी का दो टूक जवाब और हम दोनों चुप । फिर थोड़ी देर बाद विषय बदल गया ।
मिलकर आने के बाद मैं कई दिनों तक इस यह सोचती रही कि उन्हें कुछ भी याद नहीं, फिर भी उन्हें एक इन्सान याद है, वे हैं – राजेन्द्र यादव । विस्मृति में भी राजेन्द्र जी की स्मृति रखने वाली मन्नू जी का वह कौन-सा स्नेह सूत्र अथवा कसकती पीड़ा रही होगी जिससे वे उबर नहीं पा रहीं ! 35 सालों तक अनेक टूटन-घुटन के पश्चात् भी जिस रिश्ते को वे संभाले रहीं, कितना तो टूटी होंगी अलगाव के फैसले के समय ! क्या सचमुच वे अलग होकर भी अलग हो पायीं ! अलग होने के बाद ‘एक कहानी यह भी’ में वे लिखती हैं, “आज बिलकुल अकेली हो गई हूँ… पर राजेन्द्र के साथ रहते हुए भी तो मैं बिल्कुल अकेली ही थी । पर कितना भिन्न था वह अकेलापन जो रात-दिन मुझे त्रस्त रखता था ! साथ रहकर भी अलगाव की, उपेक्षा और संवेदनहीनता की यातनाओं से इस तरह घिरी रही थी, सारे समय कि कभी अपने साथ रहने का अवसर ही नहीं मिलता था । आज सारे तनावों से मुक्त होने के बाद अकेले रहकर भी अकेलापन महसूस ही नहीं होता ! आज कम से कम अपने साथ तो हूँ” ।
जो जूझता है, वह सींझता है और जो सींझता है वो पिघलता भी है और अपने अंतस से मजबूत भी होता है, जिसका अंतस मजबूत होता है वही लिखने का साहस भी कर पाता है । पाठकों के दिल में उतरने वाली मन्नू जी किस तरह अपने व्यक्तिगत जीवन में जूझ रही हैं, यह किसी को नहीं पता था क्योंकि मन्नू जी का स्वयं मानना था कि व्यक्ति में इतना साहस होना चाहिए कि वह अपने दुःख को झेल सके । कुछ बेहद निजी संबंधों के अतिरिक्त वे अपनी पीड़ा किसी से नहीं बताती थीं । धीरे-धीरे उनकी पीड़ा मन से लेकर शारीरिक व्याधियों में बदल गई । कथादेश और तद्भव में प्रकाशित साक्षात्कारों और आलेखों ने जिस तरह से उन्हें झकझोरा कि मवाद बना पीड़ा एक बार बहना शुरू किया तो बहता ही चला गया और इस तरह से बह गया कि कई प्रसंग तो राजेन्द्र जी ने स्वयं ही खोल रखा था उस पर मोहर लगाने का काम मन्नू जी ने कर दिया ।
किसी के व्यक्तिगत जीवन पर बात करने का हमें कोई अधिकार नहीं होता किंतु जब कोई व्यक्ति / लेखक स्वयं अपनी आत्मकथा / आत्मकथांश / आत्मकथ्य के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन को सार्वजनिक कर दें तो पाठक उस पर बात करने का अधिकार रखता है क्योंकि आत्मकथा लिख कर प्रकाशित ही इसी उद्देश्य से किया जाता है कि उनका व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक हो सके । राजेन्द्र यादव जी की आत्मकथा ‘मुड़ मुड़कर देखता हूँ’ (सं. प्रथम 2001, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली) तथा मन्नू भंडारी की आत्मकथा ‘एक कहानी यह भी’ (सं. प्रथम 2007, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली), जिसे दोनों लेखकों ने आत्मकथा न मानकर ‘आत्मकथ्यांश’ माना है, का प्रकाशन सार्वजनिक करने के ही उद्देश्य से हुआ है । राजेन्द्र जी लम्बे समय तक अतीत में जीने और वर्तमान तक पहुँचने की यात्रा को आत्मकथा मानते हैं जिसमें आत्मकथाकार को अपनी यात्रा के लिए जस्टीफ़िकेशन या वैधता की तलाश होती है, इसलिए वे अपने ग्रंथ को आत्मकथा न मानकर ‘आत्मकथ्यांश’ मानने पर बल देते हैं और मन्नू भंडारी अपने इस ग्रंथ को अपने लेखकीय व्यक्तित्व और लेखन यात्रा पर केन्द्रित ‘जीवन का एक टुकड़ा’ मानती हैं ।
दोनों ही लेखक बड़ी ही सजगता से अपने-अपने आत्मकथ्यांश को साहित्यिक यात्रा का अंश बनाने का प्रयास करते हैं । किंतु आत्मकथ्यांश में ‘आत्म’ सिर्फ साहित्य तो नहीं हो सकता ? अथवा उनका ‘स्व’ मात्र कोरा कागद तो नहीं था जिस पर सिर्फ ‘साहित्य’ लिखा गया हो, इसलिए ‘स्व’ और स्व से जुड़ें ‘पर’ का भी उल्लेख होना स्वाभाविक था । साथ ही बचाव हेतु ‘पर’ की प्रतिक्रिया और प्रतिक्रिया पर प्रतिक्रिया लिखना अथवा लिखवाये जाना भी जस्टिफ़िकेशन की ही अपेक्षा है । वह कौन-सा अथवा किसका भय था जिसके लिए ‘जस्टिफ़िकेशन’ से पहले ही बचाव पक्ष (तोते की जान) तैयार कर लिया गया ? अथवा बच-बच कर लिखा गया और अंत में स्पष्टीकरण (देखा तो इसे भी देखते…) देना पड़ा ? चाहे अपने को जस्टिफ़ाई करने के लिए आत्मकथ्यांश लिखा गया हो अथवा जस्टिफ़िकेशन से आहत होकर जवाब के लिए आत्मकथांश लिखा गया हो, अंततः आत्मकथा ही बनती है और पाठकों को जस्टिफ़िकेशन का अधिकार भी दे देती है । डॉ. नगेन्द्र का मानना है कि आत्मकथा में वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण किया जाता है, वे लिखते हैं, “ ‘आत्मकथाकार’ अपने संबंध में किसी मिथ की रचना नहीं करता कोई स्वप्न सृष्टि नहीं रचता । वरन् अपने गत जीवन के खट्टे-मीठे, उजाले-अंधेरे, प्रसन्न-विषन्न, साधारण-असाधारण, संरचना पर मुड़कर एक दृष्टि डालता है, अतीत को पुनः कुछ क्षणों के लिए स्मृति में जी लेता है और अपने वर्तमान तथा अतीत के मध्य संबंध सूत्रों का अन्वेषण करता है” ।
इसी प्रकार डॉ. श्याम सुन्दर घोष आत्मकथा को समय-प्रवाह के बीच तैरने वाले व्यक्ति की कहानी मानते हैं, “आत्मकथा समय-प्रवाह के बीच तैरने वाले व्यक्ति की कहानी है । इसमें जहाँ व्यक्ति के जीवन का जौहर प्रकट होता है, वहाँ समय की प्रवृत्तियाँ और विकृत्तियाँ भी स्पष्ट होती हैं” ।
यह ध्यान रखने योग्य बात है कि किन्हीं दो व्यक्तियों के आपसी निजी संबंधों के बीच प्रवृत्तियों और विकृत्तियों पर कोई तीसरा मात्र अपना मत दे सकता है, समस्या समझ सकता है, घटनाओं को उछाल सकता है, पर घटी घटना को (वह भी निरंतर चलने वाले रिश्ते को) कभी भी जस्टिफ़ाई नहीं कर सकता ।
‘एक कहानी यह भी’ के अनुसार तद्भव में प्रकाशित राजेन्द्र जी के आत्मकथ्य के प्रत्युत्तर में मन्नू जी ने ‘देखा तो इसे भी देखते…’ लिखती हैं, जो कि उन्होंने अपने स्वभाव के विपरीत तीखे स्वर में लिखा है । अन्यथा ‘एक कहानी यह भी’ में साहित्यिक यात्रा का वर्णन करते हुए वैवाहिक जीवन की खटास-मिठास को संयत स्वर में ही प्रस्तुत करने का प्रयास किया है । ‘मन्नू भंडारी का रचनात्मक अवदान’ नामक पुस्तक में सुधा अरोड़ा मन्नू भंडारी के विषय में कहती हैं, “मन्नू जी घोर नैतिकतावादी हैं – संस्कार और मूल्यों के प्रति गहरा सरोकार और लगाव । लेकिन अपने टूटने की क़ीमत पर संस्कारों और मूल्यों को बचाने का सवाल हो तो वे बेहद निर्मम होकर अपने को बचाने की कोशिश करेंगी, अपने जीने की क़ीमत पर वह मूल्यों के लिए अड़ नहीं जायेंगी… और संस्कारों और अपने आत्मसम्मान को बचाए रखने के इस संतुलन ने ही उन्हें सिर उठाकर अपने मूल्यों को भी बचाकर रखते हुए जीने की ताकत दी है” ।
‘एक कहानी यह भी’ एक आत्मनिर्भर, नैतिक, बौद्धिक स्त्री की कहानी है जो बिफर-बिफर कर अपनी बात न तो पुस्तक में कर सकती हैं और न ही व्यक्तिगत जीवन में । शायद बौद्धिकता की खोल ही ऐसी है कि जीवन की संपूर्ण पीड़ा को हृदय सोख लेता है, पीड़ा कहानियों-कविताओं में उतरती है पर लेखक प्रत्यक्ष रूप से कहने का साहस नहीं जुटा पाता । कदाचित् इसीलिए साहित्यकारों को कई-कई प्रकार की शारीरिक व्याधियों से जूझना भी पड़ता है । मन्नू जी अपनी आत्मकथा में वैवाहिक जीवन के विषय में जितना भी प्रस्तुत करती हैं उन वाक्यों के अन्दर कई कई वाक्य गूढ़ रहस्य लिए उभर आते हैं । कोई भी व्यक्ति लिखते समय अथवा बात करते समय अपने जीवन की घटनाएँ गिना सकता है, हो सकता है कुछ घटनाओं से जुड़ी संवेदना को भी प्रस्तुत करने में कामयाब हो जाए, लेकिन उस घटना के घटित होते समय, उसे झेलते समय तथा उबरने के बाद स्मृत्ति में भी जिस पीड़ा, टूटन-घुटन से वह गुज़रा है, उसकी यात्रा शब्दों में नहीं समझाया जा सकता । बहुत सी संवेदना सिर्फ समझी जा सकती हैं पर कही नहीं जा सकती । आखिर 35 सालों का सफ़र समझा पाना इतना आसान तो नहीं ! मन्नू जी कहते हुए भी चूक चूक जाती हैं ।
ख्यातिलब्ध राजेन्द्र जी का साथ साहित्य जगत में साहचर्य और समानता के भाव से एक दूसरे को सम्मानपूर्वक कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने की उम्मीद ने दोनों लेखकों को सहजीवन बना दिया, अधिकतर समय यह हुआ भी है कि कभी मन्नू जी ने अपने उपन्यास की थीम दे दी और कई बार राजेन्द्र जी मन्नू जी की कहानियों एवं उपन्यासों का नाम रखते थे । लेकिन जैसे ही गृहस्थ जीवन का जिक्र आता है, वहाँ मन्नू जी मात्र प्रेम करने वाली विशुद्ध पत्नी के रूप में ही नज़र आती हैं । पति-पत्नी का रिश्ते में सबसे अधिक निःस्वार्थ और सबसे अधिक स्वार्थ दोनों का समान रूप से समावेश होता है । ऐसे में ‘समानांतर ज़िन्दगी’ के पैटर्न में समान ध्यान न मिलने पर उपेक्षा का आभास होना स्वाभाविक ही है । लेखक के प्रति श्रद्धा से परे व्यक्तिगत संबंधों में रिश्ता हर रोज दोनों तरफ से निभाने की, जीने की प्रक्रिया का नाम है । कदाचित् आर्थिक और पारिवारिक जीवन के उत्तरदायित्वों का वहन करते समय मन्नू जी ने एक सामान्य पत्नी की भाँति “चाहा था तो एक अटूट विश्वास, एक निर्द्वन्द्व आत्मीयता और गहरी संवेदना” ।
ऐसा नहीं था मन्नू जी अपनी कहानी में सिर्फ पीड़ा ही व्यक्त करती हैं बल्कि राजेन्द्र जी का विवाह से पूर्व मिलन का एहसास, स्वप्न और विवाहोपरांत कभी कभी राजेन्द्र जी का उन्हें अस्पताल ले जाना, टिंकू के लिए रोना तथा साहित्यिक चर्चाओं का भी वर्णन करती हैं, इसी प्रकार राजेन्द्र जी भी मन्नू जी पर विश्वास रखते हैं और अपनी यात्रा की सफलता में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करते हैं । मन्नू जी का कलकत्ता के बन्द समाज में खुलेआम इनसे विवाह करना, पैर तथा आँखों को लेकर हीनता-ग्रंथि से उबारने में इनका सहयोग करना, घर-परिवार में आर्थिक आधार बनना, अक्षर प्रकाशन की स्थिति सुधारने के लिए रॉयल्टी लेना, इनकी सहायता के लिए वेतन का प्रॉविडेंट फंड तक निकाल देना, मित्रों से सहायता लेकर कूर्की हो रहे घर को बचाना, चिट फंड के पैसे न चुका पाने पर इन्हें धोखे के आरोप से बचाना तथा एक्सीडेंट और बीमारियों में इनके लिए रात-दिन एक देने वाली भूमिकाओं से राजेन्द्र जी प्रभावित भी थे । “ठहराव और गहराई तो मन्नू ने ही दी” कहते हुए भी मन्नू जी के साथ ठहर न पाने की हीनताग्रंथि पर विजय पाने की लालसा थी अथवा कुछ नया पा लेने की चाह अथवा कुछ कर गुजरने की चाह ! ऐसे कई सारे प्रश्नों के उत्तर उनके निजी जीवन के अंतरगता में छुपे हैं, जिसका पता मन्नू जी को बहुत बाद में चलता है । वे उनके बाहरी और भीतरी व्यक्तित्व के अंतर्संबंधों और भेद के सूत्र को तलाशती रह गईं और सूत्र इस तरह एक-दूसरे में उलझे हुए थे कि उन्हें सुलझाना आसान नहीं था ! जिसके सूत्र ‘तोते की जान’ लेख में मिलता है, “अब तो सामने है चौतरफा प्रहार । उनके कवच के भीतर क्या हाल है इसका अन्दाज़ा लगाना आसान नहीं क्योंकि सूराख अगर कहीं है तो बड़ी होशियारी से छिपाए गए हैं और भीतर का कुछ दिखता ही नहीं है” ।
विवाह की प्रत्यंचा पर चढ़े कई प्रसंगों के बीच विवाह को निर्विघ्न रूप से निभा ले जाने की जिद्द ने मन्नू जी को कहीं और सूत्र होने का संकेत तो दिया किंतु यह उनका राजेन्द्र जी पर अटूट विश्वास ही था कि जिसके आगे संशय टिक नहीं पा रहा था । जिसके लिए मोहन राकेश का विवाह न करने की सलाह देना, ठाकुर साहब का राजेन्द्र जी के भविष्य की चिंता करते हुए सब छुपा ले जाना तथा राजेन्द्र जी का अपारदर्शी एवं अंतर्द्वन्द्व भरा व्यवहार और स्वयं मन्नू जी का सत्ता के खिलाफ जाकर राजेन्द्र जी का चयन आदि ऐसे अनेक कारक हैं जो एक चुनौती बनकर इनके सामने खड़े थे और प्रत्येक चुनौतीयों को चुनौती देने के लिए मन्नू जी तैयार थीं ।
“मैं तो इनसे बहुत जुड़ी हुई थी ही और बदले में वैसा जुड़ाव ही तो चाहती थी” जैसे निर्द्वन्द्व आत्मीयता के विपरीत विवाह के सुखमय पाँच दिन (सिर्फ मन्नू जी की समझ से) गुजारने के बाद जब आर्थिक आधार न तैयार कर राजेन्द्र जी कलकत्ता वापस लौटते ही उन्हें एक दूसरे की ज़िन्दगी में बिना किसी हस्तक्षेप किए एक छत के नीचे अपनी-अपनी ज़िन्दगी जीने का ‘समानांतर ज़िन्दगी’ का आधुनिक पैटर्न का फैसला सुना देते हैं । ऐसे में छत क्या पैरों के नीचे से ज़मीन का खिसक जाना स्वाभाविक ही था । गर्भावस्था हो अथवा बेटी टिंकू का जन्म, अपनी बीमारी हो अथवा बेटी टिंकू की तबीयत खराब होना अथवा उनकी पढ़ाई, आर्थिक उत्तरदायित्व हो अथवा पारिवारिक… इन सबमें समानांतर पैटर्न की जगह इकहरा पैटर्न का ढाँचा तैयार हो जाता है, जिसके भीतर स्वतंत्रता के समानांतर पैटर्न की खोखली आवाज़ का ‘इको’ हृदय को खोखला करता गया, जिसकी भरपाई जब-तब लेखन से ही पूरा हो सकता था और मन्नू जी ने उन्हीं व्यस्ताओं में से समय निकाल कर उन्हें पूरा करने की भरपुर कोशिश भी की हैं । ‘विशिष्ट जीवन शैली’ और ‘रचनात्मकता की स्वतंत्रता’ मन्नू जी के लिए भी उतनी ही आवश्यक थीं जितनी की राजेन्द्र जी के लिए । किंतु विशिष्ट जीवन शैली का चयन करना परिवार और विवाह को हारने देना होता, जो कि मन्नू जी के लिए संभव नहीं था । वर्चस्ववादी सत्ता का दबाव जितना अधिक ‘अरेंज्ड मैरिज’ निभाने की होती हैं उससे भी कहीं अधिक ‘लव मैरिज’ निभाने की होती है । मन्नू जी किसी भी हाल में उसे निभा ले जाना चाहती थीं । कहीं न कहीं निभा ले जाने के पीछे गहरी संवेदना ही थी जिसके लिए पूरी दुनियाँ से लड़कर उन्हें पाया था अब उनसे ही लड़ कर उन्हें पाना था और उनके कातर शब्दों और आँसूओं को देखकर ‘आज नहीं तो कल’ सब ठीक हो जाने की उम्मीद भी थी । वे ‘एक कहानी यह भी’ में लिखती हैं, “अगर मैं राजेन्द्र जी के साथ रही तो उनके प्रति गहरे लगाव के कारण रही और यदि अलग हुई तो अपनी मुक्ति के लिए” ।
प्रेम में एकनिष्ठता भी एक दायित्व है और दायित्व को निभाने से ही प्रेम टिका रह सकता है । मन्नू जी का एकनिष्ठ प्रेम करते जाना तथा एकनिष्ठ प्रेम की चाह उनके वैवाहिक सफ़र को और भी अधिक दुखदायी बना दिया । ऐसे में पति के होते हुए भी न होने का बोध उनके वैवाहिक बंधन को निभा ले जाने के संकल्प को कमज़ोर बनाता गया । घायल की गति घायल ही जान सकता है, ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व से न तो पर्दा उठा पाना आसान होता है और न ही खुल कर कह पाना । क्योंकि अन्य के सामने वह चेहरा होता ही नहीं । ‘मन्नू भंडारी के रचनात्मक अवदान’ पुस्तक में कुमुद शर्मा कहती हैं, “मन्नू भंडारी ने अपने दांपत्य जीवन में उस प्यार को पाना चाहा जो जार्ज बनार्ज शॉ के लिए ब्लिसफुल मिस अंडरस्टैंडिग था और रानिया मारिया रिल्के के ‘डूथूनों एलिजी का हसीन ख्वाब’ ” ।
राजेन्द्र जी भी जीवन के उस छोर पर थे जब ज़िन्दगी के दोराहे पर खड़े होकर किसी विशेष रास्ते की तलाश कर रहे थे । किंतु यह भी सत्य है कि दोराहे पर खड़े होकर पलायन मन में प्रेम का संचारी भाव तो जाग सकता है किंतु स्थायी भाव कभी नहीं जाग सकता । ऐसे में सामने वाला ही स्थायी भाव लिए ठगा-सा रह जायेगा । मन्नू जी के साथ भी यही हुआ । ‘एक कहानी यह भी’ के अध्ययन से यह प्रतीत होता है कि मन्नू जी को लगता है कि राजेन्द्र जी उन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहते थे किंतु ‘मुड़ मुड़ कर देखता हूँ’ से स्पष्ट हो जाता है कि बोहेमियन-ज़िन्दगी की चाह रखने वाले राजेन्द्र जी कई बार मन्नू जी को छोड़ कर जाने का प्रयास कर चुके थे, कभी साहित्य लेखन के नाम पर कभी संचारी भाव की एक संचारिका को ‘वी आर मैरिड’ के नाम पर अथवा कभी भ्रमण के लिए । किंतु हर बार वे अपने दृढ़-संकल्पी माँ के दिए संस्कारों के कारण लौट आते थे ।
जितना अंतर्द्वन्द्व दोराहे पर खड़े राजेन्द्र जी के मन में था उससे कहीं अधिक तकलीफ मन्नू जी के लिए राजेन्द्र जी के अंतर्द्वन्द्व से जूझ रहे मन को समझने के बाद था, इसीलिए तो वे उन्हें सैटिल होने की सलाह भी दे देती थीं । किंतु गुमसुम राजेन्द्र जी को निरंतर अंतरंग परिचय से बिल्कुल अपरिचय की दुनियाँ में लौटते हुए देखना मन्नू जी के लिए असह्य हो गया । राजेन्द्र जी तो वेश्या लिलियन रॉथ की आत्मकथा ‘आई विल क्राई टुमारो’ से प्रभावित होकर खुद का रोना टाल सकते थे, पर जो व्यक्ति रूदन ही जी रहा हो ऐसा सहजीवन क्या करे ? सहजीवन के साथ एक कदम घर में तथा दो कदम घर के बाहर संचारिकाओं का साथ पाने अथवा हारी-बीमारी की अवस्था में सहजीवन को छोड़कर जाना राजेन्द्र जी को सहजीवन के ‘सह’ से अलग कर रहा था । ऐसे में इसका जवाब स्वयं राजेन्द्र जी देते हैं, “अर्चना वर्मा ने लिखा है कि जब भी मुझे लगता है कि दूसरा मुझ पर हावी हो रहा है, या मेरी स्वतंत्रता खतरे में है । तभी मैं अपने को खींच लेता हूँ – अपने आपको एकात्म भाव से सौंप नहीं पाता और दूसरा ‘धोखा खाए’ के भाव से झुँझला उठता है” ।
इसके बावजूद भी मन्नू जी सहजीवन के साथ इकहरे पैटर्न (न कि समानांतर) और प्रतिबद्धता के साथ जीवन के 35 वर्ष बिता लेती हैं । इन सबमें उनकी विद्रोही संवेदनतंत्रियाँ हार गईं और न्यूरोलॉजिया की शिकार हो गईं । 35 वर्ष जीवन के प्रकृतिप्रदत्त सुनहरे स्वप्न से लेकर पतझड़ के पड़ाव तक की एक लम्बी यात्रा होती है । फिर भी कई बार आरोपों के घेरे में यह सुनने में आता है कि मन्नू जी ने बहुत जल्दी अलग होने का फैसला ले लिया ।
हमारे समाज का अभी भी इतना मानसिक विकास नहीं हुआ है कि वह एक सधवा का दुख समझ पाये । वैसे तो स्त्रियों का दुःख ही वर्चस्ववादी सत्ता के लिए महत्त्व नहीं रखता, किंतु सधवा स्त्री की पीड़ा प्रेयसी, विधवा, छोड़ी हुई स्त्री अथवा परदेश गए पति की वियोगिनी स्त्री से कमतर आंका जाता है । सामान्यतः यह मान लिया जाता है कि जिसका पति साथ है उसे भला कौन-सा दुःख ! शिकायत करने वाली सधवा को भावुक, शकी, मेंटल जैसे आरोपों से नवाज़ना समाज का एक सामान्य पैटर्न है । पति से अलग होने का फैसला करने वाली सधवाओं (जिसका रिश्ता पहले ही मर चुका होता है) को बार-बार सोचने और अलगाव संबंधी निर्णय बदलने के लिए विवश किया जाता है, बगैर यह समझे कि कोई भी फैसला एक झटके में नहीं लिया जाता बल्कि लगातार चली आ रही नकार, उपेक्षा की यह प्रतिक्रिया होती है ।
व्यक्तिगत जीवन का असर मात्र सेहत पर ही नहीं बल्कि व्यवसाय और लेखन पर भी पड़ता है । मन्नू जी जिस आत्मकथांश को साहित्यिक बनाना चाहती थीं वह ‘राजमार्ग’ व्यक्तिगत कारणों से ही अवरूद्ध हुआ, भले उसका नाम बीमारी ही क्यों न हो ? किंतु यह भी सत्य है कि मन्नू जी को अपनी रचनाओं के मूल्यांकन के लिए साथ तो मिला किंतु उन्हें कंधे की जरूरत नहीं पड़ी । दो लेखकों का एक साथ होने पर भी दोनों की रचनाओं को एक-दूसरे पर बिना आरोपित, अवलम्बित किए अलग-अलग मूल्यांकित किया जा सकता है । दोनों की भाषा-शैली और कथ्य की बुनावट में अंतर स्पष्ट नज़र आता है । जिस राजमार्ग की बात मन्नू जी आत्मकथा के प्रारंभ में करती हैं अंत तक आते-आते वे स्वयं लिखती हैं, “अपनी रचनाओं की समीक्षा के लिए… पुरस्कारों के लिए या अन्य किसी उपलब्धि के लिए कभी इनके नाम की बैसाखी मैंने नहीं लगाई… और बैसाखी तो तब लगाती जब मैं इन बातों के लिए प्रयत्न करती…”
इस ग्रंथ को लिखने से जीवन में कोई बदलाव आया या नहीं यह नहीं कहा जा सकता, किंतु यह संभव है कि मन्नू जी के मन का कुछ बोझ हल्का हो गया हो । प्रो. गरिमा श्रीवास्तव ने सच ही लिखा है, “‘आत्मकथा’ लेखक का न सिर्फ विरेचन करती है बल्कि जिस समाज में वह रह रहा है, उसकी उत्थान-पतन के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों का विश्लेषण भी उसमें स्थान पाता है. आत्मकथा रचनाकार के साथ-साथ उसके परिवेश को परिवर्तित-निर्मित करने का प्रयास होती है । इसके साथ शर्त इतनी-सी है कि उसके लेखन में ईमानदारी बरती जाए. आत्मकथा की पुकार सच की पुकार होती है, लेकिन सच बोलकर हमारी सामाजिक संरचना में रचनाकार की छवि निष्कलंक रह पाएगी इसमें संदेह है” ।
‘प्रेम गली अति सांकरी’ साथ चले तो कैसे चले और छोड़कर भी चला न जाए । छूट जाने पर सब छूट जाए यहाँ तक स्मृति भी । पर उसकी स्मृति कैसे छूटे जिसने मन को जोड़ा भी और छलनी भी कर दिया । साहित्यिक यात्रा या रचना-प्रक्रिया जानने के लिए यह आत्मकथा / आत्मकथांश / जीवन का टुकड़ा पढ़ना जरूरी है । इसलिए भी जरूरी है कि हम समझ सकें कि विशुद्ध प्रेम की पीड़ा किस प्रकार स्मृति से विस्मृति तक पहुँचाती है । और इससे भी अधिक इसलिए जरूरी है कि लेखन में कोई दूसरी मन्नू भंडारी तो नहीं हो सकतीं लेकिन व्यक्तिगत जीवन में त्याग, बलिदान, प्रेम और पीड़ा के नाम पर कोई दूसरी मन्नू भंडारी न बन जाए…
रेनू यादव
फेकल्टी असोसिएट
भारतीय भाषा एवं साहित्य विभाग
गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय,
यमुना एक्सप्रेस-वे, गौतम बुद्ध नगर,
ग्रेटर नोएडा – 201 312
ई-मेल- renuyadav0584@gmail.com
………………………….