
सुधा सिंह - दिल्ली विश्वविद्यालय में वरिष्ठ प्रोफेसर। कोलकाता में जन्म, कलकत्ता विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट तक की शिक्षा दीक्षा। एम. ए और बी. ए में स्वर्ण पदक। कलकत्ता विश्वविद्यालय से ही अध्यापकीय जीवन का आरंभ। तत्पश्चात विश्व भारती विश्वविद्यालय, शांतिनिकेतन में लगभग पांच वर्षों तक अध्यापन। वहां से सन् 2004 में दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली। सन् 2010-12 तक विजिटिंग संस्थापक प्रोफेसर हिंदी पीठ, अश्गाबात, तुर्कमेनिस्तान, भारतीय विदेश मंत्रालय, भारत सरकार। सन् 2010 से सन् 2020 तक प्रोफेसर, हिंदी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, सन् 2020 से वरिष्ठ प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय। अब तक आलोचना, मीडिया और स्त्री विमर्श पर लगभग तीस पुस्तकें प्रकाशित। जिनमें 'जनमाध्यम सैद्धांतिकी', 'भूमंडलीकरण और ग्लोबल मीडिया', 'ज्ञान का स्त्रीवादी पाठ', ' जनतंत्र जनमाध्यम और वर्तमान संकट', 'मध्यकालीन साहित्य विमर्श', 'स्त्री अस्मिता साहित्य और विचारधारा ', 'स्त्री संदर्भ में महादेवी ' आदि प्रमुख हैं। माध्यम और स्त्री विमर्श में एक जाना माना नाम।
………………………….
लेख - स्त्रीः संस्कृति और स्वाधीनता
-सुधा सिंह
संस्कृतिः
दिनकर ने सन् 1956 में प्रकाशित पुस्तक ‘संस्कृति के चार अध्याय’ की भूमिका में लिखा है कि ‘‘खास दिलचस्पी की बात तो यह है कि सांस्कृतिक एकता की बातें जनसाधारण ही सुनना चाहता है; पण्डित और विशेषज्ञ ऐसी बातों से बिदक जाते हैं।’’ संस्कृति को देखने का एक तरीक़ा यह है कि हम अतीत को वर्तमान का विलोम बनाकर देखें। इस विलोम का क्रम अच्छा-बुरा या बुरा-अच्छा दोनों हो सकता है। स्त्री के संदर्भ से अगर संस्कृति को देखना हो तो बहुत सहज है कि हम पहला क्रम यानि अच्छा और बुरा को चुनें। क्योंकि वर्तमान में जिस तरह का समाज और जिस तरह की संस्कृति हमने बनाई है वह स्त्री के साथ द्वेषपूर्ण, बर्बर और हिंसात्मक है। निर्भया कांड को हम भूले नहीं हैं, गुड़िया कांड, मंदसौर की घटना, कठुआ और उन्नाव जिनमें मासूम बच्चियों के साथ बर्बरता और बलात्कार की घटना घटी है, आए दिन ये घटनाएँ और बर्बर शक़्ल में सामने आ रही हैं। बलात्कार और यौन हिंसा के बाद अब बर्बर शारीरिक हिंसा उसका एक हिस्सा बनकर सामने आ रही है। आँखें फोड़ देना, अंग-भंग करना, बाहरी वस्तु से शरीर के अंगों को क्षति पहुँचाना, हत्या कर देना, बलात्कार और यौन हिंसा की घटनाओं में आए दिन रिपोर्ट की जा रही हैं। जितनी सजाएँ हैं वे समस्या के निवारण के लिए होकर भी निवारक साबित नहीं हुईं। इस तरह की घटनाओं से रोज़ के अख़बार रंगे रहते हैं। और इस कदर हमारी भावनाओं को स्त्री के प्रति यौनिक हिंसा के लिए अनुकूलित कर दिया गया है कि हमारी प्रतिक्रिया जब तक यौन हिंसा में कोई बर्बरता का एंगल शामिल न हो, ठंडी ही होती है। हाल के थॉमसन रायटर फाउंडेशन सर्वे में भारत को स्त्रियों के लिए सबसे ख़तरनाक देश माना गया है। (संदर्भ ‘द गार्जियन’) स्त्री के संदर्भ में संस्कृति की बात करेंगे तो देखना होगा कि स्त्री के लिए हमने कैसी संस्कृति विकसित की है। यहाँ यह जानना और विश्लेषित करना जरूरी है कि स्त्री को किस नजरिए से देखते हैं क्योंकि नजरिया महत्वपूर्ण होता है। वह पूरा वातावरण बनाता है और भविष्य की गतिविधियों को भी तय करता है। स्त्री के प्रति हमारा नजरिया ही बलात्कार की संस्कृति को भी जन्म देता है। भारत का संविधान भारत की स्त्रियों को बराबर का अधिकार हर क्षेत्र में देता है। मतदान के नागरिक अधिकार से लेकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, आंदोलन का अधिकार और देह और कोख पर अधिकार भारतीय संविधान देश की स्त्रियों को देता है। यहाँ पर शहरी स्त्रियाँ हैं जो आधुनिक शिक्षा और चेतना से लैस हैं, काम पर जाती हैं। उनकी सुरक्षा के लिए ‘काम की जगह पर यौन हिंसा’ के खिलाफ क़ानून बना हुआ है। घरेलू और ग्रामीण, जिनमें शिक्षित-अशिक्षित दोनों तरह की स्त्रियाँ शामिल हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए ‘घरेलू हिंसा क़ानून’ बना हुआ है। असंगठित क्षेत्रों में काम करनेवाली स्त्रियों के लिए भी प्रतीकात्मक तौर पर कुछ सरकारी योजनाएँ जिनमें सम्मान के साथ सुनिश्चित दिनों के लिए रोजगार गारंटी है। लेकिन क्या स्त्रियाँ इन जगहों पर यानि घर, सार्वजनिक स्थानों, संगठित और असंगठित क्षेत्रों में नौकरी करते हुए अपने को सुरक्षित महसूस करती हैं? संस्कृति का सवाल स्त्री के समक्ष, उससे जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में दार्शनिक सवाल नहीं हो सकता। स्त्री के लिए संस्कृति के सवाल व्यवहार के सवाल हैं और संस्कृति स्वयं व्यवहार है और कुछ नहीं। ‘दूध की नदियाँ बहती थीं’, ‘स्वर्ण युग था’ बोलकर स्त्री के सवालों और संस्कृति से उसके संबंधों पर विचार नहीं किया जा सकता। आपको ठोस सवाल पूछने होंगे और सही सवाल सही स्थिति भी बताएगा। आपको पूछना पड़ेगा कि तब स्त्री कैसी थी, उसकी सामाजिक भूमिका क्या थी, कलाओं में उसकी उपस्थिति किस प्रकार की थी? क्या अंततः वह पुरुष के मनोविनोद और आराम का साधन मात्र थी? अगर ऐसा नहीं होता तो सुदूर अतीत में गौरवमय दावे का कोई सुनहला पक्ष आज भी तो दिखना चाहिए था। स्त्री के प्रति और स्पष्ट कहें तो स्त्री देह के प्रति ऐसी घृणा भक्ति काल में क्यों थी? ठीक उसके विपरीत गंभीर आसक्ति और अठखेली स्त्री देह को लेकर रीतिकाल में क्यों है? साहित्य की इस सुदृढ़ परंपरा का सामाजिक आधार क्या है? स्त्री के जीवन की सामाजिक सचाई से साहित्य का क्या संबंध बनता है? यह जानना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस साहित्य को पढ़कर पीढ़ियाँ तैयार होती हैं, दृष्टिकोण तैयार होता है। यह साहित्य जो मनुष्य बनाने का दावा करता है कि साहित्य पढ़कर हम थोड़े से ज़्यादा मनुष्य बनते हैं, स्त्री के संदर्भ में किस प्रकार का दृष्टिकोण तैयार करता है? एक स्त्री को संस्कृति के अंतर्गत किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलता है, यह ध्यान देने का विषय है। उसकी शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, आर्थिक निर्भरता- इन सबके बावजूद उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया जाता है, यह ग़ौरतलब है। मेडिकल की पढ़ाई करती लड़की, सामाजिक श्रेणी में निचले पायदान पर स्थित परिवार की लड़की, दलित परिवार की लड़की, मासूम नाबालिग बच्ची, प्रौढ़ स्त्री अथवा वृद्ध स्त्री सब की सब ‘वल्नरेबल’ हैं। इनके साथ कभी भी कहीं भी, यौन हिंसा, बर्बरता हो सकती है। हम इससे इंकार नहीं कर सकते कि सड़कों पर, काम की जगह पर, बाज़ार में, घर में स्त्री सुरक्षित महसूस नहीं करती। यह तब है जबकि कहें कि बहुत सी मर्दाना व्यवहारजनित असुविधाओं के साथ जीना स्त्री ने सीख लिया है और एक हद तक वह अस्तित्व के साथ लिपटी हुई असुविधाओं से तालमेल बैठाकर जीना सीख चुकी है। मतलब ठहरकर यह सोचना कितना भयाक्रांत करता है कि हम ऐसे समाज का हिस्सा हैं जो हमें हमारे अस्तित्व के साथ असहज संबंध में बँधने को मज़बूर करता है ! लड़कियों को यह बिना किसी लिखित और वैध निर्देश के सिखा दिया जाता है कि उन्हें कितने कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कितना ऊँचा बोलना है, कितना ठठाकर नहीं हँसना है, कितने बजे घर लौटना है, घर से अकेले नहीं किसीको साथ लेकर निकलना है और इतनी सब सावधानियों के बीच भी अपने साथ किसी भी तरह के यौन हिंसा के लिए तैयार रहना है। यह यौन हिंसा मौखिक से लेकर दैहिक –हर प्रकार की हो सकती है। इसके सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से स्थूल रूप हो सकते हैं। यहाँ तक कि स्त्रियों की सुरक्षा के लिए उनके पक्ष में बनाए गए क़ानून भी दोहरा मार करते हैं ! कार्यस्थल पर यौनिक हिंसा रोकने का क़ानून बनने के बाद अक़्सर पुरुष अधिकारियों अथवा शिक्षकों को यह कहते पाया जाता है कि उन्हें मातहत या प्रशिक्षु के रूप में महिला के बजाय किसी पुरुष को दिया जाए ! कंपनियाँ स्त्रियों को काम पर रखने पर विशेष सुविधाएँ देनी होंगी, महिला कर्मचारियों की नियुक्तियों में आनाकानी करती हैं। उन्हें महिलाओं का सस्ता श्रम तो चाहिए पर उन्हें महिला होने के कारण कोई विशेष सुविधा देनी होगी, इसे वे सहज रूप में नहीं ले पातीं। एक स्त्रीवादी विचारक ने कहा था कि स्त्रियाँ सामाजिक व्यवहार के दौरान कभी नहीं भूल पातीं कि वे स्त्री हैं। भारत की स्त्रियों के बारे में यह और भी कटु सत्य है कि हमारे समाज में स्त्रियों की परवरिश ‘स्त्री’ के रूप में जन्म (पालने से कहना सटीक नहीं होगा, क्योंकि ‘पालने’ का पुत्र संतान के लिए ही बहुधा जिक्र हुआ है।) से ही करना अरंभ कर देते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो स्टैटिसटिक्स के 2012 से लेकर 2016 के आंकड़े बताते हैं कि 40 प्रतिशत बलात्कार की शिकार अवयस्क बच्चियाँ हुईं हैं और उनमें से 95 प्रतिशत बलात्कारी को पहले से किसी न किसी रूप में जानती थीं। यानि बलात्कार का मामला ‘विश्वास’ का मामला भी बनता है। ‘जिन पर तकिया था, वही पत्ते हवा करने लगे’।भरोसे की हत्या का मामला था। हम एक ऐसा परिवार की संस्कृति बनाई है जिसके अंदर लड़की असुरक्षित है। हमने ऐसे समाज की संस्कृति बनाई है जहाँ या तो लड़की घूरी जा रही है, उसका पीछा किया जा रहा है, उसे अपशब्द कहे जा रहे हैं, तमाम शिक्षा और आर्थिक उपलब्धियों के बावजूद कभी भी उसका बलात्कार हो सकता है, वह ‘वल्नरेबल’ है। अपराधी घर से लेकर कार्यस्थल, शिक्षण स्थल, सार्वजनिक स्पेस कहीं भी घात लगाए हो सकता है। स्त्री पर अपराध किसी भी समय किसी भी उम्र में सिर्फ स्त्री होने के कारण हो सकता है। स्त्री पर यौनिक हिंसा के मामले उस घृणित सांस्कृतिक समझौते की तरफ इशारा करते हैं कि स्त्री महत्वहीन है ! उन्हें अपने को समेट-सिकोड़कर जीना सीखना चाहिए, उन्हें जीना है तो सीखना चाहिए कि उनकी उपस्थिति से पुरुषों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। यहाँ तक कि असुविधाओं की सूची में उन्हें होने वाली यौन उत्तेजना भी शामिल है! जिसके कारण ऐसी कहानियाँ प्रचलित की जाती हैं कि फलाँ व्यक्ति अपने पास स्त्री कर्मचारी या ऑफिसर को आने नहीं देता, उनसे नहीं मिलता! सामान्य तौर पर पुरुष सहकर्मी के व्यवहार में महिला सहकर्मी की उपस्थिति में सहजता नहीं दिखाई देती। कई शोध इस तरह के हुए हैं जिनमें पाया गया है कि पुरुष सहकर्मी आपस में जिस तरह की बातें करते हैं उसमें वे महिला सहकर्मी को सहज ही शामिल नहीं करते। यदि महिला सहकर्मी को बातचीत में शामिल करते हैं तो बातचीत का विषय एकदम अलग, औपचारिक या हल्का-फुल्का हो जाता है। आज के समय में संस्कृति को परिभाषित करने वाला तत्व मीडिया है। मीडिया के हस्तक्षेप के बिना कोई बहुत बड़ा सांस्कृतिक परिवर्तन इस समय संभव नहीं है। मीडिया यदि चाहे तो स्त्री के प्रति नजरिये में बदलाव ला सकता है। वह जानता है कि संस्कृति कैसे बदली जाती है। उसकी ताक़त बहुत है। अगर माध्यमों में स्त्री के प्रति नजरिये में गुणात्मक परिवर्तन आता है तो व्यवहार में भी यह दिखाई देगा। स्त्री से जुड़े मसलों पर, सामाजिक आदतों और रवैय्यों पर, मान्यताओं पर मीडिया का असर देखा जा रहा है। अगर यह बढ़े तो आशातीत नतीजे सामने आएंगे क्योंकि मीडिया के जरिए बहुत कुछ सीखा जा रहा है।
स्वाधीनताः
स्त्री के लिए स्वाधीनता के क्या मायने हैं? हमारे सरोकार का क्षेत्र स्त्री की स्वाधीनता के सवाल पर संविधान न होकर सामाजिक व्यवहार और मान्यताएँ हैं। जिस समाज में स्त्री की स्वाधीनता के लिए ‘जिमि स्वतंत्र होय बिगरहिं नारि’ कहा गया हो और उसकी पराधीन दशा की बदहाली को देखते हुए विधाता के द्वारा उसके बनाए जाने यानि जन्म पर ही सवाल खड़े किए गए हों कि जब परीधीन होकर सुख नहीं है तो विधाता ने स्त्री को सिरजा ही क्यों? ठीक वैसे ही यह कातर सवाल है जैसे कि जायसी के नाम से प्रचलित पद गीत में लड़की पिता से पूछती है कि ‘काहे को ब्याहे बिदेस, लखिया बाबुल मोरे/ भइया को दिहले बाबू महल दोमहला हमको दियो परदेस, लखिया बाबुल मोरे?’ यानि स्त्री की सामाजिक बदहाली और नारकीय जीवन को देखते हुए उसके जन्म या अस्तित्व को ही प्रश्नांकित करना जिससे जाहिर हो कि ऐसे जीवन से तो जीवन का न होना ही बेहतर है, स्त्रियों की सामाजिक दुर्दशा को दिखाता है। 19वीं शताब्दी में स्त्री का मुद्दा जब धार्मिक-सामाजिक सुधार आंदोलनों के एजेण्डे पर आया तो उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा शामिल नहीं थी। स्त्री स्वतंत्रता का प्रश्न तो अभी बहुत दूर था। स्त्री की स्वतंत्रता से जुड़े मसले बीसवीं शती में प्रमुखता से उभरकर सामने आते हैं। औपनिवेशिक दासता के युग में राष्ट्र की स्वतंत्रता की मांग और उसके लिए संघर्ष महत्वपूर्ण था। अन्य सभी चीजें आनुषंगिक थीं। एक तरफ देश की स्वतंत्रता की धारणा थी जिसके साथ किसी का विरोध नहीं था लेकिन अन्य समूह भी उसी परतंत्रता का अनुभव कर रहे थे जिनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। स्वतंत्रता का प्रश्न जितना समाज के लिए जरूरी था उतना ही व्यक्ति के लिए भी। इसका आरंभ परिवार से होना था, मुक्तिबोध ने परिवार के भीतर के असंतोष और असुविधा का विश्लेषण करते हुए लिखा है, ‘‘परिवार समाज की इकाई है, चाहे वह रूसी समाज हो या चीनी, हिन्दुस्तानी हो अथवा ब्रिटिश। अगर हमारे परिवार में असंतोष, विक्षोभ, अन्याय, भूख और दरिद्रता होगी तो निश्चय ही उनका असर नौजवान की मनोदशाओं और प्रवृत्तियों पर होगा। हमारे नौजवानों में जो आज छिछली रोमानी प्रवृत्ति, घुमक्क्ड़पन, गैरजिम्मेवाराना बर्ताव, खास तरह का फक्कड़पन, पलायनशीलता आदि दुर्गुण उत्पन्न होते हैं, तो इन प्रवृत्तियों का मूल हमारे परिवार में छाए व्यापक असंतोष में निहित है।’’ ‘‘लेकिन यहाँ तो यह स्थिति है कि नारी जिस घर में बंदिनी है, उसमें कोई खिड़की भी नहीं है – न तो हवा के लिए न प्रकाश के लिए। उसे तो अभी खिड़की भी खोलनी है। और संतोष की बात है कि नई शिक्षा ने मध्यवर्गीय घरों में भी प्रवेश किया। शिक्षा ने चारों ओर से बंद घरों में छोटी-सी खिड़की खोल दी। कवि की जो आकांक्षा थी कि कोई आँधी-तूफान आकर उस खिड़की को भी तोड़ दे, वह तो न हो सका, लेकिन खिड़की जरूर खुल गई, भले ही उस पर परदा भी टाँग दिया गया हो।’’ बीसवीं सदी के आरंभ में राजनीतिक स्वतंत्रता की जो स्वीकृति थी, वही स्त्री की स्वतंत्रता की नहीं थी। स्वयं अधिकांश स्त्रियों में इस बात को लेकर चेतना नहीं थी कि उनकी वर्तमान स्थिति में किसी प्रकार का सुधार या परिवर्तन संभव हो सकता है। लेकिन सन् 1920 के बाद तक प्रखर चिंतनशील स्त्रियों का एक पूरा समूह देश के कोने-कोने में तैयार हो जाता है जो उस समय प्रकाशित सभी पत्र-पत्रिकाओं में स्त्री की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थितियों पर टिप्पणी करने लगता है। महादेवी का प्रखर स्त्री-संबंधी चिंतन इसी चेतना की अगली कड़ी है। एक बड़ी सामाजिक त्रासदी को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में महादेवी देखती हैं, ‘‘इस समय हमारे समाज में केवल दो प्रकार की स्त्रियाँ मिलेंगी – एक वे जिन्हें इसका ज्ञान ही नहीं है कि वे भी एक विस्तृत मानव-समुदाय की सदस्य हैं और उनका भी एक ऐसा स्वतंत्र व्यक्तित्व है जिसके विकास से समाज का उत्कर्ष और संकीर्णता से अपकर्ष संभव है। दूसरी जो पुरुषों की समता करने के लिए उन्हीं के दृष्टिकोण से संसार को देखने में, उन्हीं के गुणावगुणों का अनुकरण करने में जीवन के चरम लक्ष्य की प्राप्ति समझती हैं। सारांश यह कि एक ओर अर्थहीन अनुसरण है तो दूसरी ओर अनर्थमय अनुकरण और यह दोनों प्रयत्न समाज की श्रृंखला को शिथिल तथा व्यक्तिगत बन्धनों को सुदृढ़ और संकुचित करते जा रहे हैं।’’ स्त्री के लिए सर्वाधिक कष्टप्रद स्थिति है, उसके स्वतंत्र व्यक्तित्व का न होना। स्त्री को विभिन्न सामाजिक स्थितियों में कंडीशनिंग की जाती है, उसे तैयार किया जाता है। स्त्री को सिर्फ दिए गए स्त्रीकरण के ढाँचे पर चलकर आदर्श स्थिति के पद तक पहुँचना होता है। आधुनिक समय में विषमता के प्रश्न को स्त्री और पुरुष की विषम सामाजिक स्थिति और जैविक भेद के रूप में देखा है। लेकिन विषमता का बड़ा कारण स्त्रियों में चेतना का अभाव है, यह एक नई दृष्टि है जो विषमता के प्रश्न पर महादेवी के यहाँ मिलती है, ‘‘असंख्य विषमताओं का कारण , स्त्री का अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व को भूलकर विवेकशक्ति को खो देना है। उसके बिना जाने ही उसका कर्त्तव्यपथ निश्चित हो चुकता है जिस पर चलकर न उसे सफलताजनित गर्व का अनुभव होता है, न असफलताजनित ग्लानि का। वह अपनी सफलता असफलता की छाया पुरुष की आत्मतुष्टि या असंतोष में देखने का प्रयत्न करती है, अपने हृदय में नहीं।’’ स्वतंत्रता एक भाव है जिसे अर्जित करना होता है। स्त्रियों ने अपनी सारी शक्ति और ऊर्जा स्वतंत्रता हासिल करने में नहीं बल्कि पुरुषों की छाया मात्र बनने, उनके सुख और उपभोग की सामग्री बने रहने और अपने व्यक्तित्व को पीछे धकेले रखने में किया है। उनमें अपार संयम और शक्ति है कि मनुष्य होते हुए भी मनुष्य होने के अधिकार से वंचित रहीं और विरोध नहीं किया। ‘‘वे बड़े से बड़ा त्याग प्राणों पर खेलकर हँसते-हँसते कर डालने पर उद्धत रहती हैं, परन्तु उसका मूल्य वही है जो बलिपशु के निरुपाय त्याग का होता है। वे दूसरों के इंगितमात्र पर किसी भी सिद्धांत की रक्षा के लिए जीवन की बाजी लगा देंगी, परन्तु अपने तर्क और विवेक की कसौटी पर उसका खरापन बिना जाँचे हुए; - अतः यह विवेकहीन आदर्शाचरण भी उनके विवेक को अधिक से अधिक संकुचित तथा समाज के स्वस्थ विकास के लिए अनुपयुक्त बनाता जा रहा है।’’ ‘‘दर्पण का उपयोग तभी तक है जब तक वह किसी दूसरे की आकृति को अपने हृदय में प्रतिबिंबित करता रहता है, अन्यथा लोग उसे निरर्थक जानकर फेंक देते हैं। पुरुष के अंधानुसरण ने स्त्री के व्यक्तित्व को अपना दर्पण बनाकर उसकी उपयोगिता तो सीमित कर ही दी थी, साथ ही समाज को भी अपूर्ण बना दिया।’’ स्वतंत्रता का प्रश्न अनिवार्यतः व्यक्तित्व के अर्जन से जुड़ा है। स्त्री की स्वतंत्रता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के बावजूद भी तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक कि स्त्री स्वयं इस चेतना से युक्त न हो और इसके लिए हर तरह का जोखिम उठाने के लिए तैयार न हो। स्त्री सामाजिक सांचों में किस प्रकार ढाली जाती है, उसे समाज किस प्रकार उसकी इच्छाओं के अनुरूप नहीं ढ़लने देकर अपनी अपेक्षाओं के अनुकूल बनाता है, इसकी बानगी देखिए- ‘‘मन माँग रहा था रहा था विस्मय जग माँग रहा था पीड़ा !’’ स्त्री के लिए अपने मन की और बाहर की दुनियाओं में कोई मेल नहीं है। बाहरी दुनिया से स्त्री की दुनिया का अंतर्विरोध उसके बालजीवन से ही आरंभ हो जाता है। स्त्री के बिना संसार का काम नहीं चल सकता, स्त्री भी संसार में ही अपनी सार्थकता ढूँढ सकेगी लेकिन यह विषम और अंतर्विरोधी संबंध है। स्त्री का संसार उसके किशोरी और युवती होने के साथ साथ ही सिकुड़ने लगता है। उसका सामाजिक स्पेस अनेक चीजों के नाम पर – कभी भय, कभी उसकी सुरक्षा की चिंता, कभी नैतिकता, कभी सामाजिक आचरण के नाम पर उससे छिनता चला जाता है और उसकी सीमा बना दी जाती है। वह सीमा या बंधन भी अत्यंत सीमित दायरे वाला होता है – ‘‘जाती नवजीवन बरसा जो करुण घटा कण-कण में, निस्पन्द पड़ी सोती वह अब मन के लघु बंधन में!’’ स्त्री के जीवन में समाज से जो प्राप्त है उसमें तथाकथित सुख की मात्रा कम और दुख की मात्रा ज़्यादा है। इन दोनों के बीच सामंजस्य बैठाते हुए स्त्री के जीवन और ऊर्जा का बहुत बड़ा अंश रीत जाता है। यह रीतना अनुत्पादक है। इसका किसी भी तरह का सृजनात्मक मूल्य न तो समाज के लिए है न ही स्त्री के लिए।
जो सीमा उसके लिए बना दी जाती है, वह इतनी कठोर होती है कि महादेवी ने अपने गद्य में उसे जीवित समाधि कहा है। स्त्री की सार्वजनिक गतिविधियों को सीमित करके उसके व्यक्तित्व के विकास की संभावनाओं को समाप्त कर दिया जाता है। बहुत से भाव जिनमें जोखिम, साहस, संघर्ष, बहुत सी क्रियाएँ जिनमें स्वप्न, इच्छा, निर्णय आदि पनपने ही नहीं पाते। स्त्री केवल भय, असुरक्षा, संशय, साहसहीनता जैसे भावों और संघर्षरहित सुरक्षित जीवन की परिकल्पनाओं में जीने को अभिशप्त है। परिस्थितियों से निर्द्वन्द्व टकराकर, उनसे उलझते-जूझते, निर्णय लेते हुए स्त्री का जिस प्रकार व्यक्तित्व बन सकता था वह उसके लिए सीमा निर्धारित कर देने पर नहीं बन सकता। स्त्री के जीवन का सबसे बड़ा कष्ट है कि उसका अतीत और भविष्य उसका नहीं। उसकी समस्त अनथक चेष्टाएँ, सारा श्रम जो उसने समाज के लिए किया है उन जरा सी सहूलियतों की तुलना में कहीं ज़्यादा है जो समाज ने स्त्री के लिए छोड़ा है। स्त्री का अपने श्रम और दाय के वैभव से अपरिचय इतना बड़ा है कि वह अपनी वर्तमान की किसी भी तरह की उपलब्धि पर गर्व महसूस नहीं करती। सब चीजों को, यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को लेकर भी, एक उदासीनता और विरक्ति स्त्री के व्यवहार में चुपचाप शामिल हो जाती है। सब कुछ करके भी वह उन कार्यों का श्रेय किसी और को देना चाहती है। और समाज उसके कार्यों का श्रेय स्वयं लेते समय भी एहसान जताकर लेता है। उसकी हर तरह की क्षमता पर संदेह व्यक्त कर उसके व्यक्तित्व को छोटा बताने की कोशिश की जाती है। यह स्थिति एक दिन में पैदा नहीं होती, न ही स्त्री की उपलब्धियों को लेकर सामाजिक संदेह की ज़ेहनियत एक दिन में बनती है। इसकी लंबी सांस्कृतिक परंपरा है जो स्त्री के खिलाफ सक्रिय है। स्त्री की जो चाहना है, उसमें पूरी क़ायनात शामिल है। उसे किसी की निग़हबंदी में नहीं खोजा जा सकता। बड़ी चीज की खोज और इच्छा के लिए स्वतंत्र प्रयास की जरूरत है। निर्देशित प्रयास अंततः अपनी सीमा ही प्रकट करेंगे। स्त्री की यह चाहना स्वतंत्रता की चाहना है जिसके आलोक में वह अपना व्यक्तित्व निर्मित कर सके और उसकी चुनौतियों के लिए भी तैयार हो सके। स्त्री की इच्छा किसी स्वप्नलोक को हासिल करने की नहीं, वह यथार्थ से सीधे संवाद है। स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व के लिए कोई सीमा नहीं होनी चाहिए।
‘‘हों मेरे लक्ष्य-क्षितिज की, आलोक-तिमिर दो छोरें !’’
………………………….
किताबें
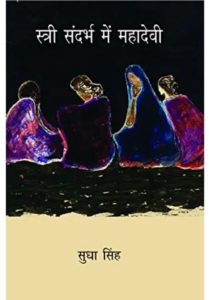

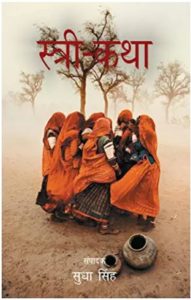



………………………….
विडियो
………………………….
