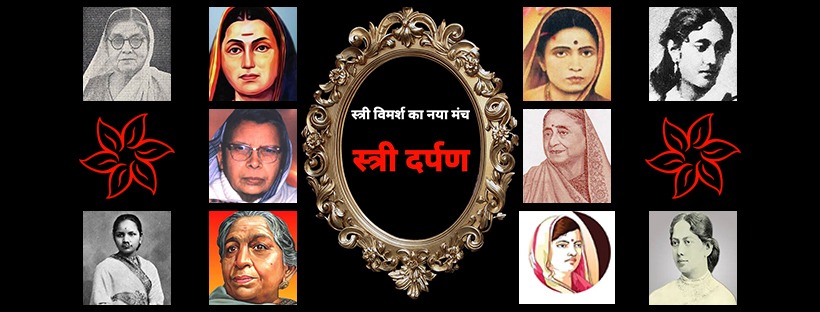मित्रो। क्या आपको आर्मेनिया के भीषण जनसंहार के बारे में पता है?शायद नहीं पता होगा।बीसवीं सदी के इतिहास की यह क्रूरतम घटनाओं में से एक है। अगले रविवार को आर्मेनिया जनसंहार के 107 साल पूरे होनेजा रहे हैं।इस जनसंहार पर हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री सुमन केशरी की एक किताब आ रही है।।अभी हाल ही में उनका नाटक “गांधारी” भी आया है जो चर्चा में है।तो पढ़िये इस जनसंहार पर उनका यह आलेख।
क्यों याद करें आर्मेनियाई जनसंहार को?
-सुमन केशरी

24 अप्रैल 2015 को आर्मेनियाई जन-संहार के सौ वर्ष पूरे हो गए… हममें से कितनों को याद है यह?
‘आखिर आज कौन आर्मेनियाइयों की हत्या और तबाही की बात करता है?’
-एडोल्फ़ हिटलर, सन् 1939
ऐसा माना जाता है कि ऑटोमन साम्राज्य (वर्तमान तुर्की) द्वारा, 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभिक तीन दशकों में किए आर्मेनिया के भीषण जनसंहार पर टिप्पणी करते हुए सन् 1939 में हिटलर ने यह कहा था।
इतिहास गवाह है कि खुद हिटलर ने यहूदियों और अपने विरोधियों का संहार अत्यंत निर्ममतापूर्वक किया था। आज भी “हिटलर” के नाम भर से रीढ़ में सिहरन होजाती है…पर आर्मेनियाई जन संहार? इसे विडंबना ही कहेंगे कि आज भी विश्व में या खुद भारत वर्ष में कितने लोग आर्मेनिया और आर्मेनियाई जनसंहार के बारे में जानते हैं? तथ्य तो यह है कि कई लोग तो इस देश के अस्तित्व तक से अनभिज्ञ हैं। जबकि सच्चाई यह है कि आर्मेनियाई जनसंहार को निर्विवाद रूप से बीसवीं सदी का पहला जनसंहार कहा जा सकता है!
प्रथम विश्वयुद्ध के पहले ऑटोमन साम्राज्य में करीब 20 लाख आर्मेनियाई रहते थे और उनमें से करीब 15 लाख आर्मेनियाई ई.सन् 1915-1923 के बीच मार डाले गए और बाकी लगभग 5 लाख आर्मेनियाई वहाँ से पलायन करने के लिए बाध्य हो गए। तुर्की ने आज तक इस जनसंहार को स्वीकार नहीं किया। आज भी भारत समेत संसार के अधिकांश देश चुप हैं। इस पुस्तक को तैयार किए जाने तक आर्मेनियाई जनसंहारको स्वीकृति देने वाले कुल 34 देश हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट में दी गई है।फरवरी 2020 में सीरिया तथा हाल ही में 12 दिसंबर2019 को अमेरिका के सीनेट ने आर्मेनियाई जनसंहार को मान्यता दी है। जिन प्रमुख देशों ने मान्यता दी है वे हैं- अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, नीदरलैंड, सीरिया बोलीविया, चिली आदि। तुर्की में प्रसिद्ध आर्मेनियाई पत्रकार हरान्त दिन्क की 2008 में हत्या के विरोध में “मैं क्षमाप्रार्थी हूँ” अभियान भी लगातार चलाया जा रहा है।यहाँ नोबेल पुरस्कार विजेता उपन्यासकार ओरहान पामुक को भी याद करना जरूरी है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सवाल को उठाते हुए आर्मेनियाइयों के जनसंहार पर तुर्की की खामोशी को प्रश्नांकित किया। कार्स में आधारित उनके उपन्यास “ स्नो” में भी इसकी छाया दिखाई पड़ती है।
किंतु तुर्की शासकवर्ग के अनुसार आर्मेनियाइयों पर हुआ अत्याचार दरअसल तहक़ीर कानून और प्रथम विश्वयुद्ध का परिणाम था। उसे जनसंहार नहीं कहा जा सकता!
यूँ तो कानूनी रूप से “तहक़ीर” अर्थात् “स्थानांतरण” 27 मई 1915 को लागू किया गया, किंतु 24 अप्रैल 1915 को, तलत पाशा के आदेश पर आंतरिक मामलों के तत्कालीन मंत्री महमद पाशा बे ने कॉंसटेंटिनोपॉल (आज का इस्तांबुल) में सैकड़ों बुद्धिजीवियों, कलाकारों, नेताओं, डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों और बड़े व्यापारियों आदि को निर्वासित कर या तो मरवा दिया था, अथवा उन्हें कैद कर लिया गया था। चूंकि अपने अधिकांश बुद्धिजीवियों और नेताओं को एक राष्ट्र ने एक रात में ही खो दिया था, इसीलिए 24 अप्रैल को “आर्मेनियाई जनसंहार दिवस” के रूप में याद किया जाता है। 1915 से लेकर 1923 तक के कुल आठ सालों में एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता की उन्नत कर्मठ आबादी ने अपने 15 लाख लोग खो दिए। कहते हैं कि आज विश्व में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले ही आर्मेनियाई परिवार होंगे, जिन्होंने अपने किसी सदस्य को न खोया हो, वरना तो इस जनसंहार में अनेक परिवारों ने अपने किसी न किसी सदस्य को गंवाया ही है। सारा राष्ट्र कुछ खो जाने की पीड़ा से व्यथित है। इस भयानक जन संहार के एक सौ पाँच वर्ष हो गए, किंतु एक राष्ट्र है,जो आज भी विश्व से न्याय मांग रहा है!
यूँ तो आर्मेनियाइयों की हत्या और निर्वासन का दौर बहुत पहले से शुरू हो गया था। पर हम शुरुआत करते हैं, उन्नीसवीं सदी के अंतिम दशक से। 1890 के दशक में आर्मेनियाई क्रांतिकारी फ़ेडेरेशन, डाशनाक्त्सुथ्यून ने आर्मेनियायियों को स्वायत्तता प्राप्ति के लिए एकजुट करने की कोशिश के साथ ही तत्कालीन सत्ता के विरूद्ध फ़ियादीन भी बनाए। यह राष्ट्रवादी विचारधारा के पनपने का काल था। यह सुल्तान अब्दुल हामिद द्वितीय के शासन के कमजोर होकर टूटने का भी समय था। ऐसी हालत में सुल्तान ने 1894-96 के बीच स्वायतत्ता और अधिकार मांगने के आरोप में हजारों-हजार आर्मेनियाइयों को मौत की घाट उतार दिया। किंतु स्थितियाँ इससे बदली नहीं और बेहतर शासन के लिए सारे साम्राज्य में अब्दुल हामिद के निरंकुश राजशाही के खिलाफ़ युवा तुर्कों द्वारा जब विद्रोह शुरू हुआ तो उसमें आर्मेनियाइयों ने बढ़-चढ़ कर इस उम्मीद के साथ हिस्सा लिया कि वे एक लोकतांत्रिक शक्ति का साथ दे रहे हैं, जो अल्पसंख्यकों के हितों की भी रक्षा करेगा। पर हुआ इसका उल्टा ही क्योंकि प्रथम विश्वयुद्ध का माहौल बन चुका था और ऑटोमन साम्राज्य, जर्मनी-इटली के जिस खेमे के नजदीक था उसमें कट्टर राष्ट्रवाद के बीज अंकुरित होने लगे थे। दरअसल युवा तुर्क अपने हथियार वहीं पैना करना सीख रहे थे और प्रथम विश्वयुद्ध ने तुर्कों को आर्मेनियाइयों को सबक सिखाने का यह मौका दे दिया।
दुर्भाग्य से सामरिक महत्त्व के भूखंड में स्थित होने के कारण, ऐतिहासिक रूप से आर्मेनियाइयों का निवास माने जाने वाले पूर्वी भाग पर रूस और पश्चिम में ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा हो गया था। आर्मेनियाई मुख्यतः ईसाई और एपोस्टोलिक चर्च के अनुयायी हैं। पहली सदी में ही आर्मेनियाई एपोस्टोलिक चर्च की स्थापना हो गई थी और 301 ईस्वी में आर्मेनिया दुनिया का पहला राज्य था, जिसने ईसाइयत को राज्यधर्म का दर्जा दिया। दूसरी ओर ऑटोमन साम्राज्य की बहुसंख्यक आबादी मुसलमान थी। ऐसे में जब दो परस्पर युद्धरत देशों का कब्जा, अल्पसंख्यक नस्ल अथवा जातीयता पर होता है, तो अमूमन उस अल्पसंख्यक नस्ल के लोगों का देशप्रेम संदेह का विषय बन जाता है। और अगर धर्म भी जुदा हों तो संदेह को और अधिक पुख्ता आधार मिल जाता है। आर्मेनिया इसका अपवाद न हो सका। जब ऑटोमन साम्राज्य, रूस के खिलाफ़ युद्ध में उतरा तो पूर्वी इलाकों में रहने वाले आर्मेनियाइयों से अपेक्षा की गई कि वे रूस का साथ छोड़ कर ऑटोमन का साथ देंगे। ऐसा न होने पर युवा तुर्कों को आर्मेनियाइयों के दमन का ठोस बहाना मिल गया। याद रहे कि 1913-1918 तक युवा तुर्कों की कमान मुख्यतः तीन पाशाओं- एनवेर पाशा, तलत पाशा और जेमाल पाशा के हाथ में थी। वे घोर राष्ट्रवादी थे और जर्मनी के बहुत निकट थे। प्रथम विश्वयुद्ध में तुर्की जर्मनी के साथ था जबकि रूस उसके खिलाफ़ मित्र राष्ट्रों के साथ था। ऑटोमन साम्राज्य में आर्मेनियाई समस्या को “अंतिम रूप” से हल करने के उपाय खोजे जा चुके थे। और शुरुआत हुई 24 अप्रैल 1915 को, नेताओं- बुद्धिजीवियों-व्यापारियों आदि के दमन के रूप में। एक बार फिर इसे रेखांकित करने की जरूरत है कि कहा जाता है कि हिटलर ने अपने कुख्यात ‘फ़ाइनल सोल्यूशन’ की प्रेरणा यहीं से ली थी।
इसके बाद, हजारों आर्मेनियाई पुरूषों को सेना में भर्ती के नाम पर इकठ्ठा किया गया। इनमें किसान, अध्यापक, दुकानदार, चरवाहे सब मौजूद थे। हुक्म हुआ था कि वे जैसे और जहाँ हैं, चले आएँ। वे आए तो फिर न लौट पाए और न उन्हें अलविदा कह पाए, जो उनकी राह देख रहे थे। जो देख रहे थे राह उनमें से भी कुछ ही बचे अपना हाल सुनाने को। पकड़े गए पुरुष सैनिक नहीं बनाए गए, बावजूद इसके कि तुर्की सेना को सैनिकों की जरूरत थी। वे बनाए गए मजदूर और हम्माल। काम कर पर मांग न कर। वे भूख और जहालत से तड़प कर बीमार पड़ते तो उन्हें या तो मार डाला जाता या वे रास्ते में तड़प-तड़प कर मर जाते। यही नहीं हजारों को तो रास्ते में ही जलाकर-तड़पाकर मार डाला गया।
क्रूरता यहीं नहीं रुकी। बचे हुए तमाम बूढ़ों, बच्चों और औरतों को सीरिया के रेगिस्तानों की ओर जाने का हुक्म दे दिया गया। अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए औरतों-बच्चों के साथ दुनिया भर की सत्ताएँ जो करती हैं, उनसे भला ऑटोमन कैसे अछूते रहते। तो तुर्की सैनिकों के साथ-साथ वे कुर्दों और दूसरे कबीलों द्वारा भी उत्पीड़ित किए गए और भुखमरी,अकाल और महामारियों का शिकार हुए। कइयों ने गिरजाघरों या रास्ते में पड़े भवनों या खलिहानों में पनाह ली तो उन्हें वहीं जला दिया गया। बिटलिस, आकन और खापेर्त जिलों में हजारों बच्चों को जिंदा भूना गया और कइयों को जहर भी दे दिया गया। यूफ़्रेटस नदी में डुबाने और काट कर फेंक देने की घटनाएँ भी सामने आई है। कहते हैं कि यूफ़्रेटस का पानी लाल हो गया था। इस बात के भी संकेत हैं कि हजारों औरतो-बच्चों का बलपूर्वक धर्म-परिवर्तन भी करवाया गया। यही नहीं उस दौरान खड़ी फसलों को तहस-नहस कर दिया गया। नष्ट होने वालों में केवल आर्मेनियाई ही शामिल नहीं थे वरन् असीरियन, यूनानी और अन्य अल्प-संख्यक भी थे।
आर्मेनियाइयों के नरसंहार को पूरी सदी बीत गई, दुनिया कहीं की कहीं पहुँच गई। इन सौ सालों में कई साम्राज्य और उपनिवेश प्रत्यक्षतः अपने स्पष्ट रूप में तो समाप्त हो ही चुके हैं। दुनिया, संप्रभुता संपन्न राष्ट्रराज्यों की व्यवस्था में प्रवेश कर चुकी है। समाज-कल्याण के क्षेत्र में, टेक्नालॉजी के सहारे बेहतर जीवन संभव करने के क्षेत्र में, इन सौ सालों में हुई तरक्की को कौन नकार सकता है?
लेकिन क्या यह तरक्की हर धरातल पर मानवीय संवेदना की प्रगति भी दर्शाती है? क्या दुनिया आर्मेनियाइयों, यहूदियों के जनसंहार से सीख कर जनसंहार-मुक्त, क्रूरता-मुक्त होने की दिशा में भी आगे बढ़ी है?
ऐसी मुक्ति संभव करने के इरादे से ही, दूसरे महायुद्ध की पृष्ठभूमि में संयुक्त राष्ट्र ने 1948 में जातिनाश संबंधी करार मंजूर किया, जो 1951 से लागू हुआ। जुलाई 2019 तक 152 देश इसे स्वीकार कर चुके थे। जातिनाश की मूल धारणा के विभिन्न रूपों को यह करार परिभाषित करता है। इसके अनुसार किसी समुदाय के सदस्यों की हत्याएँ करना, उन्हें शारीरिक या मानसिक यंत्रणा देना, जानबूझ कर ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न करना जिनके कारण कोई समुदाय आंशिक या पूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, समुदाय में बच्चों के जन्म की संभावनाए समाप्त करने वाले कदम उठाना, बच्चों को जबरन किसी और समुदाय के हवाले करना—-यह सब जातिनाश की इस परिभाषा में समाहित है। स्पष्ट है कि सैद्धांतिक रूप से संयुक्त राष्ट्र—-दूसरे शब्दों में दुनिया के अधिकांश देश—यह मान चुके हैं कि जातिनाश केवल बड़े पैमाने पर होने वाली हिंसा का नहीं, बल्कि खास तरह के मिज़ाज का मामला है। इस मिज़ाज या मानसिकता के शिकार किसी ऐतिहासिक पल में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो किसी अन्य पल में संभवत: कुछ कम लोग। लेकिन, संयुक्त राष्ट्र की आम राय साफ़ है: बात पैमाने की नहीं इरादे की है।
क्या हम कह सकते हैं कि आर्मेनियाई जनसंहार के सौ साल बाद, और इस करार की मंजूरी के सत्तर से ज्यादा साल बाद, मनुष्य की चेतना में जातिनाशी प्रवृत्तियाँ पूरी तरह समाप्त हो गईं हैं, या निर्णायक रूप से कम हो गईं हैं?
मनुष्य के बारे में बहुत नकारात्मक रवैया अपनाए बिना भी इस दुःखद तथ्य से मुक्ति संभव नहीं कि जातिनाश और क्रूरता की मनोवृत्ति अभी भी हमारे मन में बहुत गहरी पैठी हुई है। 1945 के बाद अनेक घटनाएँ जातिनाश की परिभाषा के दायरे में आएँगी ही, पैमाने के लिहाज से बात करें तो भी स्थितियाँ बहुत संतोषजनक नहीं हैं, इंडोनेशिया, बांगलादेश, कंबोडिया, सोमालिया, रवांडा, बोस्निया, ईराक और सीरिया… और न जाने कितनी जगहों पर जातिनाश के मामले सामने आए हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यहूदियों पर अत्याचार के निराकरण के प्रायश्चित-स्वरूप गढ़ा गया राष्ट्र-राज्य इज़राइल स्वयं जातिनाशी मानसिकता की गिरफ़्त में है। हम फ़ीलीस्तीनियों के मारे जाने की खबरें लगभग रोज ही पढ़ते हैं।
ऐसा नहीं कि जातिनाशपरक मिज़ाज और इससे प्रेरित नस्लपरक- संप्रदायपरक हिंसा किसी एक विचारधारा तक ही सीमित है। नस्ल की हो, देश की हो या विचार की, शुद्धता के नाम पर भयानक हिंसा को तरह तरह के लोग जायज ठहराते रहते हैं। कितनी ह्रदय-विदारक सचाई है कि सारी प्रगति के बावजूद मनुष्यता के मन के किसी कोने में अकल्पनीय क्रूरता लगातार निवास करती है। जातिनाश की मानसिकता केवल हिंसा की नहीं मनोविकृति की मानसिकता है। आखिर उस व्यक्ति को मानसिक रूप से स्वस्थ कैसे माना जा सकता है, जिसे लोगों को जिन्दा जलाने में सुख मिलता हो, जिसे बच्चों के सामने माँओं के साथ बलात्कार करने में, गर्भवतियों के गर्भ से बच्चों को खींच लेने में मर्दानगी महसूस होती हो? उस विचार या भावना को कैसे मानवीय माना जा सकता है जो इस तरह की क्रूरता को जायज़, बल्कि जरूरी मानता हो? यह भी ध्यान देने की बात है कि ऐसी क्रूरता का शिकार औरतों को बनाने में जातिनाशी मर्दानगी बहुत सार्थकता महसूस करती है, और खुद औरतें भी ‘अन्य’ के विरुद्ध ऐसी जातिनाशी हिंसा और क्रूरता का समर्थन करती देखी जातीं हैं। औरत हो या मर्द, किसी को विचार के नाम पर रूस, चीन और कंबोडिया में हुई हिंसा जायज़ लगती है तो किसी को अपने देश में हो रही भीड़-हत्याओं से कोई समस्या नहीं होती।
सच कहें तो समस्या की जड़ यही है। जब हम राष्ट्र या विचार के नाम पर मूलभूत मानवीय नैतिकता और सहज विवेक से कतराने लगते हैं, तब -मेरा देश ( या विचार) सही या गलत…मुझे तो हर हाल में समर्थन ही करना है—की मानसिकता की जकड़ में आ जाते हैं। हिंसा करने वालों से कहीं ज्यादा चिंताजनक है, उनकी मानसिकता, जो हिंसा और क्रूरता को जायज़ ठहराते हैं। सांप्रदायिक हिंसा की जिम्मेवारी जो लोग “गुंडों” पर डाल कर फ़ारिग हो लेना चाहते हैं, उन्हें गांधीजी बारंबार याद दिलाते थे कि ‘ गुंडे आकाश से नहीं आ टपकते, न ही वे जमीन फाड़ कर निकल आते हैं, उन्हें समाज ही पालता है, हमीं बढ़ावा देते हैं’।
जातिनाशी मानसिकता के विष-बीज नफ़रत की जमीन में पनपते हैं, क्रूरता इन बीजों का फल है। इसका इलाज बदला नहीं है, बदलाव है। जो हुआ, उसे स्वीकार करने का अर्थ यह नहीं कि बदले की वकालत की जाए। आर्मेनियाइयों का जातिनाश और जनसंहार हो या यहूदियों का, या किसी भी समुदाय का, उसे नकारने से न तो वह गायब हो जाएगा, न उसकी यादें। बेहतर यही है कि जिसे इसका सामना करना पड़ा, वह और जिसके नाम पर यह किया गया दोनों समुदाय नये सिरे से संवाद के जरिए, विवेक और संवेदना के आधार पर आपसी संबंधों का निर्धारण करें।
ऐसा न करने पर हम कितनी भी प्रगति कर लें, क्रूरता हमारे स्वभाव में कभी खुलेआम कभी छुप-छुपा कर बैठी ही रहेगी…
(“आर्मेनियाई जनसंहार: ऑटोमन साम्राज्य का कलंक” के सुमन केशरी द्वारा लिखे संपादकीय का एक हिस्सा। जनसंहार को मुख्यतः साहित्य के माध्यम से देखने का प्रयास है। यह अलग बात है कि जनसंहार को समझने के लिए व्यक्तिगत अनुभव, तथा जनसंहार संबंधी सोच व विमर्स का भी अनुवाद इसमें शामिल है।पहली बार किसी भारतीय भाषा में आर्मेनियाई साहित्य की इतनी विपुल सामग्री का अनुवाद सीधे आर्मेनियाई भाषा से किया गया है, और यह संभव हो सका,सुश्री माने मकर्तच्यान के सहयोग से। माने मूलरूप से आर्मेनियाई हैं तथा वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से हिंदी में पीएच डी कर रही हैं। इससे पूर्व उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिन्ही ऑनर्स की पढ़ाई की है। सुश्री माने मकर्तच्यान इस पुस्तक की सह संपादक हैं।)
प्रस्तुत हैं इस नरसंहार पर सुमन केशरी की दो कवितायें
—————
1.लथपथ आर्मेनिया
—————
वह ढूँढ रही है अपनी बच्ची को जिसे वह खाई में पड़ी पाट पर छोड़
चली गई थी खेत में
उस आदमी के बुलावे पर
बावजूद इसके कि
वह उन्हीं में से था
जिनसे छिपी भाग रही थी अब तक
उस आदमी के हाथ में रोटियाँ थीं और
औरत के पेट में इतनी भूख
कि उसे मंजूर था
बच्ची को पाट पर लिटा
उसके पीछे
खेतों में चली जाना
भूख से यूँ भी बच्ची उससे ज्यादा अधमरी थी
जितनी वह औरत जिसके स्तनों में अब दूध का बूंद भी न बचा था
किंतु जान कुछ ज्यादा थी
और शरीर में अब भी उभार और कटाव बाकी थे
बावजूद कई दिनों के फाके के
और भूखी अंतड़िया लिए
चलते रहने के मीलों-मील
जाने कैसे तो वह अब तक साबुत बची थी
और उस आदमी को दिख गई थी एक साबुत औरत
चेहरे से साबुत
अपनी चाल में साबुत
रोटियों की जादूगरी में बंधी वह औरत
बस इतना जानती थी
कि उसे एक बार
भरपेट रोटी खानी थी
और फिर सोना था
अपनी बच्ची का सिर अपनी बाँह के तकिए पर रख
उसके होठों को स्तन से लगा कर
शाम ढलने पर
दुहरी होकर लौटी औरत
ढूँढ रही है
अपनी बच्ची को
जिसका नाम तक उसे याद नहीं
यह भी याद नहीं
किस खाई में पड़े पाट पर
लिटाया था उसने
उस माँसपिंड को
हाँ खून को सूंघ कर
गीदड़-सियार लपक रहे हैं
गिद्ध मंडरा रहे हैं
सूरज तो कब का डूब चुका
चाँद-तारे तक निकलने
से घबरा रहे हैं
और अब यह कलेजा चीरती
चीख!
—————
2.हमने रचे प्रेमगीत संगीनों के सायों तले…
————–
वे प्रेमगीत रचने के दिन नहीं थे
खदेड़े जा रहे थे हम
अपने घरों से
गलियों से
गाँवों से
कस्बों से
झुंड के झुंड चले जा रहे थे हम
एक नामालूम दिशा में..
कालखंड में..
रास्तों में हमने अपने ही लोगों को देखा
सियारों के मुँह में
देखा सूरज को छिपते
गिद्धों के पीछे
देखी खून और माँस-पिंडों की बरसात होते
देखे खून के ताल
नदियाँ देखीं लाल लाल
वे प्रेम करने के दिन न थे
वे दिन न थे प्रेमगीत रचने के
हम जानते थे
हमारी देहगंध उनमें
चाह नहीं
घृणा ही भरेगी
क्रोध से तमतमाने लगेंगे उनके चेहरे
अंग-प्रत्यंग उनके हथियार हो जाएंगे
हमारे लिए
भूमि कब्रगाह हो जाएगी हमारे लिए
हवा भारी होगी लोथरों की बू से
तब हमने प्रेमगीत रचा
ऐन उन आग उगलती आँखों के सामने
उसने मुझे फूल दिए कुछ जंगली
और
मेरे होठों को इबादत-सा छुआ
उसने मेरी देह में चाहत के बीज बोए
ऐन संगीनों के साए में
इस तरह अपनी उम्मीदों को हमने
चकमक-सा छिपाए रखा
अपने हृदय में…