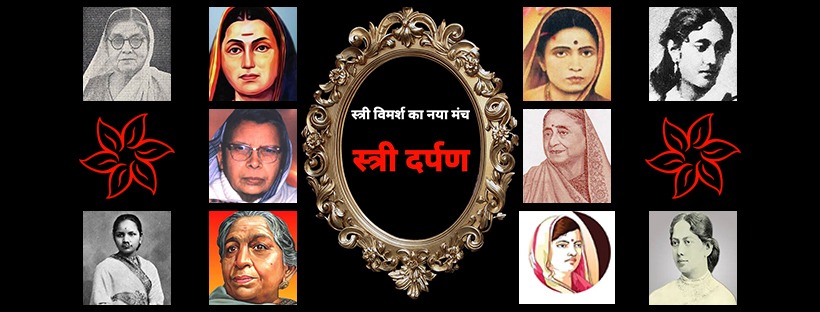आज की पीढ़ी गोपेश जी को नहीं जानती होगी तो उनकी पत्नी को क्या जानेगी। आज गोपेश जी जीवित होते तो 97 वर्ष के होते। निराला फिराक की सोहबत में जीनेवाले गोपेश जी को इलाहाबाद की साहित्यिक बिरादरी बहुत प्रेम करती रही।
मित्रो आपने अब तक 42 से अधिक लेखकों की पत्नियों के बारे में पढ़ा। आज पढ़िए मास्कों रेडियो में कार्यरत प्रसिद्ध कवि गीतकार अनुवादक गोपी कृष्ण गोपेश जी की पत्नी के बारे में जो इलाहाबाद की प्रसिद्ध संस्था परिमल के संस्थापक सदस्य थे। उनका जीवन निराला फिराक रामकुमार वर्मा जैसे लोगों की सोहबत में बीता और धर्मवीर भारती विजय देव नारायण साही जैसे लोग उनके मित्र थे। गोपेश जी मंचों पर बच्चन और नीरज के साथ कविताए पढ़ते थे। वे रूसी भाषा के प्रोफेसर भी थे और बीसेक रूसी किताबों के अनुवाद भी किये थे।
गोपेश जी की विदुषी बेटी डॉक्टर अनीता गोपेश ने अपनी माँ पर यह संस्मरण लिखा है जो प्राणिशास्त्र में प्रोफेसर होने के साथ साथ प्रसिद्ध कहानीकार उपन्यासकार और नाटककार रही हैं। वह अपने पिता की तरह प्रतिभाशाली हैं और रूसी फ्रेंच की जानकार है। तो पढ़िए उनका संस्मरण।
“स्नेहलता गोपेश: कवि, अनुवादक गोपीकृष्ण गोपेश की सहचरी, मेरी माँ”
………………………

………………………

अनिता गोपेश
सुप्रसिद्ध साहित्यकार, कवि, विश्वविख्यात महाग्रन्थों के अनुवादक तथा रूसी भाषा के प्राध्यापक श्री गोपीकृष्ण गोपेश की पत्नी स्नेहलता गोपेश के बचपन का नाम ‘‘रामकुँवरि’’ था जो गोरखपुर के उनके मायके में बिगड़ते बिगड़ते ‘‘राम कुँवर’’ हो गया था। मैं उनसे पूछती कि ‘‘ये कैसा नाम है? आप कहती हैं नाना ने बहुत सोच समझकर ये नाम दिया था।’’ वे जवाब देतीं ‘‘और क्या! ये नाम उन्होंने रामायण से लिया था। राम के दो भाइयों की पत्नियों का नाम उन्होंने हम बहनों का रखा था- उर्मिला, सुस्कीर्ति और रामकुँवरि। रामकुँवरि सीता का नाम था।’’ स्नेहलता नाम उन्हें विवाह के बाद पति गोपेश ने दिया था जो जीवन भर मान्य रहा।
उनका जन्म गोरखपुर के एक संभ्रांत, समृद्ध पुरोहित पंडित गोपाल शरण शर्मा की तीसरी पुत्री के रूप में हुआ। वह समय ऐसा था जब बेटियों के जन्म की तिथि, समय आदि का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता था। उनकी जन्म पत्री भी केवल विवाह में मिलाने के लिए बनवाई जाती थी। बेटे की प्रत्याशा में हुई तीसरी बेटी का लालन पालन उन्होंने एक लड़के की तरह किया और तमाम विरोधों के बावजूद रामकुँवरि को पिता ने ईसाईयों के मिशनरी स्कूल में नवीं कक्षा तक पढ़ाया।
अपनी दो पुत्रियों का विवाह सम्पन्न घरानों में बहुत सोच समझ कर करने के बावजूद जब पंडित गोपाल शरण शर्मा की बेटियों का वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहा तो उन्होंने संकल्प लिया कि अपनी तीसरी पुत्री का विवाह वे घराना नहीं, बल्कि प्रतिभाशाली सुपात्र देखकर करेंगे। मेरे पिता ‘‘गोपेश’’ जिनका ये उपनाम तब तक नहीं पड़ा था, विपन्नता में रहते हुए भी कुशाग्र बुद्धि, पढ़ाई में तेज और तत्कालीन समाज में अपनी पहचान बनाने में लगे थे। बरेली के फरीदपुर कस्बे से जब वे शिक्षा लेने निकले तो उन्होंने सीधे इलाहाबाद की राह पकड़ी। पीछे-पीछे उनके पिता भी चले आए। ऐसे में बाप-बेटे की गृहस्थी, किसी तरह चल रही थी। उनका घर बहुत खस्ता हाल था। गोपेश की माँ का निधन तभी हो गया था, जब गोपेश 40 दिन के थे। फरीदपुर में उनकी बुआ ने उनको पाला था। सो इलाहाबाद में परिवार के नाम पर सिर्फ बाप-बेटे और घर के नाम पर इलाहाबाद के पुराने मुहल्ले रानी मंडी में किराये की एक कोठरी, खपरैल वाली और एक सामूहिक स्नानागार भर था। किसी मध्यस्थ के चलते पंडित गोपाल शरण शर्मा की पुत्री रामकुँवरि का विवाह किशोर गोपीकृष्ण से सम्पन्न हुआ। उनके विवाह की तिथि और वर्ष का तो पता नहीं पर यह सुना था कि जब विवाह हुआ तब गोपेश 17 साल के और मेरी माँ 13 साल की थीं। सम्भवतः उनका विवाह 1943 में और गौना 1945 में हुआ था। सम्पन्न परिवार में पली-बढ़ी कन्या जब पहली विदाई के बाद ससुराल से मायके गयी तो उसने ससुराल जाने से इंकार कर दिया। खाते-पीते खुशहाल परिवार से आई किशोरी स्नेहलता का मन वहाँ कैसे लगता! पर सुसंस्कारी पिता ने प्रतिभावान पति के उज्ज्वल भविष्य की उम्मीद बंधा उन्हें घर गृहस्थी जमाने की ज़िम्मेदारी उठाने की बात समझा उनके ससुराल भिजवाया। आने के बाद उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी सँभाली और ऐसे सँभाली कि संघर्षों में कभी ‘उफ़’ न किया। 13-14 साल की किशोरी को समझाया गया- ‘‘अब वही तेरा घर है – तुझे उसे सँवारना है।’’ और फिर इलाहाबाद के पुराने मोहाल की गलियों में पति और ससुर की ज़िम्मेदारी उस किशोरवय कन्या ने उठाई तो फिर उसी में रच-बस गयी- इतनी कि अपने पति के साहित्यिक परिवार को ही अपना परिवार बना लिया।


विवाह के पश्चात पहले पुत्र के जन्म के बाद ही गोपेश स्थानीय विद्यालय में अध्यापक हो गये। पढ़ना-पढ़ाना उनका अर्थोंपार्जन का जरिया बना। उसी समय से वे कवि के रूप में लोकप्रिय होने लगे थे। कवि बच्चन, नीरज, गोपाल सिंह नेपाली, आदि कवियों के साथ वे कवि-सम्मेलनों में बुलाये जाने लगे थे और तभी से निराला, फिराक, बच्चन जैसी बड़ी साहित्यिक विभूतियों के स्नेह के पात्र होने लगे थे। आए दिन बदलते टूटे-फूटे मकानों में इन महान विभूतियों के अलावा उदीयमान साथी कवियों जैसे जगदीश गुप्त, धर्मवीर भारती, लक्ष्मीकान्त वर्मा, उमाकान्त मालवीय, रमानाथ अवस्थी जैसे लोगों का आना जाना लगा रहता। अपनी अभावग्रस्त, सीमित संसाधनों वाली गृहस्थी में भी स्नेहलता सभी की समुचित आवभगत करती और सबको पूरा सम्मान देती। निराला से लेकर नागार्जुन तक उन्होंने उस समय के सभी प्रतिष्ठित साहित्यकारों की आवभगत तबीयत से की।
महिला-विहीन अपने ससुराल में वे निरन्तर अकेले पास पड़ोस के सहारे ही प्रसव झेलती और कई संतानों को जन्म देती रहीं। संघर्ष की उस स्थिति में उनकी कई पुत्रियाँ छोटी वय में ही काल कवलित होती रहीं।
उस समय शहर में प्रगतिशील खेमे के बरअक्स साहित्यकारों की एक समानान्तर संस्था ‘‘परिमल’’ बहुत सक्रिय थी। गोपेश उस संस्था के संस्थापक सदस्यों में थे। साहित्यिक गोष्ठियाँ नियमित रूप से होती थी और हर बार किसी न किसी सदस्य के घर पर होती थी। कभी जगदीश गुप्त तो कभी रघुवंश के घर, कभी विजयदेव नारायण साही तो कभी रामस्वरूप चतुर्वेदी के निवास पर। ऐसी सभी गोष्ठियों में साहित्यकारों की पत्नियाँ ही जलपान की व्यवस्था मिलजुल कर देखती थी। इस व्यवस्था के चलते तत्कालीन सभी साहित्यकारों की पत्नियों के बीच एक स्नेहिल बहनापा बना हुआ था। उसमें स्नेहलता गोपेश भी साधारण गृहणी के स्वरूप से कुछ अधिक एक सामाजिक व्यक्तित्व में ढलती गयीं। पारिवारिक सदस्यों का अभाव जो उन्होंने ससुराल में झेला था उसकी कमी उन्होंने साहित्यिक दुनिया में पूरी कर ली। धर्मवीर भारती, उमाकान्त, गर उनके मुँहलगे देवर थे तो डॉ0 रामकुमार वर्मा, बच्चन, निराला, रामकुमार वर्मा, पंत आदि जेठ या ससुर जैसे। उस समय भी अपने विचारों का अलग तेवर उन्होंने हमेशा बना कर रखा। इस संदर्भ में एक प्रसंग उल्लेखनीय है- पड़ोस में रहने के कारण युवा धर्मवीर भारती का आना-जाना घर पर प्रायः होता था। वे मेरी माँ के बड़े प्रिय मुँहलगे देवर थे, जिन्हें वे बहुत स्नेह करती थीं और उनके घर के नाम बच्चन से ही उन्हें बुलाती थी। पर बंबई जाने के बाद जब उन्होंने पहली पत्नी को छोड़कर दूसरा विवाह किया तो माँ ने जैसे विरोध में उनसे नाता ही तोड़ लिया। उन्हें माँ ने जितना स्नेह दिया बाद के दिनों में उन्होंने उनसे उतनी ही बेरुखी अपना ली। जब कभी पिता गोपेश उनका पक्ष लेते और उनकी वकालत करते तो माँ साफ कह देती- ‘‘आप चाहे जो भी करें कहें मेरी ओर से उनसे कह दीजियेगा कि वे मेरी देहरी पर कभी कदम रखने की कोशिश न करेंगे। मैं अब उन्हें पहले जैसा स्नेह न दे पाऊँगी।’’
1946 में जब आकाशवाणी का इलाहाबाद केन्द्र खुला और वहाँ गोपेश को नौकरी मिल गयी तब घर की स्थिति बेहतर होने लगी। इस बीच पुत्र और कई पुत्रियाँ हो चुकी थीं। पति गोपेश का स्थानान्तरण आकाशवाणी के कलकत्ता केन्द्र और फिर वहाँ से मास्को हो गया। इधर स्वदेश में लगभग आठ वर्षों तक स्नेहलता ने घर और बच्चों की ज़िम्मेदारी अकेले ही उठाई और बखूबी उठाई। हम बच्चों की पढ़ाई के चलते माँ पिताजी के साथ नहीं जा सकती थीं। अब उन्हें हम भाई-बहनों को अकेले ही पालना था। अपनी सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ से यह जिम्मेदारी उन्होंने सफलतापूर्वक निभाई। इस पूरे काल में न तो हमने उन्हें निरीह या अबला पाया, न ही असंतुष्ट या अप्रसन्न।
‘‘बीच-बीच में कई बार दिलफेंक चरित्रों ने उनके अकेले होने का फायदा उठाने का प्रयास भी किया, जिसका सामना उन्होंने हिम्मत से किया। हाँ, तब आसपास के परिवार और उनके बुजुर्ग लोग हमेशा उनकी सुरक्षा में उनके साथ खड़े दिखे। अफसोस कि ये मोहल्लेदारी अब नहीं दिखती।’’
बीच में दो वर्षों के लिये हमें मास्को पिता के संग रहने का अवसर मिला। कम पढ़ी लिखी और अंग्रेज़ी बिलकुल न जानने पर भी उन्होंने हम दो बच्चों के साथ इलाहाबाद से दिल्ली और फिर दिल्ली से मास्को तक की लम्बी हवाई-यात्रा किस आत्म-विश्वास के साथ की, आज सोचती हूँ तो हैरत होती है। एक अनजान देश, अनजान भाषा, अनजान लोग। तिस पर हमने मास्को की धरती पर कदम रखा उस समय पिता गोपेश कार्य के सिलसिले में चीन गये हुए थे। हवाई अड्डे पर हमारा स्वागत वहाँ पर रह रहे भारतीय परिवार के लोगों ने किया और हमें हमारे घर तक पहुँचाया। मुझे याद है उन सभी परिवारों के सदस्यों से माँ ने भारतवर्ष आने के बाद भी सम्बन्ध जीवन पर्यन्त निभाया।
मास्को के अपने निवास काल में कैसे उन्होंने समय बिताया क्योंकि वे शुद्ध शाकाहारी और नेम धरम निभाने वाली महिला थीं। कैसे बिताया उन्होंने वह दो साल बिना किसी शिकवे शिकायत के सारी विषम परिस्थितियों को बर्दाश्त करते हुए!! मुझे स्मृतियों में मिलनसार, मृदुभाषी, प्रसन्नवदना, एक स्त्री की छवि ही दिखाई पड़ती है। वहाँ ख्वाजा अहमद अब्बास, भीष्म साहनी, रामकुमार वर्मा जैसे भारतीय लोग तो घर आते ही थे, रूसी लोगों का भी आना जाना घर पर होता था और वे अन्नपूर्णा की तरह हर एक की आवभगत करती। देश वापस आकर पहले दिल्ली में, फिर इलाहाबाद में बीते अपने जीवन में स्नेहलता गोपेश ने पति के साहित्यिक परिजनों से सम्बन्ध आजीवन निभाया।
वे गोरखपुर की और पति गोपेश बरेली के। दोनों के बीच ‘‘पुरबिया और पच्छाँह’’ के फर्क को लेकर ताना-तिश्ना बराबर चलता रहता। वैसे भी श्रीमती गोपेश एक कर्मठ सांस्कारिक, धर्मपरायण, कर्मकान्डी व्यक्ति थी और गोपेश इसके ठीक उल्टे – दो ध्रुवीय मान्यताओं के होकर भी दोनों के बीच किसी पर कभी भी कुछ आरोपित करने का प्रयास कभी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करते और एक दूसरे को उसके निर्वहन का ‘स्पेस’ हमेशा देते। कभी-कभी विपरीत रुचि अभिरुचि के चलते तनाव भी होता, पर पता नहीं कब कैसे फिर सब कुछ सहज और सामान्य हो जाता।
बाद के दिनों में मैंने अनुभव किया, माँ के मन में एक तरफ ऐसे प्रगतिशील विद्वान व्यक्ति की पत्नी होने का गुमान था, पर वहीं किसी पुरातनपंथी, कर्मकान्डी पंडित को पति के रूप में न पाने की शिकायत भी रहती। कभी कभी कहतीं- ‘‘इससे तो अच्छा होता बनारस के किसी पंडित से मेरी शादी हुई होती जो गाँठ जोड़ कर कम से कम पूजा पाठ में साथ तो बैठता।’’ पर पिता हँस कर उड़ा देते, ‘‘अब क्या करोगी! मान लो कि एक नालायक इन्सान से शादी हो गयी। हो गयी तो हो गयी। निभाओ अब।’’ सोचती हूँ अब तो लगता है- जैसे तब निभाया उन्होंने क्या मैं निभा पाती। 1974 में पिता के निधन के बाद तो जैसे उनका अपना जीवन ही समाप्त कर लिया उन्होंने। 4 जुलाई 1986 में अपने अन्तिम दिन तक जीवन की छाया मात्र बन कर रह गयीं थी वे। जीवन के सारे उद्यम क्षीण हो गये थे उनके लिए।
आज माँ और पिता के निधन के इतने वर्षों बाद सोचती हूँ- क्या संतुलन था दो विपरीत व्यक्तित्वों में। पिता ने दिखाया उड़ने को आकाश का असीम विस्तार तो माँ ने सिखाया हमेशा पाँव खींच कर ज़मीन से जुड़े रहना। इन दो विपरीत दिशाओं में आवागमन के संस्कार ने दिया मुझे जीवन के संघर्षों में आसानी से गुज़र जाने की क्षमता। बहुत सारी अच्छी आदतों के लिए मैं आज भी घड़ी-घड़ी माँ को धन्यवाद देती हूँ। सदाशयता, उदारमना, सामर्थ्य अनुसार लोगों की मदद करना, श्रम का सम्मान करना और सामाजिकता के सहारे जीवन को सुचारू रूप से चला लेना यह सारे गुण उनके व्यक्तित्व में सहज ही गुंथे हुए थे। इन गुणों का सम्मान पिता गोपेश भरपूर करते थे। जब तब अकेले में वो मुझसे कहते ‘‘देखो तुम्हारी माँ में कितने गुण हैं। उन सब को अपना लो तुम्हारे लिए लड़ने को तो मैं हूँ ही। पर गुणों को अपनाने में कोई बुराई नहीं। वह तुम्हारे जीवन में तुम्हारे हथियार बनेंगे।’’ दो विपरीत ध्रुवों के बीच ऐसा सम्मान और गरिमामय सम्बन्ध- मैं समझती हूँ मैं भाग्यशाली थी मुझे ऐसे माँ-बाप मिले।