
मृदुला गर्ग पताः ई 421 (भूतल) ग्रेटर कैलाश 11 (2) नई दिल्ली 110048 ईमेल [email protected] सक्रियता के वर्ष 1971-2019 जन्म : 25 अक्तूबर 1938, कोलकाता, भारत शिक्षा : एम ए (अर्थशास्त्र) दिल्ली स्कूल आफ़ इकोनॉमिक्स, दिल्ली , 1960 अध्यापन : इन्द्रप्रस्थ कालेज व जानकी देवी कालेज, दिल्ली , 1960-1963 माँ का नाम रवि कान्ता जैन, साहित्य प्रेमी उर्दू हिन्दी अंग्रेज़ी में प्रवीण पिता का नाम बीरेन्द्र प्रसाद जैन , वकील, मैनेजर, स्वतंत्रता सेनानी, साहित्य अध्येता 1971 में रचनात्मक लेखन आरम्भ। पहला उपन्यास उसके हिस्से की धूप व कथा संग्रह, कितनी क़ैदें 1975 में प्रकाशित। तबसे स्वतंत्र रूप से रचनारत। उनके रचना संसार में सभी गद्य विधाएं सम्मिलित है। उपन्यास, कहानी, नाटक, निबन्ध, यात्रा साहित्य, स्तम्भ लेखन, व्यंग्य, संस्मरण, पत्रकारिता तथा अनुवाद। उनका कथा साहित्य,कथ्य और शिल्प के अनूठे प्रयोग के लिए जाना जाता है। व्यक्ति व समाज के मूल द्वन्द्व उसमें एकमएक हो जाते हैं और अपनी विडम्बनाओं में गहराई तक परखे जाते हैं। भाषा की लय और गत्यात्मकता उन्हें अति-पठनीय बनाती है। 2003 से 2010 तक इंडिया टुडे (हिन्दी) में पाक्षिक स्तम्भ कटाक्ष लिखा। 2003-2005 तक के लेख, कर लेंगे सब हज़म नाम की पुस्तक में और 2006 से 2008 तक के लेख, खेद नहीं है पुस्तक में प्रकाशित । प्रकाशित कृतियों की सूची (हिन्दी) उपन्यास 1 उसके हिस्से की धूप 1975 2. वंशज 1976 3 चित्तकोबरा 1979 4 अनित्य 1980 5 मैं और मैं 1984 6 कठगुलाब 1996 7 मिलजुल मन 2009 8. वसु का कुटुम 2016 9. द लास्ट ईमेल (अंग्रेज़ी में) 2017 कहानी संग्रह 1. कितनी क़ैदें 1975 2. टुकड़ा-टुकड़ा आदमी 1976 3 डैफ़ोडिल जल रहे हैं 1978 4 ग्लेशियर से 1980 5 उर्फ़ सैम 1986 6 शहर के नाम 1990 7 चर्चित कहानियाँ 1993 8 समागम 1996 9 मेरे देश की मिट्टी अहा 2001 10 जूते का जोड़ गोभी का तोड़ 2006 11 प्रतिनिधि कहानियाँ 2017 12. संकलित कहानियाँ राष्ट्रिय पुस्तक न्यास 2011 13. सम्पूर्ण कहानियाँ राजकमल प्रकाशन 2022 नाटक 1 एक और अजनबी 1978 2 जादू का कालीन 1993 3 तीन क़ैदें 1996 4 साम दाम दण्ड भेद (बाल नाटक) 2011 5 क़ैद दर क़ैद चार नाटक 2015 1 रंग-ढंग 1995 2 चुकते नहीं सवाल 1999 3 कुछ अटके कुछ भटके (यात्रा संस्मरण) 2006 4 कर लेंगे सब हज़म (कटाक्ष) 2007 5 खेद नहीं है (कटाक्ष) 2009 6 कृति और कृतिकार (संस्मरण) 2013 7 कृति में स्त्री पात्र (आलोचना) 2016 अनुवाद मृदुला गर्ग के उपन्यास व कहानियाँ अंग्रेज़ी, जर्मन, चैक, जापानी आदि विदेशी व अन्य भारतीयों भाषाओं में अनुदित हैं। इनमें प्रमुख हैः 1 चित्तकोबरा (उपन्यास) इसी शीर्षक से अंग्रेज़ी (1999) में; द जिफ़्लेक्टे कोबरा नाम से जर्मन में (1988),कोबरा मॉएगो रज़ूमे नाम से रूसी में (2016), ल खोब्रा द लेस्प्रि नाम से फ़्रान्सीसी में (2022) अनुदित-प्रकाशित। 2 डैफ़ोडिल्स आन फ़ायर (कहानियाँ) अंग्रेज़ी में अनुदित-प्रकाशित 1999 3. कठगुलाब उपन्यास, कन्ट्री आफ़ गुडबाइज़ नाम से अंग्रेज़ी (2003) मराठी (2007) मलयाळम (2009) और वुडरोज़ नाम से जापानी में 2011 में अनुदित-प्रकाशित। 7. अनित्य उपन्यास, अनित्य हाफ़वे टु नोव्हेयर नाम से 2010 में अग्रेज़ी में और मराठी में अनित्य नाम से 2013 में अनुदित-प्रकाशित 8. मैं और मैं उपन्यास मराठी में मी आणि मी नाम से 2015 में अनुदित-प्रकाशित पुरस्कार-सम्मान 1 मध्य प्रदेश साहित्य परिषद महाराज वीरसिंह अखिल भारतीय पुरस्कार उसके हिस्से की धूप (उपन्यास) 1975 2 आकाशवाणी प्रथम पुरस्कार, एक और अजनबी (नाटक) 1978 3. साहित्यकार सम्मान, हिन्दी अकादमी दिल्ली 1988 4 मध्य प्रदेश साहित्य परिषद, सेठ गोविन्द दास अखिल भारतीय पुरस्कार, जादू का कालीन (नाटक) 1993 5 साहित्य भूषण, उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 1999 6 हैलमन-हैमट ग्रान्ट, ह्यूमन राइट्स वॉच, न्यू यार्क 2001 7 विश्व हिन्दी सम्मेलन सुरीनाम में सम्मानित 2003 8 व्यास सम्मान कठगुलाब उपन्यास 2004 9. साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलजुल मन उपन्यास 2013 10. राम मनोहर लोहिया सम्मान उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान 2015 मृदुला गर्ग समय समय पर जर्मनी, यूगोस्लाविया, जापान, चीन, रूस, इटली, डेन्मार्क, अमरीका आदि देशों के विश्वविद्यालयों व सांस्कृतिक संस्थानों में आमंत्रित हुई हैं। उन्होंने वहाँ अपना रचना पाठ किया है व समकालीन साहित्यिक व सांस्कृतिक मुद्दों पर व्याख्यान दिये है । सभी व्याख्यान देशी-विदेशी पत्रिकाओं में अंग्रेज़ी, इतालवी, रूस और जापानी भाषाओं में प्रकाशित हैं।


………………………….
समागम
मैं उस रोमांचक क्षण का इन्तज़ार कर रही थी, जो कुछ देर में मुझे अभिभूत करने वाला था। अपने-अपने अनुभव से सभी ने कहा था, अभूतपूर्व होती है, वह अनुभूति। हमेशा के लिए स्मृति में अंकित हो जाती है। अनुभव से कहा या अनुमान से, कौन जानता है? ख़ुद कहने वाला भी नहीं। शाम साढ़े सात बजे गंगा की आरती होनी थी। अभी कुल छह बजे थे। पर हर की पैड़ी पर तिल रखने की जगह नहीं थी। सीढ़ी दर सीढ़ी एक अपार भीड़ जंगली घास की तरह एक के ऊपर एक लदी हुई थी। कहीं दरार या छीड़ नहीं थी। फिर भी लोग आते जा रहे थे और भीड़ के बीच समाते जा रहे थे। मैं भी समायी थी, इसी तरह, कुछ देर पहले। सच तो यह है कि अगर नवागंतुकों का एक रेला मुझे ठेल कर अपने साथ आगे बहा न लाया होता तो मैं सरहद से ही लौट जाती। मुझे भीड़ से बहुत घबराहट होती है। नहीं, डर नहीं लगता, कम से कम वह डर नहीं सताता, जिससे प्रभावित होकर चारों तरफ़ से लाउड-स्पीकरों पर हिदायतें दी जा रही थीं। कृपया यात्री ध्यान दें। अपना सामान साथ रखें। जेबकतरों और उठाईगीरों से सावधान रहें। औरतें अपने ज़ेवर की देखभाल ख़ुद करें। बेसुरे भजन गायन के बीच में किए जा रहे सावधान के ऐलान जिस डर को शब्द दे रहे थे, वह मेरे भीतर कहीं नहीं था। ज़ेवर मैं पहनती नहीं। रुपया-पैसा, थोड़ा-बहुत जो है, गंगा तट लेकर आई नहीं। पास में धन्ना सेठ बैठा हो या उठाईगीर, मेरे लिए दोनों एक तरह की हौल को जन्म देने वाले थे। शोर बढ़ रहा था। संध्या के जोबन पर आने के साथ, भीड़ ने गंगा मैया की जै भी बोलनी शुरू कर दी थी। उसके अलावा, हाथों में बही थामे वर्दीधारी स्वयंसेवक, उचक-उचक कर, ऊँची आवाज़ में यात्रियों से आरती के लिए अनुदान माँग रहे थे, हाँ जी आप, गंगा मैया की आरती के लिए पैसा बोलिए। गंगा भैया की जै क्र-क्री, क्र-क्री गंगा मैया—क्री-क्री तोहे पियरी—क्र-क्र- चढ़ाई—क्री-बो-क्र-क्री। सामान सँभाल कर रखें। गंगा मैया की आरती के लिए कितना रुपया, बोलिए। जेबकतरों और उठाईगीरों से सावधान। क्री-क्री-जय गंगा मैया की। क्री-क्री-क्री-क्री। पता नहीं माइक की ख़राबी थी या रिकॉर्ड की, पर भजन के सुर क्री-क्री से चिर कर हवा में खो जाते थे। हाँ, ऊँचे स्वर में दी जा रही सावधान रहने की हिदायतें, फटे बाँस सी कर्णकटु होने पर भी, अपने शब्द यात्रियों तक सुरक्षित पहुँचा देती थीं। जब पहलेपहल यात्रियों के झुंड ने धकिया कर मुझे यहाँ ला बिठलाया था तो मैं देर तक नज़रें नीची किए रही थी। कम से कम जगह में समाने के लिए मैं घुटनों को हाथों से घेरे बैठी थी। मेरे चारों तरफ़ ठठ की ठठ भीड़ थी, इसका मुझे अहसास था। फिर भी उसे अनदेखा किए रहने की कोशिश में मैंने यों दम साध रखा था कि ख़ुशनुमा ठंडी हवा के बावजूद मुझे पसीना आ गया था। पेट में हौल के गोले उठ रहे थे, जिन्हें वापस दबाये रखने के लिए मैं खुलकर साँस लेने से कतरा रही थी। पर बार-बार होते दुनियादार ऐलान उन हौल के गोलों में सूई चुभोने लगे थे। इतनी दीन-हीन, जेबकतरों और उठाईगीरों से डरी हुई भीड़! इससे भला कैसी घबराहट? यह मेरा वजूद क्या ख़तम करेगी? मैंने सिर उठाकर देखा, दूर तक सिर ही सिर, धड़ ही धड़, शान्त स्थिर। कोई हलचल नहीं, धकापेल नहीं। नए आगंतुकों का रेला आता, जनसर में हिलोर उठती पर शीघ्र ही समागम हो जाता। फिर वही शान्त-स्थिर समूह। जैसे घाट की सीढ़ियों पर मोम के पुतले स्थापित कर दिये गए हों, ठूसमठूस। गहन सन्नाटे के बीच रह-रहकर उठता गंगा मैया की जै का उद्घोष भी उसे तोड़ नहीं पाता था। ध्वनि ऊपर उठती और हवा उसे सोख लेती। जैसे पसीना। हाँ, मेरे बदन का पसीना भी सूख चला था। इतने पास-पास सटे शरीरों के बावजूद किसी देह-गन्ध का अहसास नहीं था। मैंने अपने चेहरे से सटे चेहरों पर निगाह घुमाई। एकदम भावहीन। कोई आशंका, आशा, आकांक्षा नहीं। लगता नहीं था उन्हें किसी क्षण की प्रतीक्षा थी। अधैर्य न सही, सधा हुआ धैर्य तो दिखना चाहिए था। नहीं था। जो था, इतना भावहीन था कि वह अनंत काल तक, बिना प्रश्न, बिना सोच-विचार, बिना अशान्ति, प्रतीक्षा करते रहने की आदत से ही पैदा हो सकता था। तभी न उनका उद्घोष उनसे विलग था। लगता था जयकार उनके समवेत गलों से सायास नहीं निकलता, यों ही अकेल-दुकेल हवा में तिर आता है। वे सब वहाँ थे, अभिलाषा, चेष्टा, उत्कंठा से परे, जहाँ बस थे। इसे ही स्थितप्रज्ञ कहते हैं? तब क्या सिर्फ मुझे ही किसी रोमांचक क्षण का इन्तज़ार था? गंगा मैया की जै। उठाईगीरों और जेबकतरों से सावधान। अपना रुपया-पैसा सँभाल कर रखें। गंगा मैया की आरती के लिए कितना? औरतें अपना ज़ेवर बचाएँ। कर्कश घोषणाओं को हवा नहीं सोख पाई। वे हवा पर काबू पा कर, धम-धम सिर पर बरसने लगी। स्थितप्रज्ञता की धज्जियाँ उड़ गईं। गंगा मैया की आरती के लिए रुपया दीजिए। अपना रुपया-पैसा सँभालिए। उठाईगीरों से बचाइए। दीजिए-दीजिए। बचाइए-बचाइए। दीजिए-बचाइए का शोर सुन मैं तिक्त हँसी हँस दी। एक बार फिर मैंने अपने पास अँटे चेहरों पर नज़र डाली। सब शान्त, निरीह, निर्विकार। तो किसी ने कुछ नहीं सुना? मेरे पेट में दोबारा हौल के गोले उठने लगे। उस भीड़ ने भी कुछ नहीं सुना था। भीड़ सुनती नहीं। भीड़ सुन नहीं सकती। भीड़ में भटका आदमी खो जाता है, हमेशा के लिए। उसके पैरों के नीचे कुचलता चला जाता है। हम पुकारते रह जाते हैं, विनती करते रह जाते हैं, भीड़ रौंदती हुई आगे बढ़ जाती है। कोई कुछ नहीं सुनता। वह पहली-पहली पन्द्रह अगस्त थी। उत्सव की संध्या। इंडिया गेट पर ज़बरदस्त हुजूम और उसके पैरों तले रौंदा जा रहा एक बूढ़ा। मैं चीखी थी, चिल्लाई थी, नौ बरस की अपनी उम्र की तमाम ताक़त लगाकर बार-बार चीखी थी। पागल की तरह भीड़ को धक्के देकर, लात-घँूसे मारकर आगाह करने की, रोकने की, नाकाम कोशिश की थी मैंने। और उस कोशिश में अपने परिवार से बिछुड़ गई थी। भयानक थी वह भीड़, वह शाम। दोनों तरफ़ से बाधित होने पर भी मैं किसी तरह लड़खड़ा कर नीचे की पैड़ी पर खड़ी हो गई। ''बैठ जाइए,” बराबर वाले ने शान्त भाव से कहा। ''अब क्या होगा?” कातर स्वर में मैं फुसफुसायी। ''आरती होगी।” ''मुझे जाना है,” मैंने चीख़ना चाहा पर गला रुँध गया। ''अभी नहीं। आरती के बाद। बैठ जाइए,” उसी शान्त स्वर में उसने कहा। मैं बैठ गई। आँखें सामने गंगा के प्रवाह पर जमा दीं। असंख्य दीप उस पर जल-बुझ रहे थे। लोग पत्ते से बनी नाव में छोटा सा घी का दीप जला कर जल में प्रवाहित कर रहे थे। अब, जब दिन का उजाला मलिन पड़ने लगा था, दीपों का क्षीण प्रकाश टूटते तारों की तरह चकमक करके बुझ रहा था। हवा तेज़ थी। क्षण-दो क्षण में ही दीप बुझ जाते थे, पर इतने में दूसरे जल उठते थे। पानी पर जगमग तारे टूटते चले जा रहे थे। मेरे पास भी तो है पत्ते की नाव फूलों की पंखुड़ियों से भरी। बीच में स्थित नन्हा दीप और कपूर। यहाँ आकर बैठने से पहले उसे गंगा में प्रवाहित करना चाहिए था पर उससे पहले ही यात्री मंडली ने मुझे प्रवाहित कर यहाँ पहुँचा दिया था। अप्रज्वलित उदास दीप मेरी गोद में दुबका पड़ा था। भीड़ के सामने किसका वश चला है। ...फिर भी मेरे परिवार ने मुझे ढूँढ़ लिया था पन्द्रह अगस्त बीत जाने पर, अगले दिन या शायद उसके अगले दिन। बीच में अँधेरा ज़रूर घिरा था। एक अँधेरी रात या दो। अब सोचती हूँ, अगर बीच में अन्धकार न आया होता तो मैं उस बूढ़े को कभी न भुला पाती। यह भी कि अगर बूढ़ा आँखों के सामने न रहा होता तो वह तमस मुझे लील गया होता पर एक आतंक दूसरे को काटता, क्षीण करता रहा था। बूढ़ा और घुप अँधेरा, दोनों, फंतासी के हिस्से बन गए थे। मेरे कहे पर किसी ने विश्वास नहीं किया था। कल्पना थी तुम्हारी, सबने कहा था। उमस, उत्तेजना और भीड़ की गँधाती रेलपेल से पैदा हुई उद्भ्रान्ति में देखा दु:स्वप्न था। कहाँ, कहीं भी तो कोई बूढ़ा कुचला नहीं गया। कुचला जाता तो क्या उसकी लाश नहीं मिलती? शिनाख्त नहीं होती, चलो, शिनाख्त न भी होती तो लावारिस लाश, सबूत बनी, पड़ी तो मिलती। रुँदी-पिसी लाश, वह भी इंडिया गेट पर, अख़बार वाले ख़बर छापे बगैर छोड़ देते क्या? नहीं, सब बच्ची का भ्रम है, आँख लग गई होगी, सपना देखा होगा, डर गई होगी। आँख में अंजनहारी भी तो निकल रही है, दिख भी कहाँ रहा होगा ठीक से। गरमी, उमस, धकापेल, ऊपर से आँख में दर्द और उसमें से लगातार गिरता पानी। आँख में तक़लीफ़ होते हुए आपको इसे घर से बाहर ले ही नहीं जाना चाहिए था। कहानी गढ़ने का शौक़ होता है बच्चों को। कहानी को यथार्थ मान बैठते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं और हमें भी करवाना चाहते हैं। अब इसी को लें, बीच में गुज़रे वक्त के बारे में यह जो बतला रही है, वही कौन सा सच है। दो-चार सवाल करो तो बौखला जाती है, जवाब गड़बड़ाने लगते हैं। पुलिस स्टेशन पर तमाम बत्तियाँ लगी हैं, कहाँ था वह काला घुप अँधेरा, जिसकी यह बात करती है? दीखता नहीं था। साँस घुटता था, अँधेरा था सब तरफ़ अँधेरा, काला-डरावना, काला अँधेरा, काला अँधेरा। बुखार का प्रमाद था। बुखार आ गया था न वहाँ इसे, उसी का प्रलाप अब तक सिर पर हावी है। आँख में दर्द, बुखार, ऊपर से भीड़ के धक्के, उमस और घुटन। भीड़ को भी क्या दोष दें। आज़ादी का पहला दिन, उन्माद तो होगा ही। बाँध तोड़ती पहाड़ी नदी सी हरहरा रही थी भीड़, बच्चे डरेंगे नहीं तो क्या? इससे कहिए भूल जाए सब कुछ। भूल जाओ सब कुछ। बार-बार मुझसे कहा गया। कहीं कोई बूढ़ा कुचला नहीं गया। कुछ नहीं हुआ, बस तुम भीड़ में खो गई थीं और ढूँढ़ने पर वापस मिल गईं। न बूढ़ा था, न अँधेरा, सब बुख़ार में देखा गया दु:स्वप्न था, कल्पना और सपने से बुनी कहानी, भूल जाओ उसे। भूल जाओ सब कुछ, बार-बार वही शब्द दोहराये गए और मुझसे उन्हें भूलने को कहा गया। शब्द मुझे रट गए, फिर भी बहुत कुछ मैं भूल गई पर भीड़ को नहीं भूली। घर के लोग रामलीला देखने जाते तो मैं ग़ुसलखाने में छिप जाती। भीड़ मेरे लिए हौवा बन गई थी। अब सोचती हूँ अगर वाक़ई आज़ादी की उस पहली शाम, कोई बूढ़ा भीड़ के पैरों तले कुचल कर मरता तो क्या उसकी ख़बर छपती? पुलिस वाले उसकी लावारिस लाश की शिनाख्त करवाते? उस उत्सवी माहौल को एक गरीब बूढ़े की मौत के लिए कौन ध्वस्त करता? कोई नहीं। उस दिन भीड़ केवल सड़कों पर नहीं थी, हमारे भीतर, हर किसी के हृदय के अन्दर भी थी। हम भीड़ के हिस्से थे, हमारा अपना अलग वजूद मिट चुका था। हम भीड़ थे, बस भीड़ थे और भीड़ होने में ख़ुश थे क्योंकि उसी तरह हम आज़ाद थे, मुक्त थे, गरिमामय थे। फिर जब तन्द्रा टूटने पर हमारा वजूद जगा तो क्या हुआ? हम इतने हतबल क्यों हो गए, इन बुझते दीपों की तरह? ''माँ! माँ!” कोई आर्त कंठ से मेरे कान में फुसफुसाया। मैं हिल गई। अब इतनी जगह भी बाक़ी नहीं थी कि बदन हरकत कर पाता। पर मेरा पूरा अस्तित्व थरथरा गया। जितनी नज़र घूम सकती थी, मैंने घुमाकर देखा। मेरे ठीक पीछे बैठा बूढ़ा, हाथ जोड़े, क्षीण स्वर में उचार रहा था, ''माँ, गंगा माँ!” ''क्या हुआ?” मेरा स्वर काँप गया। बूढ़े को कन्धों से थामे अधेड़ ने कहा, ''अभी आरती होगी।” ''ये ठीक तो हैं?” ''हाँ माँ, गंगा माँ,” बूढ़े के सुर से सुर मिला कर उसने भी उचारा। इतना बूढ़ा आदमी। जैसे पुतला नहीं, उसकी छाया हो। भीड़ के ऊपर से तैर कर आ गया होगा, तभी कुचला नहीं गया। उसके साथ का अधेड़ ख़ुद कम कृशकाय नहीं, सत्तर से कम क्या होगा? और बूढ़ा? आयु के हिसाब के ऊपर स्वर इतना महीन कि अगर उस समय बाक़ी शोर थमा हुआ न होता तो कानों को छू कर भी अनसुना निकल जाता। अधेड़ ने उसे कन्धों से ऐसे थाम रखा था जैसे हाथ हटाते ही वह धराशायी हो जाएगा। ''माँ, गंगा माँ,” उसके स्वर का बारीक कम्पन कानों की लवों पर महसूस हो रहा था वरना पता चलना मुश्किल था कि वह जीवित है भी या नहीं। ''माँ, गंगा माँ,” अधेड़ का स्वर, कम्पन को सम्बल दिये हुए था। दोनों की अश्रुधारा बह रही थी। मेरा मन हुआ, मैं भी माँ, गंगा माँ, का उच्चारण करूँ, आँसुओं को बेरोक बह जाने दूँ। नहीं कर पाई। डर था कि एक बार अंकुश हटा दूँगी तो दोबारा अनुशासित नहीं हो पाऊँगी। फिर प्रकाश भी बहुत ज़्यादा था। संध्या का अवसान क़रीब था पर अब तक धँुधलका हुआ नहीं था। सूर्यास्त के साथ आरती होनी थी। तब तक उजाले से आँखें चुराना असम्भव था। और फिर इतने लोगों का जमावड़ा। पर वे क्या मेरी तरफ़ देखेंगे। सामने ब्रह्मकुंड में लोग डुबकी लगा रहे थे। मर्द-औरतें, दोनों निर्वसन, निर्द्वन्द्व, निस्पृह। कोई किसी की तरफ़ देख नहीं रहा था। उन पत्तों की नावों की तरफ़ भी नहीं, जो उनके पास से बही चली जा रही थीं। बीच डगर, उनकी नज़रों के सामने, कितने जलते दीप हवा के प्रकोप से बुझ रहे थे पर किसी को परवाह नहीं थी। काश, कुछ देर के लिए सारे दीप जले रह सकते। तब मैं भी माँ, गंगा माँ जप सकती, शायद। मैंने कान लगाकर सुना, बूढ़े का स्वर क्षीण से क्षीणतर होता जा रहा था पर उसका कंपित जाप जारी था। धीरे-धीरे मेरी समझ में आया कि लाउड-स्पीकर काफी देर से चुप्पी साधे हुए थे। हवा का वेग बढ़ चला था। हलकी खुनकी बदन में सिहरन पैदा कर रही थी। बूढ़े के शब्द हवा में तिरोहित हो रहे थे। बस बीच-बीच में जब हवा का कोई झोंका सेंध लगाकर हमारे पास-पास अटे शरीरों के बीच घुस आता, तो उसकी काँपती आवाज़ भी कानों को सहला कर गुज़र जाती। कोलाहल और आवागमन रहित वातावरण अब बिलकुल शान्त था पर निस्तब्ध नहीं। पहली बार मुझे समवेत प्रतीक्षा की धड़कन की अनुभूति हुई। हवा के झोंके और बूढ़े के जाप की तरह, वह भी श्वास-प्रश्वास बन, माहौल को जीवन के आह्लाद से भर रही थी। शंख की ध्वनि ने शान्ति को झंकृत किया। आरती शुरू हो गई। ब्रह्मकुंड के चारों ओर ऊँची-ऊँची लपटें उठीं। घंटे-घड़ियाल बजे और आरती के सुर घंटियों की टनटनाहट के साथ तरंगित होने लगे। ये कैसी लपटें थीं, ऊपर उठतीं, चक्राकार घूमतीं, पानी में प्रतिबिंबित होतीं, ऊँची-ऊँची लपटें। जैसे प्रकाश का भँवरजाल हो, अग्नि का उल्लसित नर्तन। जय गंगा माता, श्री जय गंगा माता। जो नर तुमको ध्याता, मैया जी को ध्याता। मनवांछित फल पाता, जय गंगा माता। सस्वर गायन के मधुर सुर प्रकाश के नर्तन को थाप दे रहे थे। मैं घुटनों के बल उठ आई। जल से भीगी, घाट की सीढ़ियों पर थोड़े-थोड़े फासले पर पुजारी खड़े थे। प्रत्येक का कपड़े से ढका हाथ एक वृहदाकार दीपगिरी थामे था। नीचे एक दीर्घकाय दीप, उसके ऊपर मंजि़ल दर मंजि़ल बने असंख्य छोटे-छोटे दीप। सब प्रज्वलित। सबकी ज्वाला मिलकर लपट बन कौंध रही थी। उसी लपट को पुजारी नदी की आरती में चक्राकार घुमा रहे थे। अग्निज्वाला का वह चक्रवात, जल में प्रतिबिंबित होकर आलोक के भँवरजाल सा प्रतीत हो रहा था। ब्रह्मकुंड का पानी आग का सोता बन गया था। उसमें से स्फुलिंग की तरह ऊपर उठ रहे थे, घंटियों और गायकों के स्वर। यही वह रोमांचक क्षण था जिसका सबको इन्तज़ार था? फिर मुझे अब भी इन्तज़ार क्यों है? पूरे दो बरस के इन्तज़ार के बाद आई थी मैं हरिद्वार। तब नहीं आई थी, बेटी ने मना कर दिया था। ''मेरी देह के अवशेष अपने बगीचे के पेड़ों में डाल देना। हड्डियों की खाद फल के पेड़ों के लिए अच्छी होती है,” उसने अपनी वसीयत में लिखा था। क्यों लिखी वसीयत उसने इतनी कम उम्र में? मैं नहीं जानती। मैं आज तक नहीं जान पाई कि उसकी मृत्यु दुर्घटना थी या हत्या। मुझे तो उसकी मृत देह मिली थी और एक सरकारी बयान। मुझे सिर्फ इतना बतलाया गया था कि उस इतवार की सुबह, वह अपने अकेले घर के ग़ुसलखाने में नहाने गई थी, और वहीं गिर पड़ी थी। नल के ऊपर बनी पत्थर की पाटी से टकराकर। यह देखिए सिर पर ज़ख्म। किसी भोथरी, भारी चीज़ से टकराने से बना घाव है। नल के ऊपर लगी पाटी बहुत नीची थी। जल्दी में उठो तो टकराने की पूरी सम्भावना रहती थी। और जल्दी में तो, आप जानती हैं अमला हमेशा रहती ही थी। पर पिछले तीन सालों से वह उसी ग़ुसलखाने का इस्तेमाल करती आई थी, अब तक सिर उससे बचाए रखना सीख चुकी होगी। होनी! दुर्घटना तिथि बतला कर नहीं होती। चौबीस घंटे बीत गए थे। किसी ने खोज-ख़बर नहीं ली थी। मंगलवार को अदालत में पेशी थी। सोमवार को मुवक्किल और साथी वकील सलाह करने आए तो दरवाज़ा पीट-पीटकर परेशान हो गए थे। खिड़की की छड़ निकाल कर भीतर दािखल हुए तो लाश बरामद हुई। हाँ, ढीली तो थीं ही खिड़की की छड़ें। अब आप जानिए छोटे क़स्बे का घर, कौन वहाँ ग्रिल लगी होती है। ग़ुसलखाने में कोई दरवाज़ा था नहीं, नहाते हुए कमरे की साँकल चढ़ा लेती थी, सो वही चढ़ी हुई थी। ठीक है, छड़ निकाल कर कोई भी अन्दर आ सकता था और उसके सिर पर वार कर सकता था। पर क्यों करता? कोई प्रयोजन तो साबित हुआ नहीं था। न उसके साथ बलात्कार हुआ, न किसी चीज़ की चोरी हुई, यहाँ तक कि तमाम कागज़ात भी ज्यों के त्यों ताले में बन्द सुरक्षित पाए गए थे। हाँ, हम जानते हैं, उन दिनों वह घोरेट की पत्थर खदानों की मज़दूर यूनियन की तरफ़ से केस लड़ रही थी। उनके नेता का अपहरण हो गया था। निचली अदालत में सिद्ध हो चुका था कि अपहरण डाकुओं ने किया था पर विपक्षी दल कुछ राजनीतिज्ञों का नाम लेने पर उतारू था। उन्होंने अमला को अपना वकील बनाया था। बहुत भावुक, संवेदनशील लड़की थी। अपनी समझ में शोषित जनता का साथ दे रही थी। पर तब तक उसकी समझ में आ चुका था कि केस में जान नहीं थी। ठोस तथ्यों के न रहने पर वह केस हारती ही हारती। अब मुवक्किल तो कहेंगे ही, अकाट्य तथ्य थे उसके पास। पर जो था ताले में बन्द, सुरक्षित अदालत के सामने पेश था। बहुत महत्त्वाकांक्षी, खरी, धुन की पक्की लड़की थी अमला। गलत चुनाव और हार, दोनों बर्दाश्त के बाहर थे उसके लिए। उसके साथी वकील ने भी यही बयान दिया था अदालत में। ''तब क्या उसने ख़ुद पाटी से सिर दे मारा?” ''न, न, हम यह नहीं कहते, बस बेख़याली में। मालिकों को, सबको बहुत दुख है उसकी मौत पर। इतनी मेधावी, निडर, दबंग, नि:शंक लड़की और ऐसा करुण अन्त!” ''फिर उसने वसीयत क्यों लिखी? इतनी कम उम्र में?...” ''वही तो। साफ़ ज़ाहिर है कि वह हताशा की मन:स्थिति में जी रही थी। आत्महत्या का ख़याल बार-बार मन में आता रहता था। मन क्षुब्ध-विक्षुब्ध हो तो दुर्घटना और आत्महत्या में फ़र्क ही कितना रह जाता है।” ''पर अमला तो कभी हताश, हतबल नहीं होती थी।” ''आप माँ हैं। आपको तो ऐसा लगेगा ही। जननी, प्राणदात्री, करुणामयी, जवान बेटी के दुख में कातर माँ, मानेगी लड़की को हतबल, हताश...या सनकी?” महिम ने विश्वास कर दिया था। सनकी नहीं तो क्या थी अमला, जो इतना पढ़-लिख कर, उज्ज्वल भविष्य की स्वामिनी होकर, लखनऊ, कानपुर में वकालत न करके, राजस्थान के धूल-धूसरित क़स्बे घोरेट में पड़ी हुई थी? मैं विश्वास नहीं कर पाई थी, इसलिए मारी-मारी फिर रही हूँ। महिम कानपुर में हैं, अपनी नौकरी पर, भीड़ से घिरे, भीड़ में समाए। शायद महिम सही थे। अपनी ओर से मैं जानती ही कितना थी। सिर्फ यह कि वह अकेली, घर से दूर घोरेट में रहकर काम करती थी। समाज के अभिशप्त, लाचार अंग की मुफ़्त वकालत करती थी, बड़े-बड़े सेठों और सरकारी प्रतिष्ठानों से लोहा लेती थी, कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू और नेकदिल थी। मेरे लिए तो वह एक जि़न्दादिल, भरोसेमन्द, हँसमुख, डूब कर प्यार करने वाली लड़की भर थी। जि़द्दी पर अड़ियल नहीं, ख़रीदने खाने की शौक़ीन, पर देने में कंजूस नहीं। हर विपदा से खूब लड़-झगड़ लेने पर, अन्तत: हँसकर बात बना ले जाने में माहिर। अगर मैं कहूँ कि वह औरों से अलग, अनूठी और अनुपम थी तो क्या? हर माँ को अपनी बेटी अनूठी लगती है। पर मेरी बेटी शायद पगली भी थी। महिम कहते हैं, सनकी। शायद ठीक कहते हैं। भीड़ में न खोने का उसका संकल्प पागलपन ही तो था। महिम उसकी दुखद परिणति के लिए मुझे दोषी ठहराते हैं। क्यों जाने दिया मैंने उसे उस बीहड़ असुरक्षित प्रदेश में? क्यों स्वीकार का सम्बल दिया, हर जोिखम भरे अभियान में? ''अजीब माँ हो तुम। बेटी की कोई फिक्र नहीं है। सारी दुनिया की माँएँ चाहती हैं, उनकी बेटियों का विवाह हो, घर-बार हो, सन्तान हो। वे सुखी, सुहागन, गृहस्थिन बनकर जिएँ। एक तुम हो, बेटी के माध्यम से अपनी महत्त्वाकांक्षाएँ पूरी करना चाहती हो। आज़ादी, चुनाव का अधिकार, मुक्त चिन्तन, दुनिया को बदल डालने के सपने, विरोध, विद्रोह, समाजसेवा, बकवास। अपने अहं को तुष्ट करने के खोखले साधन हैं सब। सारा कुसूर तुम्हारी मान्यताओं का है। ख़ुद लीक से हटकर जीने के सपने देखे। पूरे नहीं हुए तो बेटी पर थोप दिये। अब भुगतो, रोओ, चीखो, तिल-तिल कर मरो बेटी की याद में।” शायद महिम ठीक कहते हैं। शायद सारा कुसूर मेरा ही है। मेरी महत्वाकांक्षाएँ थीं, मैं इनकार नहीं करती, पर मैंने उन्हें बेटी पर नहीं थोपा। बस, उसके मार्ग में अवरोध पैदा नहीं किया। बहला-फुसला कर छोटी उम्र में उसका विवाह नहीं किया। मैंने उसे रोका नहीं, ठीक है, पर किसी रास्ते पर झोंका भी नहीं। पर मैं मनोविशेषज्ञ नहीं हूँ, मनोविश्लेषण करवाना भी नहीं चाहती। हो सकता है, मेरी असन्तुष्ट महत्त्वाकांक्षाएँ ही मेरी बेटी के मन में घर करती गई हों। मुझे प्रभावित रोमांचित करने के लिए ही वह उस कर्म पथ पर अग्रसर हुई हो। मेरे ही कारण वह...फिर भी मैं रोयी-चीखी नहीं थी। अपने को लांछित-प्रताड़ित नहीं किया था। लीक से हटकर चलने को दोष नहीं दिया था। महिम के सामने मैंने रोदन को भीतर घोट कर, उसकी मृत्यु को स्वीकार कर लिया था। धीमे स्वर में एक बार कहा था, ''ज़रूरी नहीं है कि हर बहादुर लड़की का यही अंज़ाम हो। डर-डर कर जीने से तो अच्छा है...।” ''कि मर जाओ!” महिम फट पड़े थे, ''लो मर गई लाडली मेरी। जाओ ख़ुशी मनाओ। घी के दीये जलाओ।” अब मेरे चारों तरफ़ घी के दीये जल रहे थे और मेरी बेटी... मेरा दीप बुझा पड़ा था मेरी गोद में। भीड़ मुझे ठेल कर आगे न बढ़ा देती तब भी शायद मैं उसे प्रज्वलित नहीं कर पाती। महिम का कहा याद आ जाता, तीली हाथ में लेते ही। मैं सिर झुका कर उसे सहलाने लगी। प्रकाश के नर्तन में बहुत भयावह अँधेरा था। मैं देखना नहीं चाहती थी। शायद मेरी आँखों से आँसू भी निकल रहे थे, मेरी गोद धँुधला गई थी। ''इतना घी क्यों बरबाद करते हैं ये लोग? कितने बच्चे खाना खा सकते हैं, इतने में,” मैंने सुना अमला कह रही थी। अमला। अमला कहाँ है इस हुजूम में? पर...हुजूम भी कहाँ है? एकदम सूना है घाट, हर पैड़ी रीती। मगर अमला कहीं है ज़रूर, तभी न मैं उसकी आवाज़ साफ़ सुन रही हूँ जैसे मेरी अपनी गोद से निकल कर आ रही हो। ''तुझे क्या जवाब दूँ, बेटी, मैं ख़ुद प्रश्नचिह्न बनी हुई हूँ। समाधान और शान्ति की खोज में भटक रही हूँ।” ''तुम बहुत भोली हो माँ, यहाँ भला क्या मिलेगा? भीड़ में कुछ नहीं मिलता। जो मिलता है, अकेले। अकेले जूझना पड़ता है, निपट अकेले।” मैं जानती हूँ, अमला! मैं यहाँ बिलकुल अकेली हूँ। जब आई थी, मेरे चारों तरफ़ भीड़ थी। अब नहीं है। मैं देख रही हूँ यहाँ हर आदमी अकेला है। भीड़ का मतलब क्या है, किसे कहते हैं भीड़ हम? बहुत सारे अकेले व्यक्तियों के एक साथ एक जगह, जमा होने को ही न। भीड़ से मेरा डर मिट गया। पर तू अपनी कह बेटी। तुझे अपने किसी सवाल का जवाब मिला था, मरने से पहले? उपलब्धि का सन्तोष, प्राप्य का हर्ष, अपनी तरह जी पाने का आनन्द, कुछ पाया था? या यूँ ही रीती की रीती, सब इच्छाएँ मन में सँजोए चली गई? यह क्या हो गया, बेटी! क्यों हुआ? अपना रोदन कानों में पड़ा तो चौंककर मैंने आसपास देखा। आरती समाप्त हो चुकी थी। लोग उठकर जा रहे थे। सीढ़ियों पर खाली जगह दिखने लगी थी। पर मेरी कमर पर दूसरे शरीर का भार वैसा ही बना हुआ था। मैंने गरदन घुमाकर देखा। मेरे कन्धों पर अपना भार डाले जो व्यक्ति बैठा था, उसकी गोद में बूढ़ा अकड़ा पड़ा था। सूखी लकड़ी सा निर्जीव। बूढ़े की सद्गति हो गई थी। इतनी सुखद मृत्यु। बेटे की गोद में, गंगा किनारे, ठीक आरती के समय। ''मैं तेरी गोद में सिर रखकर मरी होती, अमला, तो मुक्ति मिल गई होती मुझे।” ''ठीक से देखो, माँ, बेटा बाप की गोद में मरा पड़ा है, बाप बेटे की गोद में नहीं। मैं तुम्हारी गोद में सिर रखकर मरती। तब भी...” सच! आँसू पोंछ कर देखते ही समझ में आ गया। मेरे कन्धे से कन्धा लगाए जो बैठा था, बूढ़ा ही था। उसकी गोद में उसका अधेड़ बेटा जड़ पड़ा था। उसकी काठ हुई देह को लाठी की तरह थामे बूढ़ा अब भी माँ, गंगा माँ, बुदबुदा रहा था। मेरा सर्वांग काँप गया। पर मैं हिली-डुली नहीं। मेरा सहारा हटते ही बूढ़ा भरभराकर गिर पड़ता। मैंने हाथ बढ़ाकर पास खड़े आदमी का कुर्ता पकड़कर खींचा। उसने देखा। औरों ने भी देखा होगा। चार-पाँच लड़कों ने झुक कर मृतक की देह को बूढ़े की गोद से उठा लिया। हाथ की लाठी छूटते ही बूढ़ा काँपते पत्ते की तरह पीछे गिरा। मैंने उसे अंक में भर लिया। छोटे बच्चे की तरह। वह अब भी माँ, माँ उचारे जा रहा था। ''अमला, अमला,” मैंने पुकारा। ''क्यों इतना सोच करती हो माँ, मृत्यु मृत्यु होती है, कहीं भी, कैसे भी हो।” ''नहीं, मुझे बतला, क्या रहस्य था तेरी मृत्यु के पीछे? वह दुर्घटना थी या हत्या या...? मुझे बतला।” ''यह क्या है, माँ? दुर्घटना, महाप्रयाण, निर्वाण या लम्बे अभाव के कारण हुई हत्या?”



''सवाल मत कर। मैं तेरी तरह वकील नहीं हूँ टीचर भर हूँ। पर बच्चों को तभी पढ़ा पाऊँगी, जब मन को शान्ति मिलेगी। यह सब क्यों हुआ, बेटी! मुझे बतला, मैं क्या करूँ?” ''जीवन को सँवारो, माँ, और क्या है करने को।” ''कैसे अमला?” मैंने पुकारा। ''अंत्येष्टि के लिए चलो माँ।” कोई लड़का मुझे बाँहों से घेर कर उठाते हुए कह रहा था। मैंने देखा, बूढ़ा मेरी गोद से किसी युवक की गोद में पहुँच चुका था। कुछ और लड़के मुझे घेरे खड़े थे। ''आओ माँ,” लड़के ने पुचकार कर मुझसे कहा। ''अमला, अमला,” मैंने पुकारा। कोई जवाब नहीं मिला। ''वह चली गई,” मैं फूट-फूटकर रो दी, ''मुझे छोड़कर चली गई।” उन्होंने मुझे बेटी का नाम लेकर रोने दिया। फिर धीरे-धीरे, बिना जल्दी मचाए, मुझे उठाकर खड़ा किया। मैंने एक लड़के के कन्धे का सहारा लिया और उनके साथ चल पड़ी। फूलों की पंखुड़ियों से लदी पत्ते की नाव उन्होंने मेरे हाथ से लेनी चाही, पर मैंने अपनी पकड़ नहीं छोड़ी। अंत्येष्टि के लिए मेरे पास पुष्पांजलि रहे और आँखों में आँसू। इस बार रोदन को भीतर नहीं घोटँूगी, जी भरकर रोऊँगी। (1992)
………………………….
कविताएं
1
एक थी पदमा नदी अल्हड़ आवारा या बदचलन? अनगिन महबूब नहीं थे उसके दो आशिक़ों की माशूका थी एक का नाम हिन्द दूसरा बंग था उनके बीच इतनी बार डोलती कभी इसके आग़ोश में कभी उसके लगता सौ पचास के साथ सो ली जब जब आशिक़ बदलती आफ़त आ जाती कगार टूट टूट कर गिरते झोंपड़े तिनकों से उड़ जाते मछलियाँ रेत पर तड़पतीं उत्ताल लहरों के आलिंगन से मछुआरे बमुश्किल जान बचाते पदमा इतराती अठखेलियाँ करती कुदरत कहती अल्हड़ है सम्भल जाएगी भटकना छोड़ एक ठौर ठहर जाएगी पर पदमा न बदली न सम्भली कुदरत का सब्र चुक गया वायु से कहा उठा चक्रवात पदमा समझ जाए बंदिश लगाने को कोई है वायु ने चक्राकार उछाला हिलकोरा खाती तरंगों को पदमा खिलखिलाई चलूँ उस ओर इधर समन्दरी झंझावात उठ आया जैसे ही पलटी पीछे से किसी ने जिस्म उसका दबोच लिया गुस्से से फनफनाई छोड़ो बंग वह साँस घोटती दानवी जकड़ उस नफ़ीस महबूब की नहीं थी विकराल अम्फ़न घात लगाये बैठा था जैसे ही हवा ने चक्रवात उठाया जबड़े खोल उसे निगल लिया विकट राक्षसी ताक़त से लैस बाहर उगला कि क़यामत आ गई समुद्री बेला की ऊँचाई पहाड़ों से होड़ लेने लगी तूफ़ान का वेग ऐसा पहाड़ों को चक्राकार घुमा दे एक बाँह की जिन्नाती गिरफ़्त में सिर धुनती पदमा को जकड़े समन्दरी तरंगे उछाल धरती धराशायी कर ऐसा ताण्डव किया अम्फ़न ने कि शिवशंकर त्राही त्राही कर उठे दोनों आशिक़ों के पाँव तले कगार धसके कि समन्दर सदाबहार पर काबिज़ हुआ वे तटीय हिन्द-बंग के जादुई सुन्दरबन वे नायाब जड़ी-बूटियाँ पेड़-पौधे वे जीव जन्तु परिन्दे सरीसर्प वे सुन्दरी गगंवा निपा के पेड़ वे शेर जंगली बिल्ली चीतल ऊद जल किरात अजगर कोबरा कच्छप वे सफ़ेद सारस बाज़ हार्नबिल सुर्ख़ाब वे रंग बिरंगे दमकते कौरिल्ला वह पदमा की मदमाती चाल वह ज़िन्दगी की थिरकन आह नेस्तनाबूद हो गये और इंसान...कहाँ गये इंसान... वह कबीलों से विलगे आदीवासी वह जंगल में कच्चे घरों के निवासी वह समन्दर में बेख़ौफ़ उतरे मछुआरे वह सांवले सलोने ज़मीनी इंसान... तबाह कर सुन्दरबन वायु का वेग धीमा पड़ा तरंगों का उठान कम हुआ पेट भरे अजगर सा अम्फ़न जिस्म ढ़ीला छोड़ सो रहा कब तलक...पर ...कब तलक ...
2
इच्छित मृत्यु मृदुला गर्ग पितामह अंतिम क्षणों में पास तुम्हारे अर्धसत्य के नायक धर्मराज आये थे नीति-अनीति का ज्ञान लेने दिया तुमने दिया द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर भी मूक रह देख चुके जब चीर हरण कुरु राजसभा में जहाँ तुम चाकर थे मूक रहे पर बधिर न थे कदापि कान लगा सुना द्रौपदी का प्रश्न नृप धर्मराज ने दाँव पर मुझे लगाया स्वयं को हारने से पहले या बाद में सम्भाली तुरंत राज वकील की कमान दाँव पर लगाना तर्क सम्मत ठहराया युक्ति खोजी न्याय व धर्मशास्त्र में नृप स्वयं को हार दास बना तो क्या दास की पत्नी भी होती उसकी सम्पत्ति इसी कूटनीतिज्ञ कौशल का ज्ञान लेने आये थे धर्मराज पास तुम्हारे? कुशल वकील बनने को भीष्म कहलाये तब देवव्रत पितामह नाम क्या बुरा था? मेरा प्रश्न कुछ और है उत्तर दो कैसा लोकातीत कल्पनातीत विलक्षण वरदान मिला था तुम्हें इच्छित मृत्यु! वरण की नहीं क्यों वकील बनने से पहले पिता की कामुकता को श्रद्धेय मान सौतेली माँ व वंशजों की रक्षा हेतु शपथ ली राजपाट त्याग ब्रह्मचारी रहने की भीष्म थी शपथ सो भीष्म कहलाये पर वरदान भी मिला भीष्म लोकातीत विलक्षण इच्छित मृत्यु! कुरु नृप ने तुम्हारी सम्मति नकार दास बनाया अनैतिक निर्णयों का तब पितामह किस लोभ में तुमने अलौकिक वर का लाभ न उठाया इच्छित मृत्यु का वरण न किया जीते गये कुरु राज की चाकरी में अप्रतिम चाकर बनने को भीष्म कहलाये तब देवव्रत पितामह नाम क्या बुरा था? द्रौपदी के प्रश्न का उत्तर दिया मेरे प्रश्न का दोगे न पितामह यह क्या... संशय उठ आया मेरे अपने तर्कशील मन में प्रथम कुकर्म तुम्हारा अपना था कुरु राजपुत्र का आदेश नहीं अपहरण किया स्वयं इच्छा से दो भाइयों हेतु तीन युवतियों का शिखन्डी वध करता या करता नर पुंगव मृत्यु रहती तुम्हारी नारी का प्रतिशोध इसीलिए इच्छित मृत्यु वरण न की जानते थे अम्बा का प्रतिशोध लेगा जन्म जन्मांतर और तुम्हें जीना होगा पीढ़ियों तक प्रायश्चित की प्रतिक्षा में लो दे दिया उत्तर मैंने अपने प्रश्न का फँस गई यधिष्ठिर सम अर्ध सत्य में। बहुत बरस बाद बल की कूटनीति से अपहृत किया तुमने गांधारी को जन्मांध राजकुमार की पत्नी बनाने नीति शास्त्र ने नृप बनने न दिया पर बलपूर्वक पति बनाने में संकोच न था तब अम्बा का जन्म जन्मांतर का कष्ट अछूता छोड़ गया न तुम्हें कुकर्म राजसत्ता के नहीं तुम्हारे थे आंतिम क्षणों में पितामह स्वीकार पाये अपने दुष्कर्म और हुए लज्जित उठाया क्यों विवेकहीन राजसत्ता की मूक चाकरी का भीष्म कष्ट यही ज्ञान दिया अर्ध धर्मराज को अपने और धरा के अंतिम क्षणों में मेरा प्रश्न कुछ और है उत्तर दो भीष्म कष्ट सहा क्यों पीढ़ियों तक पितामह बनने से बहुत पहले वरण क्यों न की इच्छित मृत्यु वही करना था जो किया तुमने देवव्रत पितामह कहलाना क्या बुरा था?
3
एकान्त नहीं कोरोना काल में मृदुला गर्ग मुझे एकान्त की आदत है मुझे एकान्त प्रिय है एकान्त में स्मृति जगती है बेआहट बेआवाज़ ऐसे कैसे आ जाता प्रेमी निःशब्द अचानक पास इतने कितने चुम्बन पाती आत्मा मूक निर्बाध ज्यों प्रकृति हरियायी हँसी नहीं आँसू नहीं हल्की स्मित ओंठों पर दूर चिड़ियां चहचहातीं ऐसे कैसे धीमे से मौन भंग नहीं होता स्मित में आता फैलाव स्मृति हरियाती ज्यों प्रकृति एकान्त बना रहता बेआहट बेआवाज़... जब से कोरोना काल आया एकान्त मिला नहीं पल भर घर में अकेले क़ैद कान सुनते इतनी कितनी भीषण आवाज़ें भूखे बच्चों का करुण क्रन्दन बेघरों का सिसकता प्रलाप बेरोज़गारों का हुजूम ऐसे कैसे दो दो मीटर दूर जैसे फ़ौज की टुकड़ी बूटों की धमक से जिसके टूट जाते हैं पुल प्रेमी ठिठका रहता चौखट पर धकियाया-सा बेआवाज़ गलों से आतीं इतनी कितनी चीखें स्मृति मूर्छित हो जाती एकान्त की धज्जियां उड़ जातीं
4
कौन डरता है मरने से अपने मरने से कौन डरता है कौन डरता है अपने मरने से हम डरते हैं उनके लिए जो बिना डरे, अन्याय से लड़े और बहुतों की मदद कर शेष हो गये यौवन की दहलीज़ पर हम प्रवचन सुनते रह गये मरना तो है एक दिन बिला डरे मरो प्यार में मरो अन्याय से लड़ कर मरो और वह शेष हो रहा… श्रीकृष्ण की अनुमति के बावजूद अभिमन्यु वध का प्रतिशोध न ले सके किससे लेते…हमें घेर लिया था अनेक देसी विदेशी अनजान जनों ने सुना रहे थे गाथा उसकी मदद करने की जितने मुँह उतनी बातें उतनी दुआएं कुछ दिलदार तो कुछ दिलफ़ेंक…वही बतलाती हूँ… हँस कर कहा किसी ने माँ-बाप के विरोध को धता बतला पंडित बुला करवाई सगाई हमारी आप ही के घर की छत पर माँ बाप नाराज़ नहीं हुए आनन्दित थे बिला दहेज़ शादी से हमसे ज़्यादा आशीर्वाद दिया उसे समाज की लंतरानी से बचा लिया बतलाओ श्रीकृष्ण असर हुआ नहीं क्यों …कहते हो गीता पढ़ो कर्म करो फल की चिन्ता न करो जिएंगे नहीं तो फल पाएंगे कैसे अगले जन्म में ओह हाँ आत्मा अनश्वर है पर श्रीकृष्ण हम तब भी डरते थे जब वह था अब डरते हैं अगले जन्म के लिए फिर से डरे बिना वह जिया और बिना डरे मर गया यौवन क़ी दहलीज़ पर हम सुनते रह गए प्रवचन मरना तो है एक दिन मरने से क्या डरना कब कविवर कब श्रीकृष्ण कब होगा यह एक दिन मरना अस्सी बरस की पकी आयु में या मुहब्बत के परवान चढ़ते ही तीस बरस पूरे होने से पहले मृदुला गर्ग
………………………….
फोटो



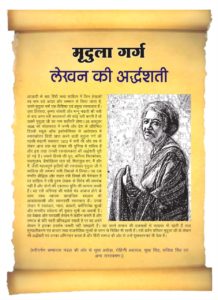
………………………….
