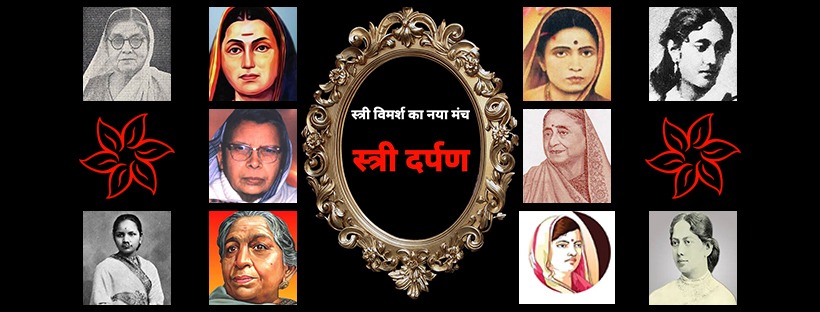(असंबद्ध भाषाऔं के बीच का विवेक)
रवीन्द्र त्रिपाठी
अनामिका अनु के पहले काव्यसंग्रह `इंजीकरी’ पर बात करते हुए एक स्पष्टीकरण जरूरी लगता है। वो ये कि इस संग्रह की कविताएं भले ही नारीवादी चेतना की सशक्त अभिव्यक्तियां हों लेकिन इन्हें सिर्फ इतने तक सीमित रखना इनके साथ अन्याय होगा। साथ ही दूसरा स्पष्टीकरण भी जरूरी है कि नारीवादी चेतना की अभिव्यक्ति के रूप में इन कविताओं का आस्वाद भी आवश्यक है। इन दोनों स्पष्टीकरणों का निचोड़ ये है कि अनामिका अनु की कविताओं को पढ़ते और गुनते हुए उनके काव्यतत्व की संश्लिष्टता का ध्यान रखना आवश्यक है।
इन दिनों समकालीन हिंदी कविता की एक विशिष्टता युवा स्त्री- कवियों ( कवयित्री शब्द आज के नारीवादी समय मे बेमानी हो गया है) का उदय है। हिंदी कविता में अच्छी संख्या में स्त्रियों की उपस्थिति पिछले तीस-बत्तीस साल से लगातार बढ़ी है। इसी का पहला नतीजा ये है कि कई महिला-कवि वरिष्ठों की सूची में भी आ चुकी हैं और आज की हिंदी कविता पर बात करते हुए उनकी उपेक्षा असंभव है। और दूसरा नतीजा ये है कि आज की युवा हिंदी कविता, और इसमें अमूमन चालीस की उम्र के इर्दगिर्द के कवि शामिल हैं, मोटे तौर नारी- कविता भी हो गई हैं। कहने का आशय ये है कि युवा कविता में स्त्री- स्वर की उपस्थिति अब अल्पसंख्यक नहीं बल्कि बहुसंख्यक हो गई है। संख्या के स्तर पर ही नहीं गुणवत्ता के स्तर पर भी। अगर उम्र के आधार समकालीन कविता को पढ़ा जाए तो युवा स्त्री- कविता ज्यादा देदीप्यमान दीखती है। हालांकि कइयों को इस स्थापना पर आपत्तियां होंगी जिनमें कुछ जायज भी होंगीं। लेकिन ये भी कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इस तरह की स्थापना, प्रथम दृष्ट्या भले सरलीकृत या एकांगी लगे, लेकिन जो बहुविध उर्वरता आज की युवा स्त्री- कवियों में दीख रही है वो हिंदी कविता के इतिहास में नई और सुखद घटना की तरह है। भविष्य का संकेत भी। ये लैंगिक विमर्श (जेंडर डिस्कोर्स) के लिहाज से भी महत्त्वपूर्ण है और साहित्य की दृष्टि से भी।
हालांकि इस पहलू को भी सही परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है क्योंकि बेकार का वितंडा खड़ा करने वाले कुछ लोग भी आजकल हिंदी की दुनिया में अतिशय सक्रिय हैं। ये ठीक है नारी-कविता औऱ पुरुष-कविता के बीच एक स्तर पर फर्क बेमामी भी है क्योंकि मैं भी ये मानता हूं कि कविता मुख्यत: और अंतत: कविता होती है; चाहे वो पुरुष की हो, स्त्री की हो (या उभयलिंगी की हो)। पर ये एक तात्विक सच है। समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें, जिसके बिना साहित्य और समाज के संबंध को समझना कठिन है, तो स्त्री- कविता, दलित- कविता, आदिवासी – कविता आदि संकल्पनाएं भी सामाजिक उभारों- बदलावों और उनके सिलसिले में साहित्य के भीतर गतिशील प्रवृत्तियों को जानने, पहचानने और समझने के लिए आवश्यक हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो `छायावादी कविता’, `नई कविता’ और आज की कविता आए में गुणात्मक फर्क की समझना मुश्किल हो जाएगा। और आप समाज के भीतर प्रकट हो रहे उभारों को भी नहीं चीन्ह पाएंगे। कविता को समझना समाज को भी समझना है। आकस्मिक नहीं कि आज हिंदी समाज में आदिवासी कविता में स्त्री स्वर भी उभरा है और उसे मान्यता मिली है। इसके पीछे कारण ये है कि आदिवासी जीवन में कई तरह के परिवर्तन आ रहे हैं।
ऐसे में युवा स्त्री कविता का मूल्यांकन आसान भी हो जाता है और कठिन भी। आसान इसलिए कि कोई युवा-स्त्री-कविता को मात्र नारीवादी ढांचे में रखकर उसका आकलन कर सकता है। ऐसा हो भी रहा है और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि किसी दौर में जब कोई नई साहित्यिक प्रवृत्ति उभरती है तो उसे किसी खास श्रेणी में वर्गीकृत कर उसे व्याख्यायित किया जाता है। किंतु इस तरह की व्याख्या के खतरे भी हैं। जैसे आप सभी युवा-स्त्री-कविता को सिर्फ नारीवांदी सांचे में ढालकर देखने लगें तो उससे भी सरलीकृत निष्कर्ष निकलते हैं। हर कवि की अपनी निजता भी होती है और उसे पहचाने बिना आप न कविता का आस्वाद कर सकते हैं और न उसका मूल्यांकन। सवाल ये भी रहता है उस कवि में ऐसा क्या है जो दूसरों से अलग है। हर स्त्री कवि एक ही ढंग की कविता नहीं लिख रही है। उनमें भी विभिन्न्ता है।
चलिए अब अनामिका अनु की कविता पर बात करें। उनकी काव्य संवेदना और काव्यभाषा में निहित स्थानीयता और नारीवादी स्वर की चर्चा अधिक हुई है। उनके यहां घर-परिवार, माता पिता के प्रति लगाव की भी भरपूर अभिव्यक्ति है। जिस बिहारी (मुजफ्फरपुरी) परिवेश में उनका जन्म हुआ और जहां उनकी पढाई लिखाई हुई, वहां की भाषा औऱ बोलीचाली का असर उनकी रचना पर न हो ऐसा संभव नहीं। इसलिए लीची (लीची शहर की सूनी छत) जैसे फल और बेगुसराय (मास्को में है क्या कोई बेगुसराय) जैसी जगहें उनकी कविताओं में आती हैं तो ये स्वाभाविक है। पर अनामिका अनु का काव्यबोध बिहार से बाहर भी निकलता है कई राज्यों और देशों में फैल जाता है। उस नदी की तरह जिसका उद्गम तो कोई एक स्थान पर होता है लेकिन जो बहते बहते कई देश- देशांतरों को समेट लेती है। एक छोटी सी जलधारा कई पड़ावों से गुजरती हुई एक विशाल जलराशि में बदल जाती है। एक ऐसी नदी की तरह अनामिका अनु की कविताओं में बहु-स्थानिकता आ गई है। और बहु- सांस्कृतिकता भी। यानी इन कविताओ में बिहार है तो मिजोरम भी है, राजस्थान भी है, अरुणाचल प्रदेश मे थांका पेंटिंग बनाती लड़की भी है, दागिस्तानी कवि-लेखक रसूल हम्जातोव का गांव भी है और वियतनाम भी है जहां 1968 में कुछ अमेरिकी अफसरों के कहने पर `माई लाई’ सामूहिक हत्याकांड हुआ था औऱ वहां कई लोग मारे गए थे। इस पर पूरी दुनिया में हंगामा हुआ था। अमेरिकी फोटोग्राफर रोनाल्ड एल हायबेरले ने जब उस सामूहिक हत्याकांड में मारे गए लोगों के फोटो लिए थे तब पता चला कि जो मारे गए उनमें बड़ी संख्या में, महिलाएं, बच्चियां और नवजात शिशु भी थे। उसी को याद करते हुए `माई लाई गांव की बच्चियों की कब्र’ कविता में अनामिका लिखती हैं
माई लाई गांव में मारी गईं
कुछ बच्चियां शिन्ह पेंटिंग बन गईं
कुछ फूलों की क्यारियां
कुछ प्राचीन लाल टाइलों वाली छत
और दीवारें
कुछ अब भी विचरती रहती हैं
गोल नाव में बैठकर वे देखती हैं
कभी आकाश तो कभी नारियल के पेड़
यहां इन पंक्तियों की व्याख्या की कोई आवश्यतता नहीं है। बस इतना कह देना ही पर्याप्त है कि ये पंक्तियां हिंदी कविता के आयतन का विस्तार भी करती है क्योंकि इसके दायरे में सिर्फ राष्ट्रीय ही नहीं अंतरराष्ट्रीय जगत भी आ रहा है। कुंवर नारायण, अशोक वाजपेयी और विष्णु खरे जैसे कवियों ने भी ऐसा किया है।
अब चलें अन्य विंदुओं की ओर जिनके कारण भी अनामिका अनु की कविताओं की अपनी इयत्ता है। बाकी कवियों से अलग। कई वजहों से भी, खासकर वैश्वीकरण के बाद आज के भारतीयों को विभिन्न जगहों पर रहना या नौकरी करना पड़ता है। यही नहीं, बिहार- उत्तर प्रदेश के मजदूरों का भी दूसरे राज्यों में आना- जाना- रहना हो रहा है। एक वक्त था जब बिहार के मजदूर ज्यादातर पंजाब जाते थे पर आज की तारीख में वे केरल -कर्नाटक आदि राज्यों में भी जा रहे हैं। और सिर्फ मजदूर ही नहीं मध्यव्रर्ग के लोग भी नौकरी और रोजगार के लिए अपने अपने राज्य को छोड़ दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। इसीलिए हिंदी भाषा अब सिर्फ हिंदी राज्यों की भाषा नहीं रह गई है। आजादी के पहले हिंदी भाषी राज्यों के लोग रोजगार की तलाश में कोलकाता जाते थे। उसके बाद कल के बंबई यानी आज के मुंबई जाने लगे। फिर सूचना उद्योग के विस्तार की वजह से बंगलुरू, पूना, हैदराबाद, त्रिवेंद्रम जैसे शहरों में। स्वाभाविक है मजदूर से लेकर दूसरे मध्यवर्गीय पेशे वालों की स्थानीयताएं बदल रही है। उनकी सोच और संस्कृति में नई चीजें जुड़ रही है। इसलिए हिंदीवाला अब सिर्फ हिंदी प्रदेश वाला नहीं रहा। वो हिंदीवाला है पर साथ ही बंगलुरूवाला या पूनावाला भी हो गया। ऐसे में हिंदी के कवियों और लेखकों के अनुभव-क्षेत्र भी बदल रहे हैं और उनके लेखन में भाषाई अंतर्क्रियाएं भी हो रही हैं। अनामिका अनु बरसों से केरल में रह रही हैं। उनकी कविताओं में भी केरल की रंगतें- मलयाली संस्कृति, परिवेश, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, जगहें, और साहित्यकारों की रचनाओं के प्रसंग आदि प्रवेश कर चुके हैं। वो शायद हिंदी की अकेली कवि हैं जिनमें केरल की संस्कृति की इतनी सशक्त उपस्थिति हैं।
ये बोध `इंजीकरी’ संग्रह में प्रचुरता से मौजूद है। ये मलयाली परंपरा से जुड़ा काव्यसंग्रह भी है।
इंजीकरी केरल या मलयालम में अदरक (इंजी) से बनी करी (उत्तर भारत में कढ़ी) को कहते है। हां, इसमे अदरक अलावा भी कई चीजें होती हैं। इंजीकरी से जुड़ी एक लोककथा भी केरल में प्रचलित है जिसमें एक युवा, मेधावी औऱ शादी के प्रति अनिच्छुक विद्वान के सामने एक प्रवास के दौरान एक घर में एक कन्या के साथ शादी का प्रस्ताव रखा गया तो उसने कहा कि यदि एक घंटे में वो लड़की एक हजार इंजीकरी खिला दे तो वो शादी कर लेगा। कन्या ने सिर्फ एक इंजीकरी बनाई और वो इतनी स्वादिष्ट थी कि उस युवा विद्वान को हजारों इंजीकरी के बराबर लगी। अनानिका अनु की इस पहली `इंजीकरी’ में भी इतना रस है कि साहित्य के सहदयों को बहुसांस्कृतिक और बहुस्थानिक रसात्मकता का बोध होगा। कवि अनामिका अनु की अस्मिता का विस्तार हो चुका है। इन पंक्तियों से इसे समझा जा सकता है-
मैं कोट्टारक्करा तंपुरान राजा का रामनाट्म हूं
मैं मंदिरो मे पुष्प बटोरती स्त्रियों का दासीअट्म हूं
इस संग्रह की आखिरी कविता `दो पत्र जो गंतव्य तक नहीं पहुंचे’ में आन्ना (जो कवि का ही दूसरा नाम है) कहती है- `कावालंब चलोगे मेरे साथ, नाव पर बैठकर जायेंगे। मुझे अयप्पा पणिकर के स्म़तियों वाले कावालंब से मिलना है। अयप्पा कहते हैं बीमार प्रेमी को प्रेमिका का एक स्पर्श चंगा कर देता है। तो बीमार प्रेमिका को भी प्रेमी का स्पर्श चंगा करता होगा न! बोलो न! अयप्पा सच ही कहते होंगे न?
………….
आओगे न! साथ में तरलि अप्पन बनाएंगे, भाप में पकती खूशबू में भीगकर मैं एक गीत लिखूंगी, विरह गीत।‘
ये पंक्तियां मूल रूप से लिट्टी- चोखा और लीची के इलाके की रहनेवाली कवि का तरलि अप्पंम या (दूसरे मलयाली व्यंजनों) का स्वाद –विस्तार भर नहीं है बल्कि फणीशवर नाथ रेणु की एक प्रशंसिका का मलयाली लेखक अयप्पा पणिकर की मुरीद बनना भी है। इस संग्रह में रेणु की एक कहानी `रसप्रिया’ से प्रेरित एक कविता- `जी नहीं रहे हैं जनाब थेथरई कर रहे हैं’ भी इस संग्रह में है। अनामिका अनु की ऐसी कविताओं से हिंदी वालों की रसानुभूति का विस्तार भी होगा। रेणु की कहानियों के रसिक अय्यप्पा पणिकर और दूसरे दक्षिण भारतीय लेखकों- कवियों की रचनाओ के रस से सहज ही जुड़ सकेंगे।
हिंदी गद्य और कहानी में इस तरह के रस-बोध विस्तार की जमीन निर्मल वर्मा ने तैयार की थी।। उन्हीं के कारण पूर्व चेकोस्लोवाकिया, और अब चेक गणराज्य की राजधानी प्राग, की संस्कृति हिंदी पाठकों के सहज बोध का हिस्सा बन गई है। कविता में कुछ कुछ इसी तरह की भूमिका अनामिका अनु की है। मुझे नहीं मालूम कि हिंदी के किसी और कवि-लेखक ने केरल को इस तरह हिदी पाठकों के बोध का हिस्सा बनाया है। इस कारण अनामिका के इस संग्रह की सिर्फ साहित्यिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक अहमियत भी है। ये हिंदी की अ-स्थानीयता भी है और स्थानीयता का विस्तार भी। यही वजह है कि अनामिका अपने को `अंसबद्ध भाषाओं का विवेक कहती है’ और अपनी एक अन्य कविता में लिखती हैं-
मुझे मेरे शहर के जाति, धर्म पूछते लोग शकुनि या धृतराष्ट्र से लगते हैं, जिनकी या तो आंखें अंधी हैं या मन। चलो न! इन अंधों के बीच से भागकर फिर पेरियार के तट पर चलते हैं वहां `तकषि का कुत्ता’ पढ़कर साथ में खूब रोएंगे, प्यार लौट आएगा। अगर तुम आ सको तो आना और जल्दी आना।
अपनी एक अन्य कविता तथाकथित प्रेम में में उनका कहना हैं-
तथाकथित प्रेम, मिट्टी में रिस-रिस कर
उस नदी में मिल जाएगा जिसे लोग पेरियार कहते हैं
पेरियार दक्षिण भारत की नदीं है और प्रेम या तथाकथित प्रेम की उस नदी में मिलना भी गंगा के इलाके की रहनेवाली कवि और पाठक के काव्यमन का विस्तार ही है। उत्तर भारत के लोग गंगा और नर्मता से विशेष प्रेम करते हैं। इसमें कुछ अनूचित नहीं है। लेकिन कावेरी या पेरियार उनके बोध में कम क्यों हैं? अगर आप उत्तर भारतीय से आगे बढ़कर संपूर्ण भारतीय बनना चाहते हैं देश की सभी नदियों को अपना मानना होगा। तथ्य के स्तर पर नहीं बल्कि संवेदना के स्तर पर। और यही राष्ट्रीयता की सच्ची परिभाषा है। हर उत्तरभारतीय को एक ऐसा सार्वदेशिक बोध विकसित करना होगा जिसमें देश की हर नदी चेतना में सहज रूप से आ जाए। इस तरह कि मन में आए कि पिछले साल गंगा स्नान किया था तो इस साल कावेरी-स्नान किया जाए। जब हम इस संग्रह में पद्मनाभास्वामी मंदिर, श्री वड्डाकुनाथन मंदिर, त्रिरूवामबाड़ी मंदिर, परामेकावु देवी मंदिर, वड़ाकुंडा मंदिर, कडला पायसम ( चने की दाल की खीर जो कोकोनट मिल्क से बनती है) का उल्ल्ख पाते हैं तो अनायास ही कहने का मन हो जाता है अनामिका अनु हिंदी कविता का सार्वदेशिक विस्तार हैं।
अनानिका में बहुसांस्कृतिकता के साथ साथ बहुधार्मिकता भी है। ये प्राय: कहा और लिखा जाता है कि भारत एक बहुधार्मिक देश है। किंतु इसी के साथ दूसरा तथ्य ये भी है कि आज के भारत में बहुधार्मिकता की धारणा पर लगातार आघात हो रहे हैं। खासकर कुछ राजनैतिक दलों औऱ संगठनों की ओर से। दूसरे धर्म या धर्मों को अपने धर्म का विऱोधी माना जाता है और उनके समूल नाश की बाते हो रही है हैं। ऐसे लोगों के लिए यही `केरला स्टोरी’ है। पर अनामिका अनु की केरला- स्टोरी अलग है। समावेशी और बहुधार्मिक।
कृष्ण की मजार पर चादर हरी हरी सजी है
मरियम के बुर्के में सलमा सितारा है
अल्लाह के मुकुट में मोर बंधे हैं
नानक के सिर पर नमाजी निशान हैं
(मैं भूल जाती हूं)
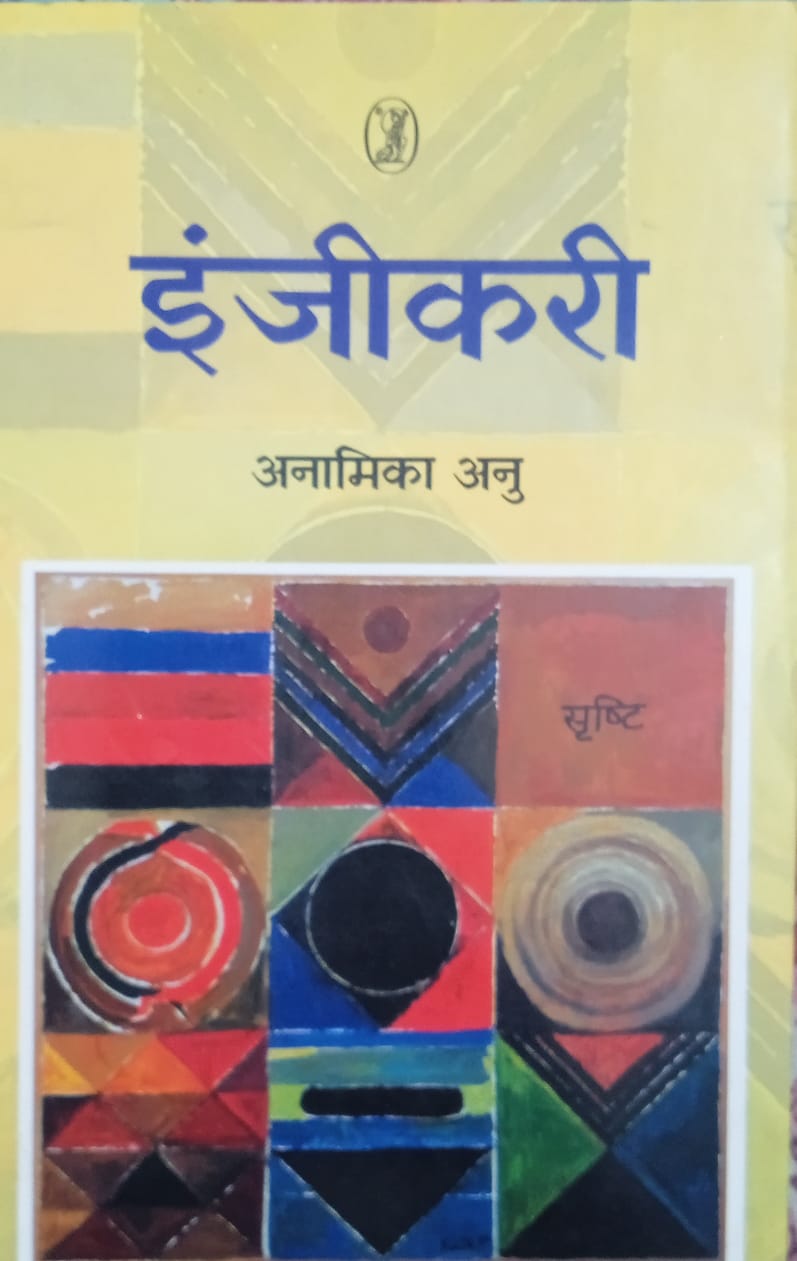
हम सबके अनुभवों में कई वाकये होते हैं जो मन के भीतर दर्ज रहते हैं। ये इनमें परिवार की या आसपास के कई ऐसे चरित्र होते हैं जो असंवेदनशीलता के शिकार हो जाते हैं। इस तरह के वाकयो में यों तो कोई बड़ी कूरता के निशान नहीं होते। फिर भी परिवार या समाज या दोनों के कुछ कारनामें ऐसे होते हैं जो किसी व्यक्ति पर भारी पड़ते हैं। कोई संवेदनशील मन ही इनको इनको देख और समझ सकता है। इस संग्रह में अनामिका अनु की एक कविता है `दौड़ू’। कविता एक बयान की तरह है जिसका एक ऐसा आदमी है जिसकी जिंदगी अपने संयुक्त- परिवार के लिए खटने में खत्म हो जाती है। ऐसे परिवार आज भी गांव- जवार में होते हैं जिनमें कुछ पुरुष सदस्य ठीक से पढ़ लिख नही पाते क्योंकि वे अपने परिवार के बड़ों- पिता, भाई, चाचा, मां, भाभी, बुआ – के इस तरह के आदेशों का पालन करते हैं – `मिल से गेंहूं पिसा ले आ, फलां को स्टेशन या बस स्टैंड पहुंचा दो, रात के किसी रिश्तेदार की तीमारदारी के लिए अस्पताल में रहो’.. आदि आदि। आगे चलकर जब इनकी शादी हो जाती है तो ऐसे लोगों की पत्नियां भी इसी तरह के कामों में लगी रहती है। और अंतत: इनका व्यक्तित्व हमेशा के लिए दबा दबा रह जाता है और इनका परिवार भी आर्थिक मामलों में पिछड़ जाता है। इनके `योगदान’ या `अवदान’ का परिवार में कोई कभी उल्लेख भी नहीं करता। इन बातों को याद रखेंगे तभी `दौड़ू’ कविता और उसकी ये पंक्तियां दिमांग में घंटी बजाएंगी-
दौड़ू कभी एक साथ नहीं ला पाता
पत्नी के लिए साया साड़ी ब्लाउज टिकली और
सिंदूर
दौड़ुओं की पत्नियां ही जीतीं
औऱ खूब खटती हैं
ये है अनामिका अनु के काव्य संसार की परिधि। इसका फैलाव अंतरराष्ट्रीय जगत से लेकर राष्ट्रीय और पारिवारिक संदर्भों तक है। ऐसे कम समकालीन युवा कवि हिंदी में है जिनकी कविता का दायरा इतना चौड़ा है।