(रूपम मिश्र के कविता संग्रह `एक जीवन अलग से’ पर केंद्रित लेख)
रवीन्द्र त्रिपाठी
कविता का एक काम उन रीतिरिवाजों का परीक्षण करना भी है जिनके बारे में अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये हमारी परंपरा हैं और सनातन भी हैं। और ऐसी परंपरा या परंपराएं अक्सर महिमा-मंडित की जाती हैं और उनको महान और उदात्त बताया जाता है हालांकि वे समाज के एक बड़े वर्ग के लिए जकड़नों का काम करती हैं। परंपरा के नाम पर ये रीतिरिवाज धीरे धीरे समाज के एक बड़े हिस्से में इस तरह अपना लिए जाते हैं या थोप दिए जाते हैं कि दैनंदिन के जीवन में प्रतिमान अथवा दिशा-निर्देश की तरह काम करने लगते हैं। कुछ कुछ लक्ष्मण- रेखा की तरह कि इन्हें पार किया कि समाज और परिवार से बाहर।
वैसे पितृसत्ता की धारणाएं अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में मौजूद हैं लेकिन कुछ जगहों या देशों में वो शिक्षा के प्रसार और औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के विस्तार की वजह से कुछ ढीली पड़ी हैं। भारतीय समाज में भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है। पर ये भी सच है कि भारतीय गावों और कस्बों में अभी भी उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और ये भी सही है कि गांव के रीतिरिवाज अपनी चौहद्दी पार कर शहरों में फैल गए हैं। अर्थात शहरों और कस्बों में भी पितृसत्ता आज बहुत असरदार है। उसकी छायाएं महानगरों पर भी हैं। इसके कई रूप हैं। एक ओर तो पुरुषवाद डंके की चोट पर अपनी ताकत और धमक को कायम रखना चाहता है दूसरे स्त्रियों और महिलाओं की व्यक्तिगत और सामूहिक सोच में भी वह प्रवेश करता है। यानी औरतें भी पितृसत्ताक धारणाओं को अपने भीतर समा लेती हैं।
बेहतर होगा कि इसे रूपम मिश्र की एक कविता के माध्यम से ही समझा जाए। `एक जीवन अलग से’ में उनकी एक कविता है `अन्याय का दुलार’। उसे यहां पूरा ही उद्धृत किया रहा है ताकि समग्रता में पितृसत्ता की शक्ति और महिलाओं में मौजूद उसके रूप समझा जाए –
कुछ स्त्रियां पूरब से आई थीं कुछ पश्चिम से
दक्षिण की ज्यादा उत्तर की कम हैं यहां
उत्तर संख्या में अल्पसंख्यक होता है
बाकी अन्यायी कथाओं की आरोही हुंकारी
ये स्त्रियां ही यहां बहुसंख्यक हैं
और इनके सारे किस्सों मे रानियों की भूल पर देश-निकाला व भयावह मृत्युदंड थे
राजा जो हमेशा दूध का धोया होता है दंडक भी उसी के पास होता है
एक उम्र के बाद उलटे पल्ले और सीधे पल्ले के मत एक हो जाते हैं
चिंताएं आकर फिर अपने हाथ से छूटते जा रहे जमाने पर रूकती हैं
और फिर से इनकी चर्चा में नई लड़कियों के पंख निकल रहे हैं
हालांकि पंख टूट जाते हैं और वो घिसटती हुई एक दिन आकर
इन्हीं की बगल में खड़ी होती हैं और इन्हीं की भाषा बोलती हैं
खैर सारा दोष नई पीढ़ी की स्त्री उड़नबाजी पर है
विमर्श का केंद्र भी एक स्त्री का आशनाई में हत्या है
सभा का समवेत मत है कि ऐसी हत्याएं उतनी ही जायज और जरूरी हैं
जितना बीर बाबा का बहराम, मरी माई के थान पर कड़ाही देना
यें रंग, नस्ल और जेंडर की मक्कारियों का स्वप्रकट मठ था
यहां अन्हराई स्त्रियां स्वजातीय डाह से घटनाएओं की ओझाई करती थीं
ये तिल- तिलकट चना मसूर गेहूं जई को अंखुवाते ही चीन्ह लेती हैं
और अन्याय जवान से बूढ़ा, बूढ़े से अमर भी हो गया
और ये अभी तक उसे गोद में लेकर दुलार रही हैं।

समाज में, विशेषकर महिलाओं के बीच, किस प्रकार उन मूल्यों को आत्मसात कर लिया जाता है कि स्त्रियों के बीच स्वतंत्र चेतना का विकास अच्छा नहीं होता – उसे ये कविता रेखांकित करती है। इसमें औरतों की एक सभा का जिक्र है जो एक लड़की/स्त्री की हत्या पर हो रही है और उपस्थित महिलाएं उस स्त्री/ लड़की को ही दोषी मान रही है। जैसा कि लोककथाओं में होता रहा है – राजा को अपनी उस रानी को दंडित करने का अधिकार है जिसने किसी तरह की भूल की है। और दंड़ भी क्या? मत्युदंड। चूंकि दंडक हमेशा राजा के पास होता है इसलिए रानी कुछ कर भी नहीं सकती। होता ये भी है कि रानी कोई भूल न भी करे और राजा को शक हो जाए कि उसने कुछ गलत किया है तो भी रानी को मृत्युदंड ही मिलता है। कविता में जिस स्त्री की आशनाई की वजह से हत्या हुई है उसका पक्ष सामने नहीं आता है क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे ऐसा करने नहीं देता । स्त्रियों की इस सभा में, जो एक मठ की तरह है, यही सर्वस्वीकृति है कि जिसकी हत्या हुई उसने प्रेम कर ही गुनाह किया। आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि फलां लड़की बहुत उड़ रही है या उसके पंख निकल आए हैं। हालांकि ये मुहावरा लड़कों के बारे में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन उनको गुनाहगार नहीं समझा जाता और न उनको दंड दिया जाता है। लड़की अगर उड़ने की कोशिश करे तो उसे अक्सर सजाए मौत ही मिलती है। ये सजा वैसे ज्यादातर पुरुष देते हैं पर उसमें परिवार और समाज की महिलाओं की भी सहमति होती है और वे हुंकारी भरती हैं कि उड़नेवाली के साथ ठीक किया गया। इनमें वे स्त्रियां भी होती है जो कुछ आधुनिक मानी जाती है। कविता में जिन्हें `उलटे पल्ले’ वाली कहा गया है वो तुलनात्मक रूप से आधुनिक मानी जाती है। और `सीधे पल्ले’ वाली स्त्रियां पांरपरिक या गंवई। (ये दीगर बात है कि आजकल महानगरों में भी सीधे पल्ले का रिवाज चल पड़ा है।) उड़ते पंखों वाली लड़कियां या स्त्रियां किसी को स्वीकार नहीं, चाहे वो सीधे पल्ले वाली हों या उल्टे पल्ले वाली। उनकी नजर में आशनाई में लगी लड़की की हत्या जायज है। और इस तरह ज्यादातर स्त्रियां उस अन्याय का दुलार ही करती हैं जो दरअसल उनके ही विरूद्ध है।
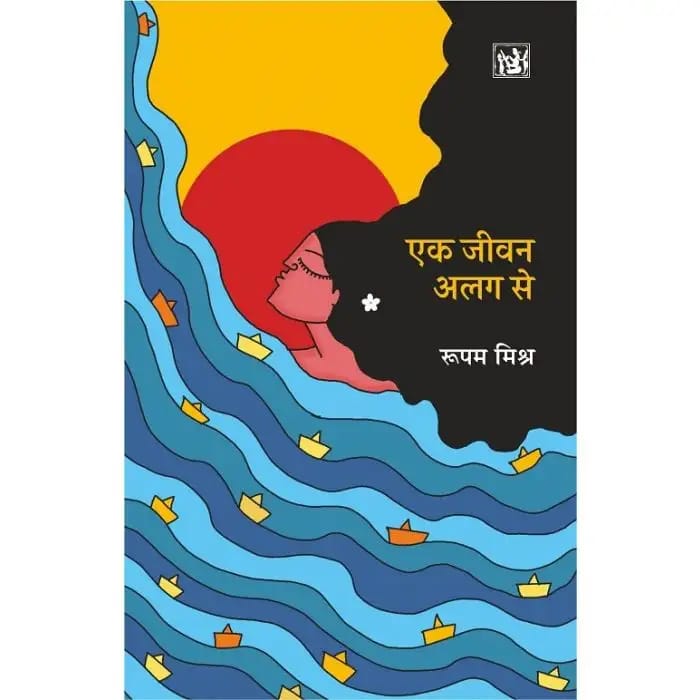
भारतीय समाज में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस कारण सदियों पुरानी और जमी जमाई स्त्री- विरोधी- धारणाएं एक सीमा तक अशक्त हुई हैं। मगर एक सीमा तक ही। फेमिनिज्म यानी नारीवाद की अवधारणा हमारे यहां आई तो समाज में उन मान्यताओं का विरोध भी शुरू हुआ है जो औरतों के खिलाफ होती हैं और जिनकी कानून और संविधान भी इजाजत नहीं देता। किंतु समानांतर रूप से ये भी सच है कि समाज का एक शक्तिशाली वर्ग फेमिनिज्म का विरोध भी करता है। इसमें पुरुष तो शामिल हैं ही, औरते भी हैं। इसीलिए फेमिनिज्म भारतीय महानगरों से लेकर कस्बों – गावों तक निंदा और संदेह का पात्र भी माना जाता है। अक्सर ये कहा और लिखा भी जाता है कि नारीवाद पश्चिम से आई अवधारणा है और इसी कारण संदेहास्पद और अस्वीकार्य भी हैं। गोया पश्चिम से आई हर बात या वस्तु गलत है। पश्चिम से आई रेलगाड़ी, हवाई जहाज व कार जैसे वाहन का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और किंतु फेमिनिज्म के खिलाफ लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं। साहित्य में यथार्थवाद की अवधारणा भी पश्चिम से भारत आई पर उस पर कोई आरोप नहीं लगाता। दक्षिणपंथी ही नहीं कई वामपंथी भी फेमिनिज्म के विरुद्ध होते हैं। इसी कारण भारत में कई लोग – लड़कियों के पिता- दादा, मां- दादी भी – स्त्री- शिक्षा के प्रति भी दुराग्रह पाले रखते हैं और अपनी बेटियों-पोतियों की पढाई लिखाई के प्रति न सिर्फ अनिच्छुक बने रहते है, बल्कि कई बार तो उसका विरोध भी करते हैं। एक आम मुहावरा है जो लड़कियों को लेकर सुनाई पड़ता है – क्या ये कलक्टर बनेंगी? हालांकि लड़किया कलक्टर भी बन रही हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन गावों –कस्बों में उनकी शिक्षा को लेकर दुराग्रह कायम है। इसी को लक्षित करते हुए रूपम की एक कविता है- `चली हैं कलेक्टर बनाने’। इसमें एक लड़की के बचपन से लेकर उसके वयस्क बनने के अनुभवों का बयान है। कविता इस तरह शुरू होती है-
पहली बार स्कूल जाते हुए खूब रोई तो
दादी ने मां को डांटा, नहीं पढ़ती है तो जाने दो
चलीं है कलेक्टर बनाने!
चूल्हे के पास राख पर उंगली से लिखाती
मां फिर डांट दी गई कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ
चलीं है कलेक्टर बनाने
और जब आगे चलकर जब यही बच्ची शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो वहां भी उसे उसी तरह के कटाक्ष सुनाई देते हैं
स्कूल और मां दोनो छूटे
किताबों को हाथ में ही थामे
मैं अब ससुराल आ गई थी
अबोध मन अभी गिरस्ती नहीं सीख पाया था
कदम- कदम पर होती रही गलतियां
जलती उंगलियों पर गीला आटा चिपकाती
सुनती रही सास की कड़क आवाज
कि एक भी शऊर नहीं सिखाया माई ने
चली थीं कलेक्टर बनाने
जिसे भारत में परंपरा बताया जाता है वो अपने तरीके और विधि-विधानों से स्त्रियों के जीवन का नियमन करता है। छोटी बच्चियों से लेकर स्त्रियों को `क्या करना चाहिए’, `कैसे चलना चाहिए’’. `क्यों सार्वजनिक स्थलों पर चुप रहना चाहिए ’(यानी बोलना नहीं चाहिए) – ये सब इस इन विधानों में शामिल होते है। एक बीमारी होती है एगोराफोबिया (agoraphobia ) जो अक्सर महिलाओं में पायी जाती है। इसका एक लक्षण होता है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर जाने या वहां बोलने -घूमने में डर लगता है। वे इन स्थलों पर घबरा जाती हैं। 2016 में इसी पर केंद्रित पवन कृपलानी की एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था `फोबिया‘। इसमें राधिका आप्टे की मुख्य भूमिका थी। हालांकि फिल्म होने की वजह से इसमें एक कहानी भी थी और साथ ही कुछ बातें भी थी लेकिन मूल बात वही थी –अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के पीछे कई तात्कालिक कारण भी होते हैं। पर सबसे बड़ी वजह है भीतर का डर। ये कई वजहों से पैदा होता है। बचपन या युवावस्था में यदि परिवार या आसपास के लोगों द्वारा किसी के भीतर डर भऱा जाए तो वो अगोराफोबिया का शिकार हो सकता/ सकती है। हमारे यहां ग्रामांचलों में ( और ईरान जैसे कई और देशों में भी) लड़कियों पर बचपन से लेकर युवावस्था तक सार्वजनिक जगहों पर जाने या वहां बोलने पर निषेध होता है। एक कविता में इसी की शिनाख्त करते हुए रूपम कहती हैं.
हमें अधिकार का पर्यायवाची कर्तव्य बताया गया
हमने साहस की जगह हमेशा डर पढ़ा
स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में हमने कभी भाग नहीं लिया
क्योंकि आजी कहती मुंहजोरी भले घर की लड़कियों के लक्षऩ नहीं
हमें हमेशा बोलना नहीं सुनना सिखाया गया
तोते की तरह रटाए गए कुछ अति विनीत शब्द
जो गर्दन को और झुका प्रतीत कराते
ये `विमर्श हड़पने की नीति’ है जो समाज में लंबे समय से जारी है। यही कारण है कि फेमिनिज्म का विरोध आम जीवन में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में भी होता है। `अभी हमारी बहुत- सी जगहें हैं जहां हम नही हैं‘ लिखते हुए रूपम सामाजिक उपक्रमों में औरतों की अपेक्षाकृत अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं और अपनी एक अन्य कविता में इसी महिलाद्वेष के परिणाम की ओर भी इशारा करते हुए कहती हैं `कुछ तितलियां बिना उड़े ही बूढ़ी हो जाती हैं’। तितलियों से यहां आशय उन औरतें से है जो जीवन भर अपनी किसी स्वाभाविक और सहज चाहत को अभिव्यक्त भी नहीं कर पातीं। ये वही माहौल हैं जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं है। जब कोई लड़का प्रेम करता है तो ये सहज माना जाता है पर लड़की के प्रेम को गलत कहा जाता है उसके लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो है फंसना। यानी लड़की प्रेम नहीं करती, वह किसी के साथ फंस जाती है – इस जैसा निष्कर्ष अक्सर सुनाई देता है।
इस संग्रह में कई ऐसे सामाजिक वृतांत औऱ वाकये हैं जिनसे हम अक्सर ही टकराते हैं। इस संग्रह में कई कहानियां हैं जो कविता की शक्ल में है। ये कहानियां या कविताएं उन सामाजिक प्रसंगों को सामने लाती हैं जिनमें महिलाद्वेषी दृष्टिकोण उभरते हैं। कुछ ऐसी महिला व्यक्तित्व ( `शालू सिंह’ `विद्योत्तमा शुक्ला’) भी इस संग्रह की कविताओं में आती हैं जो संघर्ष और प्रतिकार की दृष्टांत बन जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र में आए कुछ हालिया तबदीलियों को दर्ज करने की कोशिश भी रूपम ने की है। जैसे जब से पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण जैसे प्रावधान लागू किए गए तब से महिला मुखिया/सरपंचों की संख्या भी बढ़ी है। इससे एक तो ये हुआ कि पंचायती लोकतंत्र की परिधि का विस्तार हुआ है और वहां पुरुष- स्त्री का असंतुलन कुछ कम हुआ। पर दूसरी तरफ उन महिला मुखिया/ सरपंचों के पतियों या पिताओं की पौबारह हो गई है और प्रछन्न अधिकार उनके हिस्से में आ गए। अंग्रेजी मे जिसे`डे ज्यूरे’ और `डी फैक्टो’ कहते हैं उसका समकालीन रूप आज के भारत के कई पंचायतों मे दिख रहा है। `डे ज्यूरे’ या औपचारिक सत्ता तो महिला मुखिया/सरपचों के पास है लेकिन `डी फैक्टो’ यानी वास्तविक सत्ता पुरुषों के पास ही रहती है जिसे पति या पिता इस्तेमाल करते हैं। चूंकि प्रावधानों की वजह से महिलाएं ही आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं इसलिए कई पुरुष अपनी उन पत्नियों को भी चुनाव लड़वाते हैं जो पढ़ी-लिखी नहीं होतीं या निरक्षर होती हैं। इस तरह एक स्तर पर महिला-सशक्तिरण भी हो गया हैं और दूसरी ओर पुरुषों की दबंगई भी जारी रहती है। इस तरह का विरूपित- सामंजस्य हमारी पंजायती व्यवस्था पर एक सवालिया निशान भी है। आज भारत के गावों और कस्बों में कुछ कारों के पीछे या आगे मुखियापति / सरपंचपति के छोटे- बड़े बोर्ड दिखते है।
इस संग्रह में एक कविता है- `पंचायती चुनाव में पर्चा भरने आई एक स्त्री’ । ये स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है टीवी मीडिया में उसे और उसकी पढाई लिखाई को लेकर ढेर सारे सवाल और अचरज उछाले जा रहे हैं। इन्हीं सवालों और अचरजों को लेकर ये स्त्री कहती है-
हमें देखकर चिहुंका क्यों है भारत महान देश में
स्त्री विमर्श का समकालीन चरण
उनसे कहो वे आगे बढ़ें चौथे पांचवे चरण की ओर
हम अभी नागिन 2 देखते हुए साड़ी में छठवीं आलपिन लगा रहे हैं
हमारी फर्जी उम्मीदवारी पर किसी को ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए
इतने फर्जी होते हुए भी हम सबसे कम फर्जी तार हैं इस तंत्र के
हम ही इस देश के आंकड़े और जमीन का सच
हमें खुद से पर्चा भरना नहीं आता तो इसमें हैरानी की क्या बात है
हम तुम्हारी उसी कागजी व्यवस्था की तामपत्री देन हैं
ये जो घेर कर बार- बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं
ये राष्ट्र का चौथा खंभा माइक लिए दौड़ते पत्रकार हैं
ये सब जानते हैं और सब लील भी लेते हैं
`एक जीवन अलग से’ में कई ऐसी कविताएं हैं जो भारतीय समाज में ऐसी कुछ ऐसी परिघटनाओं की याद दिलाती हैं जिनमें औरतों का शोषण सदियों से संस्थागत रूप ले चुका है। कई समुदायों की स्त्रियां इसमें शामिल हैं। जातियों में विभक्त समाज में औरतों का दोहरा शोषण होता है। एक तो जाति संबंधी और दूसरा औरत संबंधी। कुछ औरतों को आम बोलचाल में मिरासिन, कसबिन, नटिन या जोगिन जैसे नामों से पुकारा जाता हैं। कौन हैं वे औरतें? भारत में अंग्रेजी राज के जमाने कुछ जातियों को `डिनोटिफाइयड’ ट्राइब’ ( खानाबदोश समुदाय) घोषित किया गया। ये समुदाय अपराधी करार दिए गए। उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययन दृष्टि ने इनकी पड़ताल शुरू की है। पर इस दिशा में बहुत काम बाकी है। इनमें कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो कला – गाने बजाने- को लेकर समर्पित रहे पर सामाजिक रूप से हेय करार दिए गए। इनके दुख और पीड़ा को कविता में दर्ज ही नहीं किया गया, समझना तो दूर की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हुआ। नाजीवाद के समय यहूदियों के साथ तो अत्य़ाचार हुए ही, वो उन घूमंतु रोमाओं/ जिप्सियों के साथ भी हुए, जो कई देशों में फैला जन समुदाय है। ये सर्वविदित तथ्य है कि हिटलर ने लगभग ढाई से पांच लाख बीच रोमाओं को मरवाया। ये रोमाओं का जनसंहार था। यों रोमाओं के लिए प्रचलित शब्द `जिप्सी’ भी अपमानजनक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिरासिनें भी बोलचाल में भी अपमान झेलती है। मिरासिन भी एक अपमान जनक विशेषण है। ऐसे अन्य समानार्थी समुदाय की महिलाएं भी निरंतर शोषित व अपमानित होती रहती हैं। इसी को लक्षित करते हुए रूपम की कविता है `मरकही मिरासिनें’ जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह हैं-
अनगिनत पास्को और सेक्सुअल हरासमेंट केस इनकी देह और मन में दर्ज हैं
जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं
बचपन कब नष्ट हुआ इनको याद नहीं
कब विषाद मन से ही उठकर अनजाने में ही चेहरे पर बैठा
कब कमजोर की लड़ाई आंख से धाई चेहरे पर छाई
कुछ मत बताओ, कुछ न छुपाओ
मैं वहां से जानती हूं जहां से हमारी देह संरचना एक है
ये और ऐसी कई कविताओं स्त्री शोषण का इतिहास पेश करती हैं। ये कविताएं महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक इतिहास है। संक्षिप्त जरूर हे पर इतिहास है। इतिहास सिर्फ अकादमिक संस्थाओं में ही नही लिखा जाता बल्कि साहित्य – कहानियों, उपन्यासों, नाटकों और कविताओं- में भी भी लिखा जाता है।
रूपम मिश्र की एक और बड़ी खासियत अवध के इलाके में उनका गहरा धंसा होना है। मेरी जानकारी में आज की हिंदी में ऐसा कोई और कवि नहीं है जिसमें अवधी का संसार, वहां की लोकोक्तियां, मुहावरे, गीत, रीतिरिवाज , शब्द, रंगतें- इस तरह मौजूद हों। एकदम सहज रूप से। `मनशायन’, `मेहरीपन’, `अंजोरिया’, `पोढ़’, `हरियर’, `अन्हियरिया’, `संझलौका’, `दुखरोवनी’, `सुखरोवन’, `सबेरहिया’, `ढलेहिया’ जैसे शब्द उनके यहां सहज रूप से प्रयुक्त होते हैं। रूपम की कविताओं में स्थानीयता भी है और सार्वजनीनता भी और दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। कुछ लोगों के इस तरह की कविता के आस्वाद को लेकर आपत्तियां हो सकती हैं क्योंकि हिंदी का खड़ीबोलीकरण व्यापक रूप से हो चुका है। बेशक हर भाषा के साहित्य पर मानकीकरण का दबाव रहता है। फिर भी ये याद रखना चाहिए जिसे हिंदी कहते हैं वो कई बोलियों/ भाषाओं- अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा आदि- का समुच्चय है। हिंदी कथा साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में पहली बार ये स्थानीयकरण बहुत सशक्त रूप में आया था। फिर कृष्णा सोबती की रचनाओं में। हालांकि अकादमिक हिंदी जगत में उसे लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रहीं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से असहमत होते रहते हैं।
पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में स्थानीयता की उपस्थिति सहज है। कई बार जरूरी भी। संयोग नहीं कि कुछ हिंदी फिल्में भी स्थानीयता को समेटे रहती हैं। कभी उनमें मुंबइया हिंदी आती है तो कभी भोजपुरी। आमिर खान की फिल्म’ `दंगल’ में यदि हरियाणवी नहीं होती तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती। ये एक मिथ्या धारणा है कि साहित्य में बोलियों के शब्द आने से उसकी संप्रेषणीयता सीमित हो जाती है। हबीब तनवीर के लगभग सभी नाटक छत्तीसगढ़ी में हैं लेकिन वे विश्व स्तर पर सराहे और समझे गए हैं। रूपम की कविताओं का अवधी मिजाज खड़ी बोली की वाक्यरचना के रस को विस्तारित करता है। खड़ीबोली साहित्य का अवधीकरण/ भोजपुरीकरण/ बुंदेलीकरण/ बघेलीकरण भी निरंतर होते रहना चाहिए। पिज्जा की बढ़ती लोकप्रियता के दौर में लकठो का स्वाद भी बचा रहना चाहिए। भाषा स्वाद भी है।
स्त्री जीवन के अनुभवों का आलोचनात्मक इतिहास
——————-
(रूपम मिश्र के कविता संग्रह `एक जीवन अलग से’ पर केंद्रित लेख)
****
रवीन्द्र त्रिपाठी
कविता का एक काम उन रीतिरिवाजों का परीक्षण करना भी है जिनके बारे में अक्सर ये मान लिया जाता है कि ये हमारी परंपरा हैं और सनातन भी हैं। और ऐसी परंपरा या परंपराएं अक्सर महिमा-मंडित की जाती हैं और उनको महान और उदात्त बताया जाता है हालांकि वे समाज के एक बड़े वर्ग के लिए जकड़नों का काम करती हैं। परंपरा के नाम पर ये रीतिरिवाज धीरे धीरे समाज के एक बड़े हिस्से में इस तरह अपना लिए जाते हैं या थोप दिए जाते हैं कि दैनंदिन के जीवन में प्रतिमान अथवा दिशा-निर्देश की तरह काम करने लगते हैं। कुछ कुछ लक्ष्मण- रेखा की तरह कि इन्हें पार किया कि समाज और परिवार से बाहर।
वैसे पितृसत्ता की धारणाएं अलग अलग रूपों में पूरी दुनिया में मौजूद हैं लेकिन कुछ जगहों या देशों में वो शिक्षा के प्रसार और औद्योगिकीकरण व शहरीकरण के विस्तार की वजह से कुछ ढीली पड़ी हैं। भारतीय समाज में भी कुछ कुछ ऐसा हुआ है। पर ये भी सच है कि भारतीय गावों और कस्बों में अभी भी उसकी पकड़ बहुत मजबूत है। और ये भी सही है कि गांव के रीतिरिवाज अपनी चौहद्दी पार कर शहरों में फैल गए हैं। अर्थात शहरों और कस्बों में भी पितृसत्ता आज बहुत असरदार है। उसकी छायाएं महानगरों पर भी हैं। इसके कई रूप हैं। एक ओर तो पुरुषवाद डंके की चोट पर अपनी ताकत और धमक को कायम रखना चाहता है दूसरे स्त्रियों और महिलाओं की व्यक्तिगत और सामूहिक सोच में भी वह प्रवेश करता है। यानी औरतें भी पितृसत्ताक धारणाओं को अपने भीतर समा लेती हैं।
बेहतर होगा कि इसे रूपम मिश्र की एक कविता के माध्यम से ही समझा जाए। `एक जीवन अलग से’ में उनकी एक कविता है `अन्याय का दुलार’। उसे यहां पूरा ही उद्धृत किया रहा है ताकि समग्रता में पितृसत्ता की शक्ति और महिलाओं में मौजूद उसके रूप समझा जाए –
कुछ स्त्रियां पूरब से आई थीं कुछ पश्चिम से
दक्षिण की ज्यादा उत्तर की कम हैं यहां
उत्तर संख्या में अल्पसंख्यक होता है
बाकी अन्यायी कथाओं की आरोही हुंकारी
ये स्त्रियां ही यहां बहुसंख्यक हैं
और इनके सारे किस्सों मे रानियों की भूल पर देश-निकाला व भयावह मृत्युदंड थे
राजा जो हमेशा दूध का धोया होता है दंडक भी उसी के पास होता है
एक उम्र के बाद उलटे पल्ले और सीधे पल्ले के मत एक हो जाते हैं
चिंताएं आकर फिर अपने हाथ से छूटते जा रहे जमाने पर रूकती हैं
और फिर से इनकी चर्चा में नई लड़कियों के पंख निकल रहे हैं
हालांकि पंख टूट जाते हैं और वो घिसटती हुई एक दिन आकर
इन्हीं की बगल में खड़ी होती हैं और इन्हीं की भाषा बोलती हैं
खैर सारा दोष नई पीढ़ी की स्त्री उड़नबाजी पर है
विमर्श का केंद्र भी एक स्त्री का आशनाई में हत्या है
सभा का समवेत मत है कि ऐसी हत्याएं उतनी ही जायज और जरूरी हैं
जितना बीर बाबा का बहराम, मरी माई के थान पर कड़ाही देना
यें रंग, नस्ल और जेंडर की मक्कारियों का स्वप्रकट मठ था
यहां अन्हराई स्त्रियां स्वजातीय डाह से घटनाएओं की ओझाई करती थीं
ये तिल- तिलकट चना मसूर गेहूं जई को अंखुवाते ही चीन्ह लेती हैं
और अन्याय जवान से बूढ़ा, बूढ़े से अमर भी हो गया
और ये अभी तक उसे गोद में लेकर दुलार रही हैं।
समाज में, विशेषकर महिलाओं के बीच, किस प्रकार उन मूल्यों को आत्मसात कर लिया जाता है कि स्त्रियों के बीच स्वतंत्र चेतना का विकास अच्छा नहीं होता – उसे ये कविता रेखांकित करती है। इसमें औरतों की एक सभा का जिक्र है जो एक लड़की/स्त्री की हत्या पर हो रही है और उपस्थित महिलाएं उस स्त्री/ लड़की को ही दोषी मान रही है। जैसा कि लोककथाओं में होता रहा है – राजा को अपनी उस रानी को दंडित करने का अधिकार है जिसने किसी तरह की भूल की है। और दंड़ भी क्या? मत्युदंड। चूंकि दंडक हमेशा राजा के पास होता है इसलिए रानी कुछ कर भी नहीं सकती। होता ये भी है कि रानी कोई भूल न भी करे और राजा को शक हो जाए कि उसने कुछ गलत किया है तो भी रानी को मृत्युदंड ही मिलता है। कविता में जिस स्त्री की आशनाई की वजह से हत्या हुई है उसका पक्ष सामने नहीं आता है क्योंकि समाज का एक बड़ा हिस्सा उसे ऐसा करने नहीं देता । स्त्रियों की इस सभा में, जो एक मठ की तरह है, यही सर्वस्वीकृति है कि जिसकी हत्या हुई उसने प्रेम कर ही गुनाह किया। आम बोलचाल में ये कहा जाता है कि फलां लड़की बहुत उड़ रही है या उसके पंख निकल आए हैं। हालांकि ये मुहावरा लड़कों के बारे में प्रयुक्त किया जाता है लेकिन उनको गुनाहगार नहीं समझा जाता और न उनको दंड दिया जाता है। लड़की अगर उड़ने की कोशिश करे तो उसे अक्सर सजाए मौत ही मिलती है। ये सजा वैसे ज्यादातर पुरुष देते हैं पर उसमें परिवार और समाज की महिलाओं की भी सहमति होती है और वे हुंकारी भरती हैं कि उड़नेवाली के साथ ठीक किया गया। इनमें वे स्त्रियां भी होती है जो कुछ आधुनिक मानी जाती है। कविता में जिन्हें `उलटे पल्ले’ वाली कहा गया है वो तुलनात्मक रूप से आधुनिक मानी जाती है। और `सीधे पल्ले’ वाली स्त्रियां पांरपरिक या गंवई। (ये दीगर बात है कि आजकल महानगरों में भी सीधे पल्ले का रिवाज चल पड़ा है।) उड़ते पंखों वाली लड़कियां या स्त्रियां किसी को स्वीकार नहीं, चाहे वो सीधे पल्ले वाली हों या उल्टे पल्ले वाली। उनकी नजर में आशनाई में लगी लड़की की हत्या जायज है। और इस तरह ज्यादातर स्त्रियां उस अन्याय का दुलार ही करती हैं जो दरअसल उनके ही विरूद्ध है।
भारतीय समाज में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। और इस कारण सदियों पुरानी और जमी जमाई स्त्री- विरोधी- धारणाएं एक सीमा तक अशक्त हुई हैं। मगर एक सीमा तक ही। फेमिनिज्म यानी नारीवाद की अवधारणा हमारे यहां आई तो समाज में उन मान्यताओं का विरोध भी शुरू हुआ है जो औरतों के खिलाफ होती हैं और जिनकी कानून और संविधान भी इजाजत नहीं देता। किंतु समानांतर रूप से ये भी सच है कि समाज का एक शक्तिशाली वर्ग फेमिनिज्म का विरोध भी करता है। इसमें पुरुष तो शामिल हैं ही, औरते भी हैं। इसीलिए फेमिनिज्म भारतीय महानगरों से लेकर कस्बों – गावों तक निंदा और संदेह का पात्र भी माना जाता है। अक्सर ये कहा और लिखा भी जाता है कि नारीवाद पश्चिम से आई अवधारणा है और इसी कारण संदेहास्पद और अस्वीकार्य भी हैं। गोया पश्चिम से आई हर बात या वस्तु गलत है। पश्चिम से आई रेलगाड़ी, हवाई जहाज व कार जैसे वाहन का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं और किंतु फेमिनिज्म के खिलाफ लट्ठ लेकर खड़े हो जाते हैं। साहित्य में यथार्थवाद की अवधारणा भी पश्चिम से भारत आई पर उस पर कोई आरोप नहीं लगाता। दक्षिणपंथी ही नहीं कई वामपंथी भी फेमिनिज्म के विरुद्ध होते हैं। इसी कारण भारत में कई लोग – लड़कियों के पिता- दादा, मां- दादी भी – स्त्री- शिक्षा के प्रति भी दुराग्रह पाले रखते हैं और अपनी बेटियों-पोतियों की पढाई लिखाई के प्रति न सिर्फ अनिच्छुक बने रहते है, बल्कि कई बार तो उसका विरोध भी करते हैं। एक आम मुहावरा है जो लड़कियों को लेकर सुनाई पड़ता है – क्या ये कलक्टर बनेंगी? हालांकि लड़किया कलक्टर भी बन रही हैं और दूसरे क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रही हैं। लेकिन गावों –कस्बों में उनकी शिक्षा को लेकर दुराग्रह कायम है। इसी को लक्षित करते हुए रूपम की एक कविता है- `चली हैं कलेक्टर बनाने’। इसमें एक लड़की के बचपन से लेकर उसके वयस्क बनने के अनुभवों का बयान है। कविता इस तरह शुरू होती है-
पहली बार स्कूल जाते हुए खूब रोई तो
दादी ने मां को डांटा, नहीं पढ़ती है तो जाने दो
चलीं है कलेक्टर बनाने!
चूल्हे के पास राख पर उंगली से लिखाती
मां फिर डांट दी गई कि अभी तक खाना तैयार नहीं हुआ
चलीं है कलेक्टर बनाने
और जब आगे चलकर जब यही बच्ची शादी के बाद ससुराल चली जाती है तो वहां भी उसे उसी तरह के कटाक्ष सुनाई देते हैं
स्कूल और मां दोनो छूटे
किताबों को हाथ में ही थामे
मैं अब ससुराल आ गई थी
अबोध मन अभी गिरस्ती नहीं सीख पाया था
कदम- कदम पर होती रही गलतियां
जलती उंगलियों पर गीला आटा चिपकाती
सुनती रही सास की कड़क आवाज
कि एक भी शऊर नहीं सिखाया माई ने
चली थीं कलेक्टर बनाने
जिसे भारत में परंपरा बताया जाता है वो अपने तरीके और विधि-विधानों से स्त्रियों के जीवन का नियमन करता है। छोटी बच्चियों से लेकर स्त्रियों को `क्या करना चाहिए’, `कैसे चलना चाहिए’’. `क्यों सार्वजनिक स्थलों पर चुप रहना चाहिए ’(यानी बोलना नहीं चाहिए) – ये सब इस इन विधानों में शामिल होते है। एक बीमारी होती है एगोराफोबिया (agoraphobia ) जो अक्सर महिलाओं में पायी जाती है। इसका एक लक्षण होता है कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थलों पर जाने या वहां बोलने -घूमने में डर लगता है। वे इन स्थलों पर घबरा जाती हैं। 2016 में इसी पर केंद्रित पवन कृपलानी की एक फिल्म भी आई थी जिसका नाम था `फोबिया‘। इसमें राधिका आप्टे की मुख्य भूमिका थी। हालांकि फिल्म होने की वजह से इसमें एक कहानी भी थी और साथ ही कुछ बातें भी थी लेकिन मूल बात वही थी –अगोराफोबिया। अगोराफोबिया के पीछे कई तात्कालिक कारण भी होते हैं। पर सबसे बड़ी वजह है भीतर का डर। ये कई वजहों से पैदा होता है। बचपन या युवावस्था में यदि परिवार या आसपास के लोगों द्वारा किसी के भीतर डर भऱा जाए तो वो अगोराफोबिया का शिकार हो सकता/ सकती है। हमारे यहां ग्रामांचलों में ( और ईरान जैसे कई और देशों में भी) लड़कियों पर बचपन से लेकर युवावस्था तक सार्वजनिक जगहों पर जाने या वहां बोलने पर निषेध होता है। एक कविता में इसी की शिनाख्त करते हुए रूपम कहती हैं.
हमें अधिकार का पर्यायवाची कर्तव्य बताया गया
हमने साहस की जगह हमेशा डर पढ़ा
स्कूल की वाद विवाद प्रतियोगिता में हमने कभी भाग नहीं लिया
क्योंकि आजी कहती मुंहजोरी भले घर की लड़कियों के लक्षऩ नहीं
हमें हमेशा बोलना नहीं सुनना सिखाया गया
तोते की तरह रटाए गए कुछ अति विनीत शब्द
जो गर्दन को और झुका प्रतीत कराते
ये `विमर्श हड़पने की नीति’ है जो समाज में लंबे समय से जारी है। यही कारण है कि फेमिनिज्म का विरोध आम जीवन में नहीं बल्कि विश्वविद्यालयों और अकादमिक संस्थानों में भी होता है। `अभी हमारी बहुत- सी जगहें हैं जहां हम नही हैं‘ लिखते हुए रूपम सामाजिक उपक्रमों में औरतों की अपेक्षाकृत अनुपस्थिति की ओर संकेत करती हैं और अपनी एक अन्य कविता में इसी महिलाद्वेष के परिणाम की ओर भी इशारा करते हुए कहती हैं `कुछ तितलियां बिना उड़े ही बूढ़ी हो जाती हैं’। तितलियों से यहां आशय उन औरतें से है जो जीवन भर अपनी किसी स्वाभाविक और सहज चाहत को अभिव्यक्त भी नहीं कर पातीं। ये वही माहौल हैं जिसमें लड़कों और लड़कियों के लिए प्रेम की अलग अलग परिभाषाएं है। जब कोई लड़का प्रेम करता है तो ये सहज माना जाता है पर लड़की के प्रेम को गलत कहा जाता है उसके लिए जिस क्रिया का प्रयोग किया जाता है वो है फंसना। यानी लड़की प्रेम नहीं करती, वह किसी के साथ फंस जाती है – इस जैसा निष्कर्ष अक्सर सुनाई देता है।
इस संग्रह में कई ऐसे सामाजिक वृतांत औऱ वाकये हैं जिनसे हम अक्सर ही टकराते हैं। इस संग्रह में कई कहानियां हैं जो कविता की शक्ल में है। ये कहानियां या कविताएं उन सामाजिक प्रसंगों को सामने लाती हैं जिनमें महिलाद्वेषी दृष्टिकोण उभरते हैं। कुछ ऐसी महिला व्यक्तित्व ( `शालू सिंह’ `विद्योत्तमा शुक्ला’) भी इस संग्रह की कविताओं में आती हैं जो संघर्ष और प्रतिकार की दृष्टांत बन जाती हैं। भारतीय लोकतंत्र में आए कुछ हालिया तबदीलियों को दर्ज करने की कोशिश भी रूपम ने की है। जैसे जब से पंचायती राज व्यवस्था में महिला आरक्षण जैसे प्रावधान लागू किए गए तब से महिला मुखिया/सरपंचों की संख्या भी बढ़ी है। इससे एक तो ये हुआ कि पंचायती लोकतंत्र की परिधि का विस्तार हुआ है और वहां पुरुष- स्त्री का असंतुलन कुछ कम हुआ। पर दूसरी तरफ उन महिला मुखिया/ सरपंचों के पतियों या पिताओं की पौबारह हो गई है और प्रछन्न अधिकार उनके हिस्से में आ गए। अंग्रेजी मे जिसे`डे ज्यूरे’ और `डी फैक्टो’ कहते हैं उसका समकालीन रूप आज के भारत के कई पंचायतों मे दिख रहा है। `डे ज्यूरे’ या औपचारिक सत्ता तो महिला मुखिया/सरपचों के पास है लेकिन `डी फैक्टो’ यानी वास्तविक सत्ता पुरुषों के पास ही रहती है जिसे पति या पिता इस्तेमाल करते हैं। चूंकि प्रावधानों की वजह से महिलाएं ही आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ सकती हैं इसलिए कई पुरुष अपनी उन पत्नियों को भी चुनाव लड़वाते हैं जो पढ़ी-लिखी नहीं होतीं या निरक्षर होती हैं। इस तरह एक स्तर पर महिला-सशक्तिरण भी हो गया हैं और दूसरी ओर पुरुषों की दबंगई भी जारी रहती है। इस तरह का विरूपित- सामंजस्य हमारी पंजायती व्यवस्था पर एक
सवालिया निशान भी है। आज भारत के गावों और कस्बों में कुछ कारों के पीछे या आगे मुखियापति / सरपंचपति के छोटे- बड़े बोर्ड दिखते है।
इस संग्रह में एक कविता है- `पंचायती चुनाव में पर्चा भरने आई एक स्त्री’ । ये स्त्री पढ़ी लिखी नहीं है टीवी मीडिया में उसे और उसकी पढाई लिखाई को लेकर ढेर सारे सवाल और अचरज उछाले जा रहे हैं। इन्हीं सवालों और अचरजों को लेकर ये स्त्री कहती है-
हमें देखकर चिहुंका क्यों है भारत महान देश में
स्त्री विमर्श का समकालीन चरण
उनसे कहो वे आगे बढ़ें चौथे पांचवे चरण की ओर
हम अभी नागिन 2 देखते हुए साड़ी में छठवीं आलपिन लगा रहे हैं
हमारी फर्जी उम्मीदवारी पर किसी को ज्यादा शर्मिंदा नहीं होना चाहिए
इतने फर्जी होते हुए भी हम सबसे कम फर्जी तार हैं इस तंत्र के
हम ही इस देश के आंकड़े और जमीन का सच
हमें खुद से पर्चा भरना नहीं आता तो इसमें हैरानी की क्या बात है
हम तुम्हारी उसी कागजी व्यवस्था की तामपत्री देन हैं
ये जो घेर कर बार- बार मुझसे सवाल पूछ रहे हैं
ये राष्ट्र का चौथा खंभा माइक लिए दौड़ते पत्रकार हैं
ये सब जानते हैं और सब लील भी लेते हैं
`एक जीवन अलग से’ में कई ऐसी कविताएं हैं जो भारतीय समाज में ऐसी कुछ ऐसी परिघटनाओं की याद दिलाती हैं जिनमें औरतों का शोषण सदियों से संस्थागत रूप ले चुका है। कई समुदायों की स्त्रियां इसमें शामिल हैं। जातियों में विभक्त समाज में औरतों का दोहरा शोषण होता है। एक तो जाति संबंधी और दूसरा औरत संबंधी। कुछ औरतों को आम बोलचाल में मिरासिन, कसबिन, नटिन या जोगिन जैसे नामों से पुकारा जाता हैं। कौन हैं वे औरतें? भारत में अंग्रेजी राज के जमाने कुछ जातियों को `डिनोटिफाइयड’ ट्राइब’ ( खानाबदोश समुदाय) घोषित किया गया। ये समुदाय अपराधी करार दिए गए। उत्तर-औपनिवेशिक अध्ययन दृष्टि ने इनकी पड़ताल शुरू की है। पर इस दिशा में बहुत काम बाकी है। इनमें कुछ समुदाय ऐसे भी हैं जो कला – गाने बजाने- को लेकर समर्पित रहे पर सामाजिक रूप से हेय करार दिए गए। इनके दुख और पीड़ा को कविता में दर्ज ही नहीं किया गया, समझना तो दूर की बात है। और ऐसा भी नहीं है कि ये सिर्फ भारत में ही हुआ। नाजीवाद के समय यहूदियों के साथ तो अत्य़ाचार हुए ही, वो उन घूमंतु रोमाओं/ जिप्सियों के साथ भी हुए, जो कई देशों में फैला जन समुदाय है। ये सर्वविदित तथ्य है कि हिटलर ने लगभग ढाई से पांच लाख बीच रोमाओं को मरवाया। ये रोमाओं का जनसंहार था। यों रोमाओं के लिए प्रचलित शब्द `जिप्सी’ भी अपमानजनक है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिरासिनें भी बोलचाल में भी अपमान झेलती है। मिरासिन भी एक अपमान जनक विशेषण है। ऐसे अन्य समानार्थी समुदाय की महिलाएं भी निरंतर शोषित व अपमानित होती रहती हैं। इसी को लक्षित करते हुए रूपम की कविता है `मरकही मिरासिनें’ जिसकी कुछ पंक्तियां इस तरह हैं-
अनगिनत पास्को और सेक्सुअल हरासमेंट केस इनकी देह और मन में दर्ज हैं
जिनकी कहीं कोई सुनवाई नहीं
बचपन कब नष्ट हुआ इनको याद नहीं
कब विषाद मन से ही उठकर अनजाने में ही चेहरे पर बैठा
कब कमजोर की लड़ाई आंख से धाई चेहरे पर छाई
कुछ मत बताओ, कुछ न छुपाओ
मैं वहां से जानती हूं जहां से हमारी देह संरचना एक है
ये और ऐसी कई कविताओं स्त्री शोषण का इतिहास पेश करती हैं। ये कविताएं महिलाओं की सामाजिक स्थिति का आलोचनात्मक इतिहास है। संक्षिप्त जरूर हे पर इतिहास है। इतिहास सिर्फ अकादमिक संस्थाओं में ही नही लिखा जाता बल्कि साहित्य – कहानियों, उपन्यासों, नाटकों और कविताओं- में भी भी लिखा जाता है।
रूपम मिश्र की एक और बड़ी खासियत अवध के इलाके में उनका गहरा धंसा होना है। मेरी जानकारी में आज की हिंदी में ऐसा कोई और कवि नहीं है जिसमें अवधी का संसार, वहां की लोकोक्तियां, मुहावरे, गीत, रीतिरिवाज , शब्द, रंगतें- इस तरह मौजूद हों। एकदम सहज रूप से। `मनशायन’, `मेहरीपन’, `अंजोरिया’, `पोढ़’, `हरियर’, `अन्हियरिया’, `संझलौका’, `दुखरोवनी’, `सुखरोवन’, `सबेरहिया’, `ढलेहिया’ जैसे शब्द उनके यहां सहज रूप से प्रयुक्त होते हैं। रूपम की कविताओं में स्थानीयता भी है और सार्वजनीनता भी और दोनों एक दूसरे में घुले मिले हैं। कुछ लोगों के इस तरह की कविता के आस्वाद को लेकर आपत्तियां हो सकती हैं क्योंकि हिंदी का खड़ीबोलीकरण व्यापक रूप से हो चुका है। बेशक हर भाषा के साहित्य पर मानकीकरण का दबाव रहता है। फिर भी ये याद रखना चाहिए जिसे हिंदी कहते हैं वो कई बोलियों/ भाषाओं- अवधी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, बुंदेली, बघेली, ब्रजभाषा आदि- का समुच्चय है। हिंदी कथा साहित्य में फणीश्वरनाथ रेणु की रचनाओं में पहली बार ये स्थानीयकरण बहुत सशक्त रूप में आया था। फिर कृष्णा सोबती की रचनाओं में। हालांकि अकादमिक हिंदी जगत में उसे लेकर आपत्तियां दर्ज की जाती रहीं। अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया से असहमत होते रहते हैं।
पर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में स्थानीयता की उपस्थिति सहज है। कई बार जरूरी भी। संयोग नहीं कि कुछ हिंदी फिल्में भी स्थानीयता को समेटे रहती हैं। कभी उनमें मुंबइया हिंदी आती है तो कभी भोजपुरी। आमिर खान की फिल्म’ `दंगल’ में यदि हरियाणवी नहीं होती तो उसकी विश्वसनीयता कम हो जाती। ये एक मिथ्या धारणा है कि साहित्य में बोलियों के शब्द आने से उसकी संप्रेषणीयता सीमित हो जाती है। हबीब तनवीर के लगभग सभी नाटक छत्तीसगढ़ी में हैं लेकिन वे विश्व स्तर पर सराहे और समझे गए हैं। रूपम की कविताओं का अवधी मिजाज खड़ी बोली की वाक्यरचना के रस को विस्तारित करता है। खड़ीबोली साहित्य का अवधीकरण/ भोजपुरीकरण/ बुंदेलीकरण/ बघेलीकरण भी निरंतर होते रहना चाहिए। पिज्जा की बढ़ती लोकप्रियता के दौर में लकठो का स्वाद भी बचा रहना चाहिए। भाषा स्वाद भी है।

